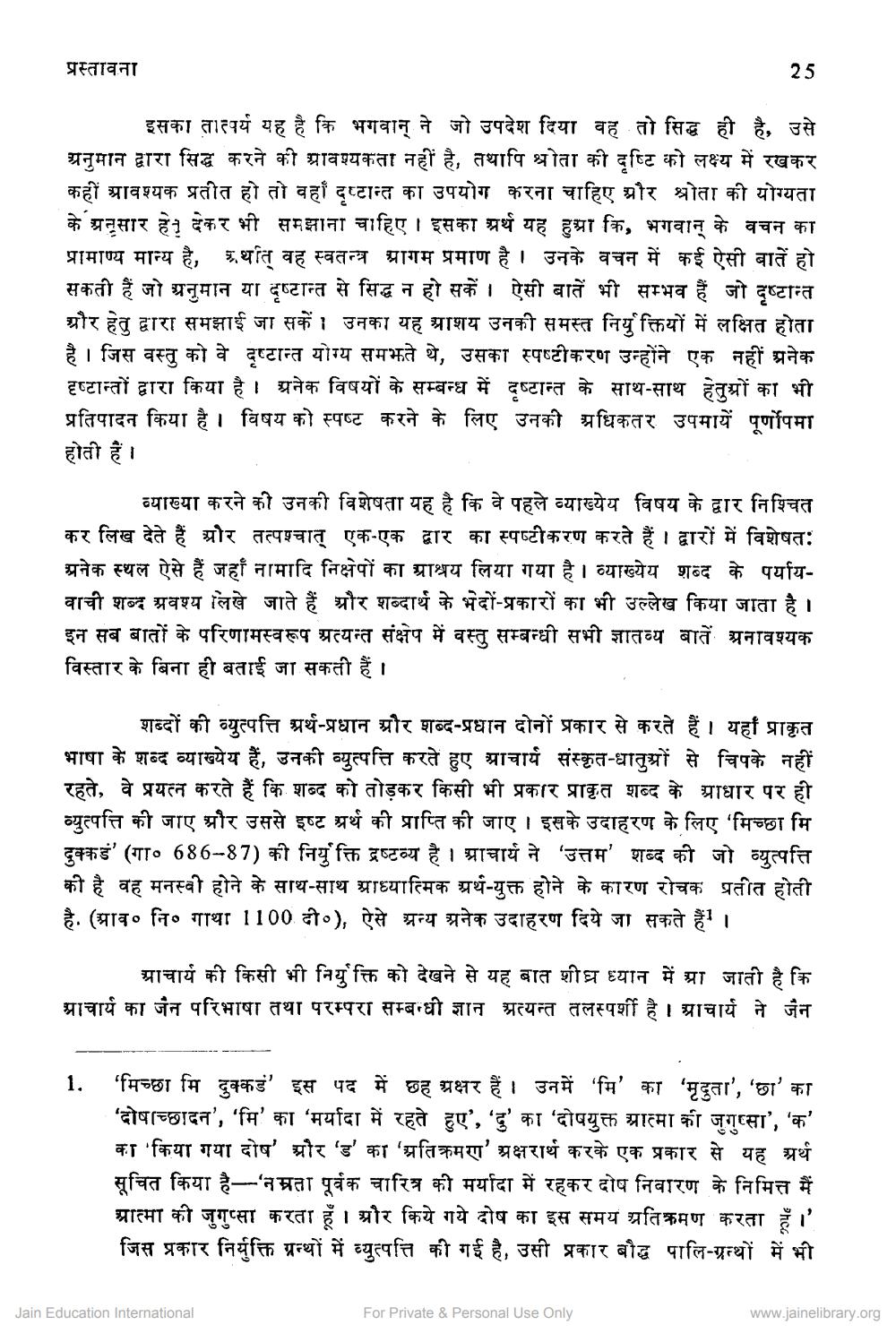________________
प्रस्तावना
इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् ने जो उपदेश दिया वह तो सिद्ध ही है, उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि श्रोता की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर कहीं आवश्यक प्रतीत हो तो वहाँ दृष्टान्त का उपयोग करना चाहिए और श्रोता की योग्यता के अनुसार हे देकर भी समझाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान् के वचन का प्रामाण्य मान्य है, अर्थात् वह स्वतन्त्र आगम प्रमाण है । उनके वचन में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो अनुमान या दृष्टान्त से सिद्ध न हो सकें। ऐसी बातें भी सम्भव हैं जो दृष्टान्त र हेतु द्वारा समझाई जा सकें । उनका यह प्राशय उनकी समस्त नियुक्तियों में लक्षित होता है । जिस वस्तु को वे दृष्टान्त योग्य समझते थे, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने एक नहीं अनेक दृष्टान्तों द्वारा किया है अनेक विषयों के सम्बन्ध में दृष्टान्त के साथ-साथ हेतुत्रों का भी प्रतिपादन किया है । विषय को स्पष्ट करने के लिए उनकी अधिकतर उपमायें पूर्णोपमा होती हैं ।
व्याख्या करने की उनकी विशेषता यह है कि वे पहले व्याख्येय विषय के द्वार निश्चित कर लिख देते हैं और तत्पश्चात् एक-एक द्वार का स्पष्टीकरण करते हैं । द्वारों में विशेषतः अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ नामादि निक्षेपों का श्राश्रय लिया गया है । व्याख्येय शब्द के पर्यायवाची शब्द अवश्य लिखे जाते हैं और शब्दार्थ के भेदों प्रकारों का भी उल्लेख किया जाता है। इन सब बातों के परिणामस्वरूप अत्यन्त संक्षेप में वस्तु सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य बातें अनावश्यक विस्तार के बिना ही बताई जा सकती हैं ।
25
शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थ - प्रधान और शब्द प्रधान दोनों प्रकार से करते हैं । यहाँ प्राकृत भाषा के शब्द व्याख्येय हैं, उनकी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य संस्कृत धातुत्रों से चिपके नहीं रहते, वे प्रयत्न करते हैं कि शब्द को तोड़कर किसी भी प्रकार प्राकृत शब्द के आधार पर ही व्युत्पत्ति की जाए और उससे इष्ट अर्थ की प्राप्ति की जाए। इसके उदाहरण के लिए 'मिच्छामि दुक्कडं' (गा० 686-87 ) की नियुक्ति द्रष्टव्य है । प्राचार्य ने 'उत्तम' शब्द की जो व्युत्पत्ति
है वह मनस्वी होने के साथ-साथ आध्यात्मिक अर्थ-युक्त होने के कारण रोचक प्रतीत होती है. (प्राव० नि० गाथा 1100 दी०), ऐसे अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं ।
आचार्य की किसी भी नियुक्ति को देखने से यह बात शीघ्र ध्यान में प्रा जाती है कि प्राचार्य का जैन परिभाषा तथा परम्परा सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त तलस्पर्शी है । प्राचार्य ने जैन
1.
'मिच्छामि दुक्कडं' इस पद में छह ग्रक्षर हैं । उनमें 'मि' का 'मृदुता', 'छा' का 'दोषाच्छादन', 'मि' का 'मर्यादा में रहते हुए', 'दु' का 'दोषयुक्त आत्मा की जुगुप्सा', 'क’ का किया गया दोष' और 'ड' का 'अतिक्रमण' अक्षरार्थ करके एक प्रकार से यह अर्थ सूचित किया है - 'नम्रता पूर्वक चारित्र की मर्यादा में रहकर दोष निवारण के निमित्त मैं श्रात्मा की जुगुप्सा करता हूँ। और किये गये दोष का इस समय प्रतिक्रमण करता हूँ ।' जिस प्रकार निर्मुक्ति ग्रन्थों में व्युत्पत्ति की गई है, उसी प्रकार बौद्ध पालि-ग्रन्थों में भी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org