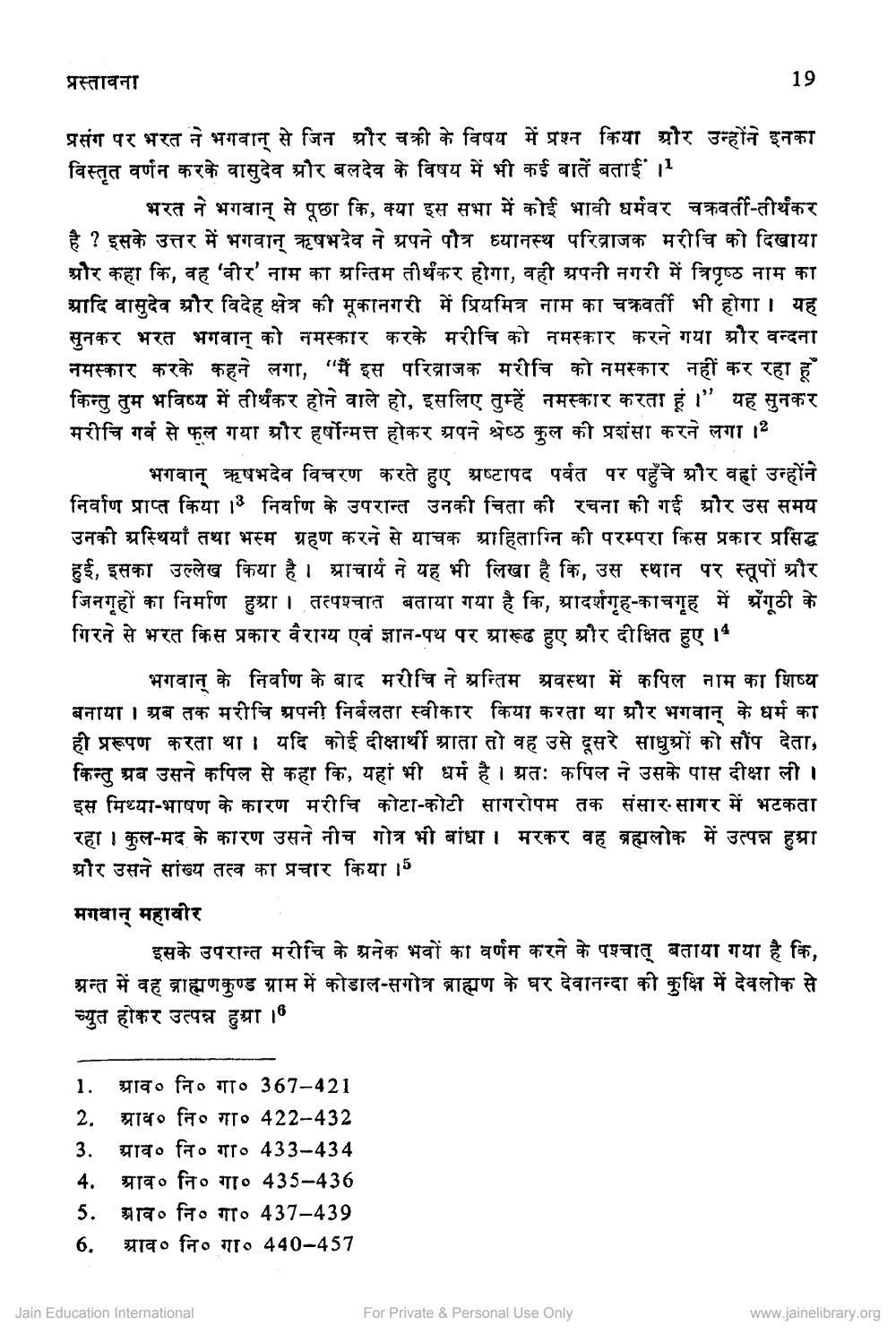________________
प्रस्तावना
प्रसंग पर भरत ने भगवान् से जिन और चक्री के विषय में प्रश्न किया और उन्होंने इनका विस्तृत वर्णन करके वासुदेव और बलदेव के विषय में भी कई बातें बताई।।
भरत ने भगवान् से पूछा कि, क्या इस सभा में कोई भावी धर्मवर चक्रवर्ती-तीर्थकर है ? इसके उत्तर में भगवान् ऋषभदेव ने अपने पौत्र ध्यानस्थ परिव्राजक मरीचि को दिखाया और कहा कि, वह 'वीर' नाम का अन्तिम तीर्थंकर होगा, वही अपनी नगरी में त्रिपृष्ठ नाम का आदि वासुदेव और विदेह क्षेत्र की मूकानगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती भी होगा। यह सुनकर भरत भगवान् को नमस्कार करके मरीचि को नमस्कार करने गया और वन्दना नमस्कार करके कहने लगा, "मैं इस परिव्राजक मरीचि को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ किन्तु तुम भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार करता हूं।" यह सुनकर मरीचि गर्व से फल गया और हर्षोन्मत्त होकर अपने श्रेष्ठ कुल की प्रशंसा करने लगा।
__भगवान् ऋषभदेव विचरण करते हुए अष्टापद पर्वत पर पहुँचे और वहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । निर्वाण के उपरान्त उनकी चिता की रचना की गई और उस समय उनकी अस्थियाँ तथा भस्म ग्रहण करने से याचक आहिताग्नि की परम्परा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, इसका उल्लेख किया है। प्राचार्य ने यह भी लिखा है कि, उस स्थान पर स्तूपों और जिनगृहों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात बताया गया है कि, आदर्शगृह-काचगृह में अँगूठी के गिरने से भरत किस प्रकार वैराग्य एवं ज्ञान-पथ पर आरूढ हुए और दीक्षित हुए।
भगवान के निर्वाण के बाद मरीचि ने अन्तिम अवस्था में कपिल नाम का शिष्य बनाया। अब तक मरीचि अपनी निर्बलता स्वीकार किया करता था और भगवान् के धर्म का ही प्ररूपण करता था। यदि कोई दीक्षार्थी अाता तो वह उसे दूसरे साधुओं को सौंप देता, किन्तु अब उसने कपिल से कहा कि, यहां भी धर्म है। अतः कपिल ने उसके पास दीक्षा ली। इस मिथ्या-भाषण के कारण मरीचि कोटा-कोटी सागरोपम तक संसार सागर में भटकता रहा । कुल-मद के कारण उसने नीच गोत्र भी बांधा। मरकर वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुना और उसने सांख्य तत्व का प्रचार किया । मगवान् महावीर
इसके उपरान्त मरीचि के अनेक भवों का वर्णम करने के पश्चात् बताया गया है कि, अन्त में वह ब्राह्मणकुण्ड ग्राम में कोडाल-सगोत्र ब्राह्मण के घर देवानन्दा की कुक्षि में देवलोक से च्युत होकर उत्पन्न हुआ।
1. आव० नि० गा० 367-421 2. आव०नि० गा० 422-432 3. आव० नि० गा० 433-434
आव०नि० गा० 435-436 5. आव०नि० गा० 437-439 6. आव०नि० गा० 440-457
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org