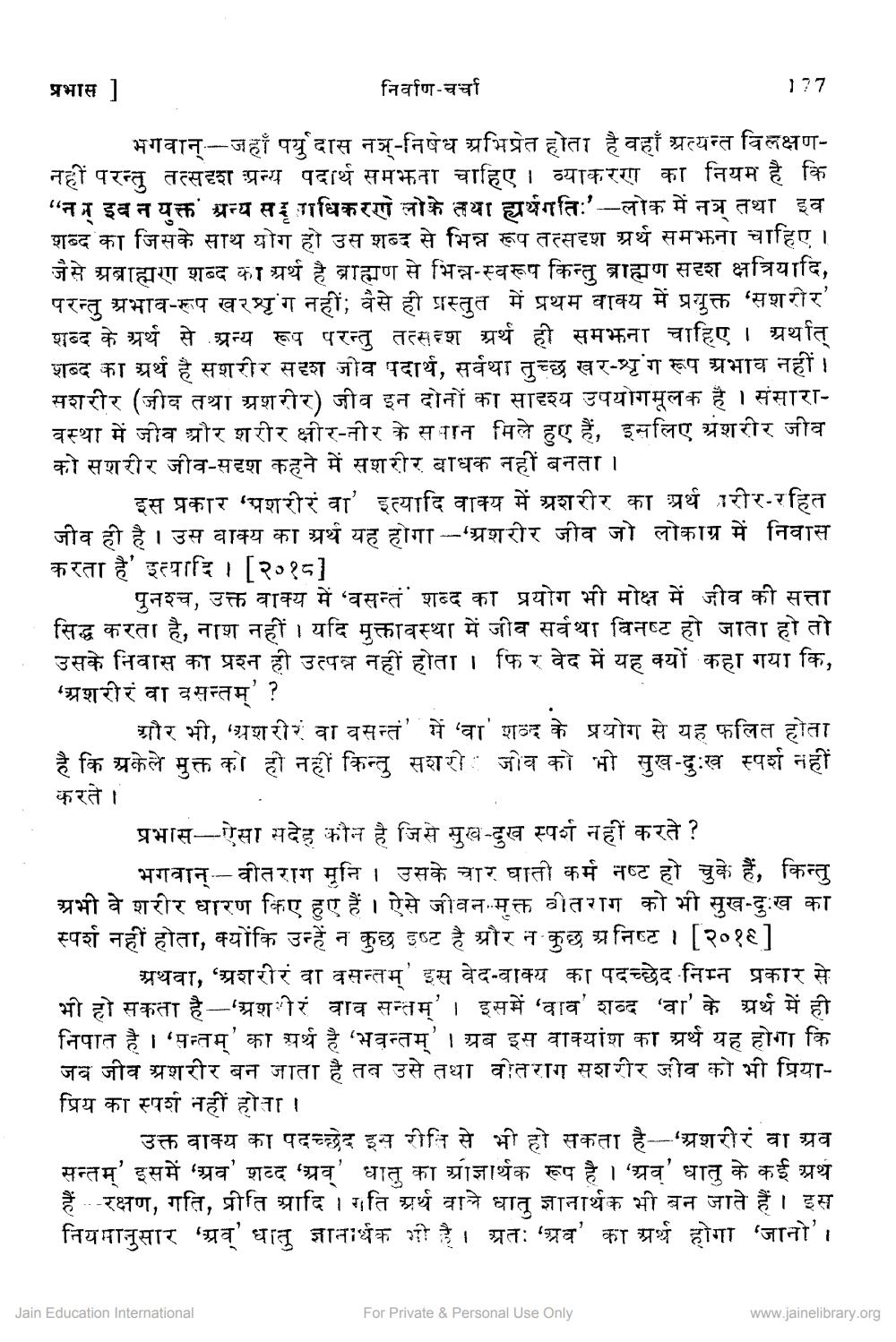________________ प्रभास ] निर्वाण-चर्चा 177 भगवान्-जहाँ पर्युदास नञ्-निषेध अभिप्रेत होता है वहाँ अत्यन्त विलक्षणनहीं परन्तु तत्सदृश अन्य पदार्थ समझना चाहिए। व्याकरण का नियम है कि "नम् इव न युक्त अन्य सदृशाधिकरणे लोके तथा ह्यर्थगतिः' -लोक में नत्र तथा इव शब्द का जिसके साथ योग हो उस शब्द से भिन्न रूप तत्सदृश अर्थ समझना चाहिए। जैसे अब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्राह्मण से भिन्न-स्वरूप किन्तु ब्राह्मण सदृश क्षत्रियादि, परन्तु अभाव-रूप खरशृग नहीं; वैसे ही प्रस्तुत में प्रथम वाक्य में प्रयुक्त 'सशरीर' शब्द के अर्थ से अन्य रूप परन्तु तत्सदश अर्थ ही समझना चाहिए / अर्थात् शब्द का अर्थ है सशरीर सदृश जोव पदार्थ, सर्वथा तुच्छ खर-शृंग रूप प्रभाव नहीं। सशरीर (जीव तथा अशरीर) जीव इन दोनों का सादृश्य उपयोगमूलक है / संसारावस्था में जीव और शरीर क्षीर-नीर के समान मिले हुए हैं, इसलिए अंशरीर जीव को सशरीर जीव-सदृश कहने में सशरीर बाधक नहीं बनता। इस प्रकार 'प्रशरीरं वा' इत्यादि वाक्य में अशरीर का अर्थ परीर-रहित जीव ही है / उस वाक्य का अर्थ यह होगा -'अशरीर जीव जो लोकाग्र में निवास करता है' इत्यादि / [2018] पुनश्च, उक्त वाक्य में 'वसन्तं शब्द का प्रयोग भी मोक्ष में जीव की सत्ता सिद्ध करता है, नाश नहीं। यदि मुक्तावस्था में जीव सर्वथा विनष्ट हो जाता हो तो उसके निवास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फि र वेद में यह क्यों कहा गया कि, 'अशरीरं वा वसन्तम्' ? और भी, 'शरीरं वा वसन्तं' में 'वा' शब्द के प्रयोग से यह फलित होता है कि अकेले मुक्त को ही नहीं किन्तु सशरो जीव को भी सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते। प्रभास-ऐसा सदेह कौन है जिसे सुख-दुख स्पर्श नहीं करते? भगवान्- वीतराग मुनि / उसके चार घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, किन्तु अभी वे शरीर धारण किए हुए हैं। ऐसे जीवन मुक्त वीतराग को भी सुख-दुःख का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि उन्हें न कुछ इष्ट है और न कुछ अनिष्ट / [2016] ___अथवा, 'अशरीरं वा वसन्तम्' इस वेद-वाक्य का पदच्छेद निम्न प्रकार से भी हो सकता है-'अशीरं वाव सन्तम्' / इसमें 'वाव' शब्द 'वा' के अर्थ में ही निपात है / 'सन्तम्' का अर्थ है 'भवन्तम्' / अब इस वाक्यांश का अर्थ यह होगा कि जब जीव अशरीर बन जाता है तब उसे तथा वीतराग सशरीर जीव को भी प्रियाप्रिय का स्पर्श नहीं होता। उक्त वाक्य का पदच्छेद इस रीति से भी हो सकता है-'अशरीरं वा अव सन्तम्' इसमें 'अव' शब्द 'अव्' धातु का आज्ञार्थक रूप है / 'अव' धातु के कई अथ हैं .-रक्षण, गति, प्रीति आदि / गति अर्थ वाले धातू ज्ञानार्थक भी बन जाते हैं। इस नियमानुसार 'अव्' धातु ज्ञानार्थक भी है। अत: 'व' का अर्थ होगा 'जानो'। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org