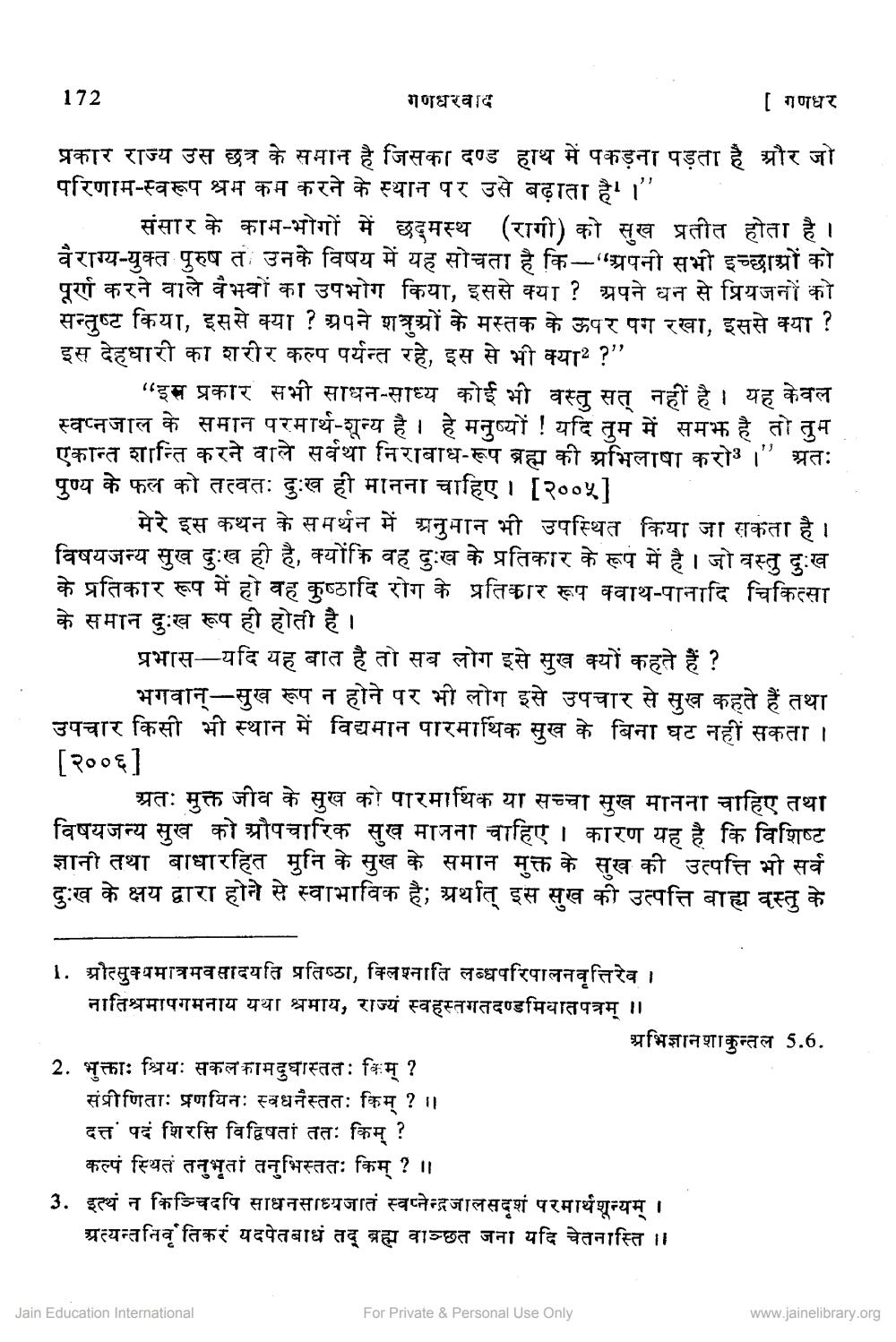________________ 172 गणधरवाद [ गणधर प्रकार राज्य उस छत्र के समान है जिसका दण्ड हाथ में पकड़ना पड़ता है और जो परिणाम-स्वरूप श्रम कम करने के स्थान पर उसे बढ़ाता है।" __ संसार के काम-भोगों में छद्मस्थ (रागी) को सुख प्रतीत होता है / वैराग्य-युक्त पुरुष त उनके विषय में यह सोचता है कि-"अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वैभवों का उपभोग किया, इससे क्या ? अपने धन से प्रियजनों को सन्तुष्ट किया, इससे क्या ? अपने शत्रुओं के मस्तक के ऊपर पग रखा, इससे क्या ? इस देहधारी का शरीर कल्प पर्यन्त रहे, इस से भी क्या ?' "इस प्रकार सभी साधन-साध्य कोई भी वस्तु सत नहीं है। यह केवल स्वप्नजाल के समान परमार्थ-शून्य है। हे मनुष्यों ! यदि तुम में समझ है तो तुम एकान्त शान्ति करने वाले सर्वथा निराबाध-रूप ब्रह्म की अभिलाषा करो।" अतः पुण्य के फल को तत्वतः दुःख ही मानना चाहिए। [2005] मेरे इस कथन के समर्थन में अनुमान भी उपस्थित किया जा सकता है। विषयजन्य सुख दुःख ही है, क्योंकि वह दुःख के प्रतिकार के रूप में है। जो वस्तु दुःख के प्रतिकार रूप में हो वह कुष्ठादि रोग के प्रतिकार रूप क्वाथ-पानादि चिकित्सा के समान दुःख रूप ही होती है। प्रभास-यदि यह बात है तो सब लोग इसे सुख क्यों कहते हैं ? भगवान्-सुख रूप न होने पर भी लोग इसे उपचार से सुख कहते हैं तथा उपचार किसी भी स्थान में विद्यमान पारमार्थिक सुख के बिना घट नहीं सकता। [2006] अतः मुक्त जीव के सुख को पारमार्थिक या सच्चा सुख मानना चाहिए तथा विषयजन्य सुख को औपचारिक सुख माजना चाहिए। कारण यह है कि विशिष्ट ज्ञानी तथा बाधारहित मुनि के सुख के समान मुक्त के सख की उत्पत्ति भी सर्व दुःख के क्षय द्वारा होने से स्वाभाविक है; अर्थात् इस सुख की उत्पत्ति बाह्य वस्तु के 1. प्रौत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा, क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवत्तिरेव / नातिश्रमापगमनाय यथा श्रमाय, राज्यं स्वहस्तगतदण्डमिवातपत्रम् / / अभिज्ञानशाकुन्तल 5.6. 2. भुक्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किम् ? संप्रीणिताः प्रणयिनः स्वधनैस्ततः किम् ? / / दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ? कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ? / / 3. इत्थं न किञ्चिदपि साधनसाध्यजातं स्वप्नेन्द्रजालसदृशं परमार्थशून्यम् / अत्यन्त निवृतिकरं यदपेतबाधं तद् ब्रह्म वाञ्छत जना यदि चेतनास्ति / / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org