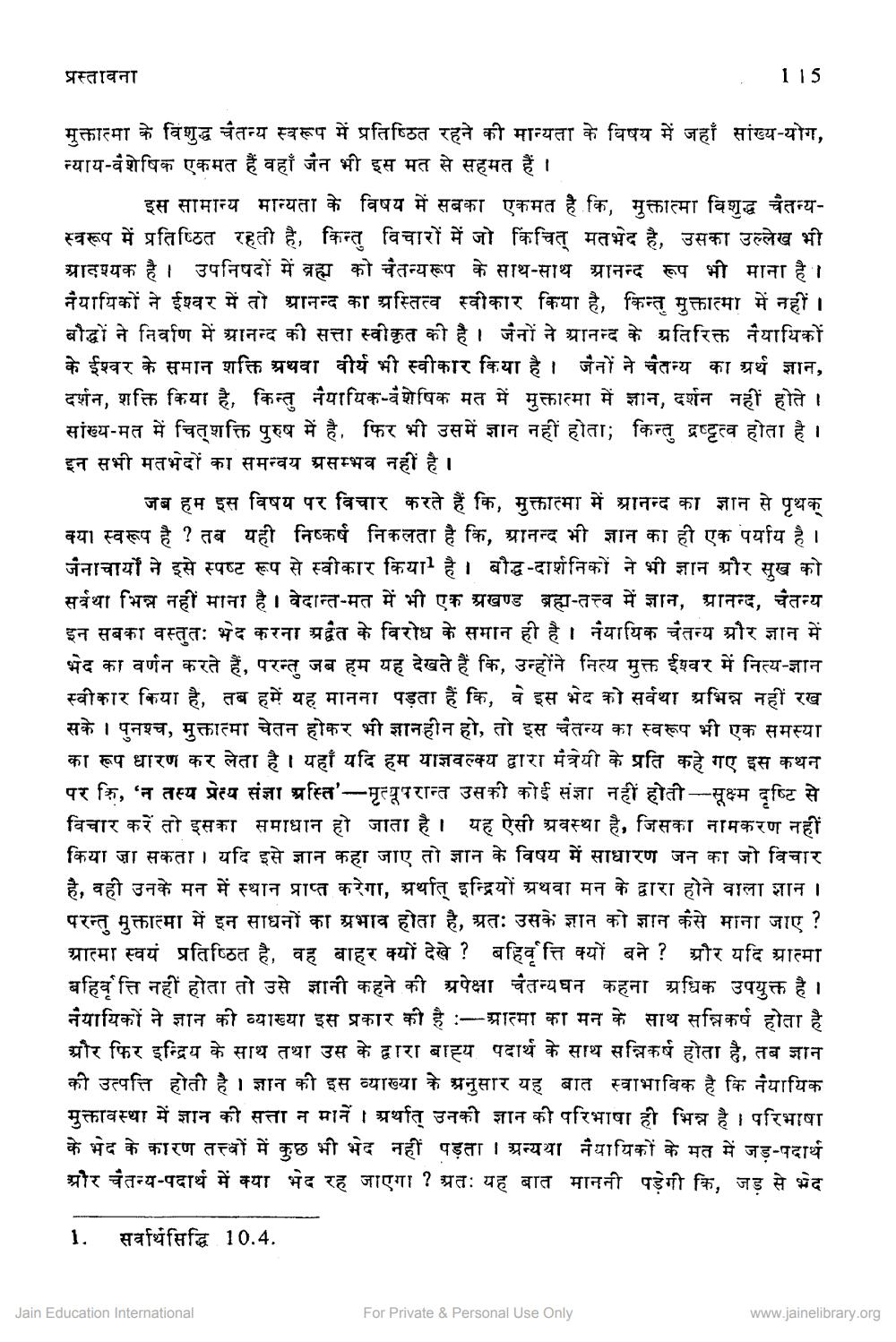________________
प्रस्तावना
115
मुक्तात्मा के विशुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने की मान्यता के विषय में जहाँ सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक एकमत हैं वहाँ जैन भी इस मत से सहमत हैं ।
इस सामान्य मान्यता के विषय में सबका एकमत है कि, मुक्तात्मा विशुद्ध चैतन्यस्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है, किन्तु विचारों में जो किंचित् मतभेद है, उसका उल्लेख भी आवश्यक है। उपनिषदों में ब्रह्म को चैतन्यरूप के साथ-साथ आनन्द रूप भी माना है। नैयायिकों ने ईश्वर में तो प्रानन्द का अस्तित्व स्वीकार किया है, किन्तु मुक्तात्मा में नहीं। बौद्धों ने निर्वाण में प्रानन्द की सत्ता स्वीकृत की है। जैनों ने आनन्द के अतिरिक्त नैयायिकों के ईश्वर के समान शक्ति अथवा वीर्य भी स्वीकार किया है। जैनों ने चतन्य का अर्थ ज्ञान, दर्शन, शक्ति किया है, किन्तु नैयायिक-वैशेषिक मत में मुक्तात्मा में ज्ञान, दर्शन नहीं होते । सांख्य-मत में चित्शक्ति पुरुष में है, फिर भी उसमें ज्ञान नहीं होता; किन्तु द्रष्ट्टत्व होता है । इन सभी मतभेदों का समन्वय असम्भव नहीं है ।
__ जब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि, मुक्तात्मा में प्रानन्द का ज्ञान से पृथक क्या स्वरूप है ? तब यही निष्कर्ष निकलता है कि, अानन्द भी ज्ञान का ही एक पर्याय है । जैनाचार्यों ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। बौद्ध-दार्शनिकों ने भी ज्ञान और सुख को सर्वथा भिन्न नहीं माना है । वेदान्त-मत में भी एक अखण्ड ब्रह्म-तत्त्व में ज्ञान, प्रानन्द, चैतन्य इन सबका वस्तुतः भेद करना अद्वत के विरोध के समान ही है । नयायिक चैतन्य और ज्ञान में भेद का वर्णन करते हैं, परन्तु जब हम यह देखते हैं कि, उन्होंने नित्य मुक्त ईश्वर में नित्य-ज्ञान स्वीकार किया है, तब हमें यह मानना पड़ता हैं कि, वे इस भेद को सर्वथा अभिन्न नहीं रख सके । पुनश्च, मुक्तात्मा चेतन होकर भी ज्ञानहीन हो, तो इस चैतन्य का स्वरूप भी एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। यहाँ यदि हम याज्ञवल्क्य द्वारा मैत्रेयी के प्रति कहे गए इस कथन पर कि, 'न तस्य प्रेत्य संज्ञा अस्ति'-मृत्यूपरान्त उसकी कोई संज्ञा नहीं होती-सूक्ष्म दृष्टि से
चार करें तो इसका समाधान हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है, जिसका नामकरण नहीं किया जा सकता। यदि इसे ज्ञान कहा जाए तो ज्ञान के विषय में साधारण जन का जो विचार है, वही उनके मन में स्थान प्राप्त करेगा, अर्थात् इन्द्रियों अथवा मन के द्वारा होने वाला ज्ञान । परन्तु मुक्तात्मा में इन साधनों का प्रभाव होता है, अतः उसके ज्ञान को ज्ञान कैसे माना जाए? अात्मा स्वयं प्रतिष्ठित है, वह बाहर क्यों देखे ? बहिर्वृत्ति क्यों बने ? और यदि प्रात्मा बहिर्वत्ति नहीं होता तो उसे ज्ञानी कहने की अपेक्षा चैतन्य घन कहना अधिक उपयुक्त है। नैयायिकों ने ज्ञान की व्याख्या इस प्रकार की है :-आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष होता है और फिर इन्द्रिय के साथ तथा उस के द्वारा बाह्य पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है । ज्ञान की इस व्याख्या के अनुसार यह बात स्वाभाविक है कि नैयायिक मुक्तावस्था में ज्ञान की सत्ता न मानें । अर्थात् उनकी ज्ञान की परिभाषा ही भिन्न है। परिभाषा के भेद के कारण तत्त्वों में कुछ भी भेद नहीं पड़ता । अन्यथा नैयायिकों के मत में जड़-पदार्थ और चैतन्य-पदार्थ में क्या भेद रह जाएगा ? अत: यह बात माननी पड़ेगी कि, जड़ से भेद
1. सर्वार्थसिद्धि 10.4.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org