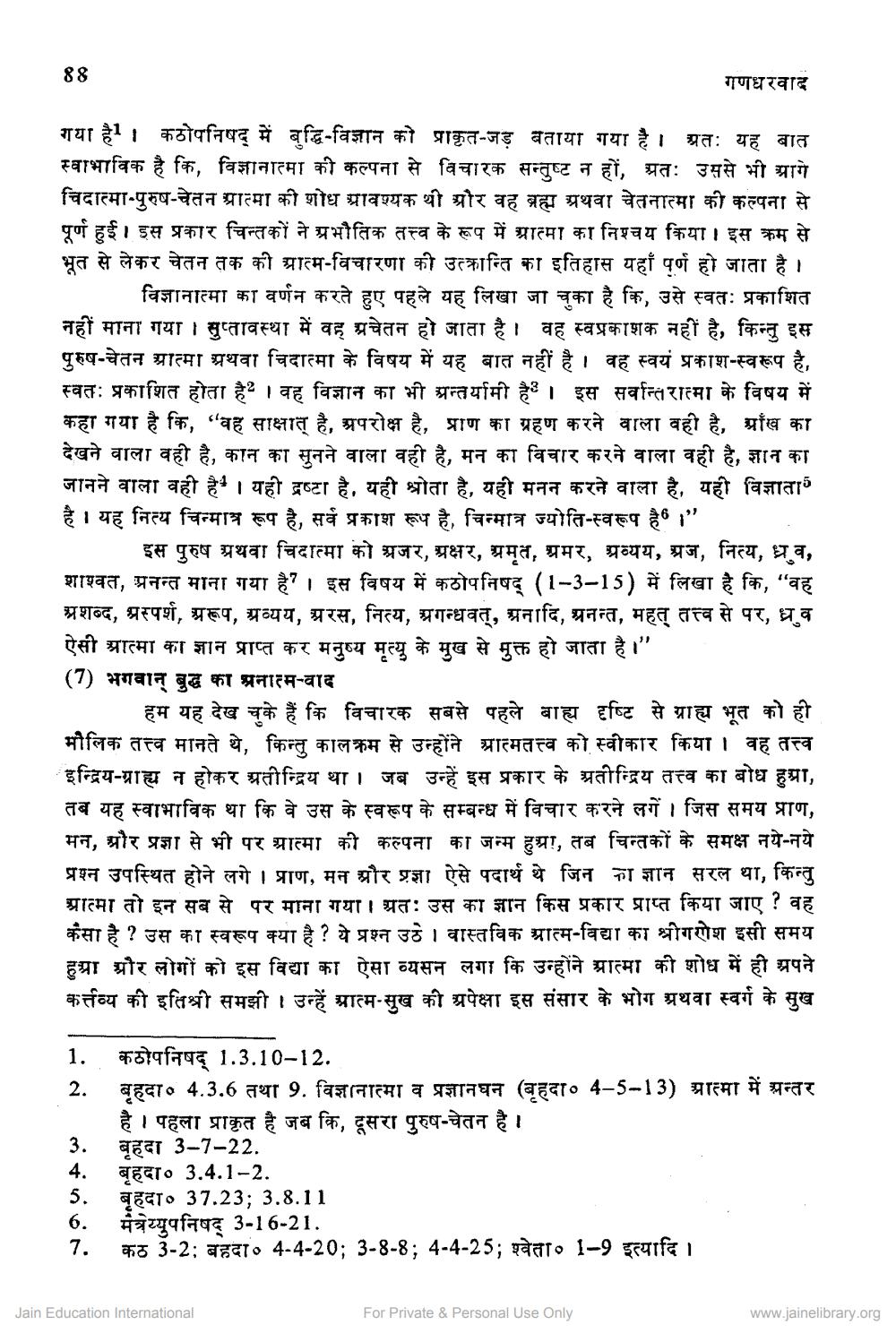________________
88
अतः यह बात
गया है । कठोपनिषद् में बुद्धि-विज्ञान को प्राकृत जड़ बताया गया है । स्वाभाविक है कि, विज्ञानात्मा की कल्पना से विचारक सन्तुष्ट न हों, अतः उससे भी आगे चिदात्मा-पुरुष- चेतन श्रात्मा की शोध प्रावश्यक थी और वह ब्रह्म अथवा चेतनात्मा की कल्पना से पूर्ण हुई। इस प्रकार चिन्तकों ने प्रभौतिक तत्त्व के रूप में ग्रात्मा का निश्चय किया। इस क्रम से भूत से लेकर चेतन तक की ग्रात्म-विचारणा की उत्क्रान्ति का इतिहास यहाँ पूर्ण हो जाता है । विज्ञानात्मा का वर्णन करते हुए पहले यह लिखा जा चुका है कि, उसे स्वतः प्रकाशित नहीं माना गया । सुप्तावस्था में वह प्रचेतन हो जाता है । वह स्वप्रकाशक नहीं है, किन्तु इस पुरुष चेतन आत्मा अथवा चिदात्मा के विषय में यह बात नहीं है । वह स्वयं प्रकाश - स्वरूप है, स्वतः प्रकाशित होता है । वह विज्ञान का भी अन्तर्यामी है । इस सर्वान्तरात्मा के विषय में कहा गया है कि, "वह साक्षात् है, अपरोक्ष है, प्राण का ग्रहण करने वाला वही है, प्राँख का देखने वाला वही है, कान का सुनने वाला वही है, मन का विचार करने वाला वही है, ज्ञान का जानने वाला वही है । यही द्रष्टा है, यही श्रोता है, यही मनन करने वाला है, यही विज्ञाता है | यह नित्य चिन्मात्र रूप है, सर्व प्रकाश रूप है, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप है ।"
इस पुरुष अथवा चिदात्मा को अजर, अक्षर, अमृत, अमर, अव्यय, अज, नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अनन्त माना गया है । इस विषय में कठोपनिषद् ( 1-3-15 ) में लिखा है कि, "वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य, अगन्धवत्, अनादि, अनन्त, महत् तत्त्व से पर, ध्रुव ऐसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है ।" (7) भगवान् बुद्ध का अनात्मवाद
हम यह देख चुके हैं कि विचारक सबसे पहले बाह्य दृष्टि से ग्राह्य भूत को ही मौलिक तत्त्व मानते थे, किन्तु कालक्रम से उन्होंने श्रात्मतत्त्व को स्वीकार किया । वह तत्त्व इन्द्रिय-ग्राह्य न होकर प्रतीन्द्रिय था । जब उन्हें इस प्रकार के प्रतीन्द्रिय तत्त्व का बोध हुआ, तब यह स्वाभाविक था कि वे उस के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करने लगें । जिस समय प्राण, मन, और प्रज्ञा से भी पर श्रात्मा की कल्पना का जन्म हुआ, तब चिन्तकों के समक्ष नये-नये प्रश्न उपस्थित होने लगे । प्राण, मन और प्रज्ञा ऐसे पदार्थ थे जिन का ज्ञान सरल था, किन्तु आत्मा तो इन सब से पर माना गया । अतः उस का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाए ? वह कैसा है ? उस का स्वरूप क्या है ? ये प्रश्न उठे । वास्तविक श्रात्म-विद्या का श्रीगणेश इसी समय हुआ और लोगों को इस विद्या का ऐसा व्यसन लगा कि उन्होंने प्रात्मा की शोध में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझी। उन्हें आत्म सुख की अपेक्षा इस संसार के भोग अथवा स्वर्ग के सुख
1.
2.
गणधरवाद
कठोपनिषद् 1.3.10-12.
बृहदा 4.3.6 तथा 9 विज्ञानात्मा व प्रज्ञानघन (बृहदा० 4-5-13) आत्मा में अन्तर
है । पहला प्राकृत है जब कि, दूसरा पुरुष- चेतन है ।
बृहदा 3-7-22.
बृहदा० 3.4.1-2.
बृहदा० 37.23; 3.8.11
3.
4.
5.
6. मैत्रेय्युपनिषद् 3-16-21.
7.
कठ 3-2 बहदा ० 4-4-20; 3-8-8; 4-4-25; श्वेता० 1-9 इत्यादि ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org