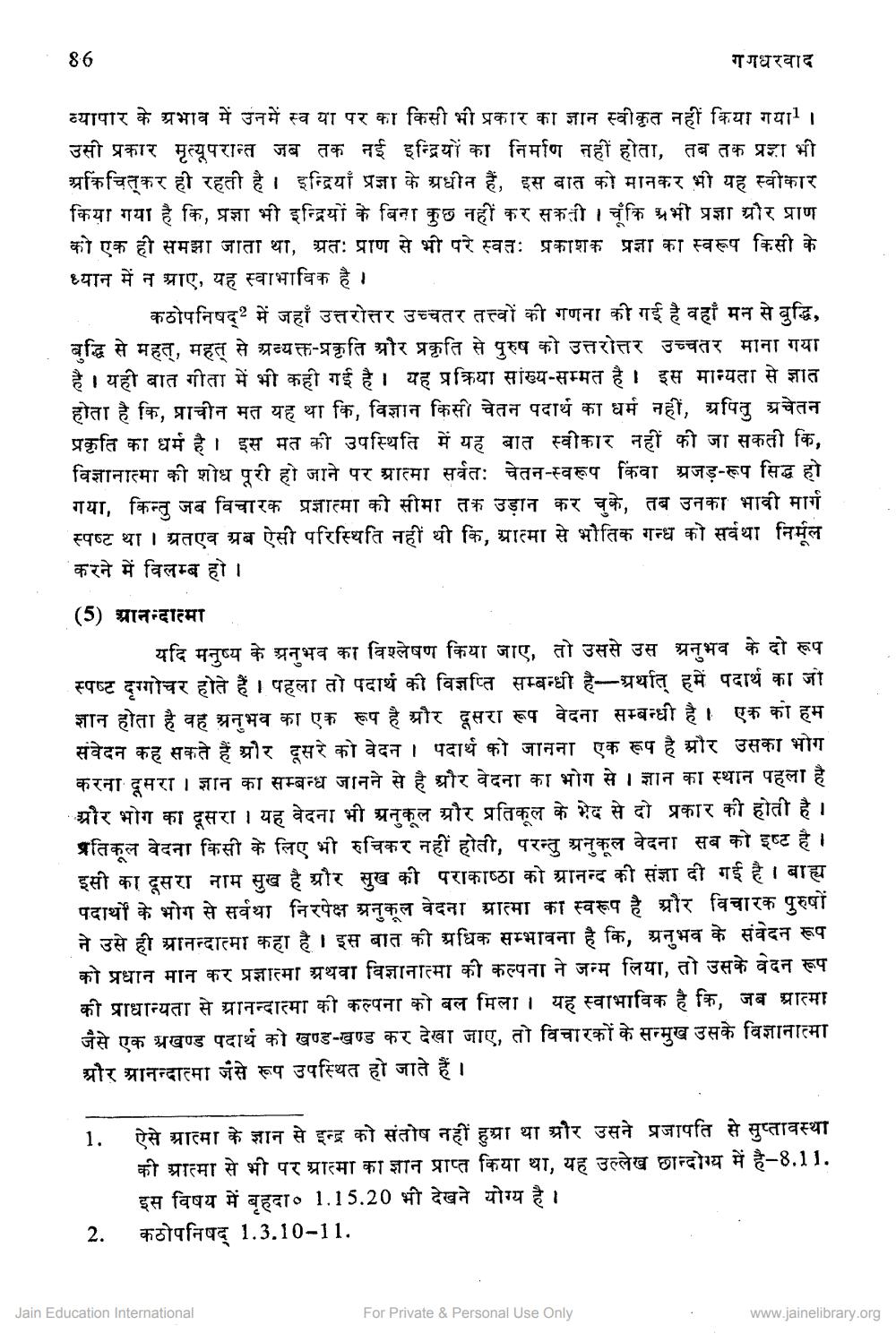________________
86
व्यापार के प्रभाव में उनमें स्व या पर का किसी भी प्रकार का ज्ञान स्वीकृत नहीं किया गया । उसी प्रकार मृत्यूपरान्त जब तक नई इन्द्रियों का निर्माण नहीं होता, तब तक प्रज्ञा भी किचित्कर ही रहती है । इन्द्रियाँ प्रज्ञा के अधीन हैं, इस बात को मानकर भी यह स्वीकार किया गया है कि, प्रज्ञा भी इन्द्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकती । चूँकि अभी प्रज्ञा और प्राण को एक ही समझा जाता था, अतः प्राण से भी परे स्वतः प्रकाशक प्रज्ञा का स्वरूप किसी के ध्यान में न आए, यह स्वाभाविक है ।
कठोपनिषद् में जहाँ उत्तरोत्तर उच्चतर तत्त्वों की गणना की गई है वहाँ मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्, महत् से अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से पुरुष को उत्तरोत्तर उच्चतर माना गया है । यही बात गीता में भी कही गई है । यह प्रक्रिया सांख्य-सम्मत है । इस मान्यता से ज्ञात होता है कि, प्राचीन मत यह था कि, विज्ञान किसी चेतन पदार्थ का धर्म नहीं, अपितु अचेतन प्रकृति का धर्म है । इस मत की उपस्थिति में यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि, विज्ञानात्मा की शोध पूरी हो जाने पर श्रात्मा सर्वत: चेतन स्वरूप किंवा अजड़-रूप सिद्ध हो गया, किन्तु जब विचारक प्रज्ञात्मा की सीमा तक उड़ान कर चुके, तब उनका भावी मार्ग स्पष्ट था । श्रतएव अब ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि, आत्मा से भौतिक गन्ध को सर्वथा निर्मूल करने में विलम्ब हो ।
(5) श्रानन्दात्मा
यदि मनुष्य के अनुभव का विश्लेषण किया जाए, तो उससे उस अनुभव के दो रूप स्पष्ट दृग्गोचर होते हैं। पहला तो पदार्थ की विज्ञप्ति सम्बन्धी है— अर्थात् हमें पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह अनुभव का एक रूप है और दूसरा रूप वेदना सम्बन्धी है ।
एक हम संवेदन कह सकते हैं और दूसरे को वेदन | पदार्थ को जानना एक रूप है और उसका भोग करना दूसरा । ज्ञान का सम्बन्ध जानने से है श्रौर वेदना का भोग से । ज्ञान का स्थान पहला है और भोग का दूसरा । यह वेदना भी अनुकूल और प्रतिकूल के भेद से दो प्रकार की होती है । प्रतिकूल वेदना किसी के लिए भी रुचिकर नहीं होती, परन्तु अनुकूल वेदना सब को इष्ट है । इसी का दूसरा नाम सुख है और सुख की पराकाष्ठा को ग्रानन्द की संज्ञा दी गई है । बाह्य पदार्थों के भोग से सर्वथा निरपेक्ष अनुकूल वेदना आत्मा का स्वरूप है और विचारक पुरुषों ने उसे ही प्रानन्दात्मा कहा है। इस बात की अधिक सम्भावना है कि, अनुभव के संवेदन रूप को प्रधान मान कर प्रज्ञात्मा अथवा विज्ञानात्मा की कल्पना जन्म लिया, तो उसके वेदन रूप की प्राधान्यता से प्रानन्दात्मा की कल्पना को बल मिला। यह स्वाभाविक है कि, जब श्रात्मा जैसे एक अखण्ड पदार्थ को खण्ड-खण्ड कर देखा जाए, तो विचारकों के सन्मुख उसके विज्ञानात्मा और आनन्दात्मा जैसे रूप उपस्थित हो जाते हैं ।
1.
गगधरवाद
2.
ऐसे ग्रात्मा के ज्ञान से इन्द्र को संतोष नहीं हुआ था और उसने प्रजापति से सुप्तावस्था की आत्मा से भी पर श्रात्मा का ज्ञान प्राप्त किया था, यह उल्लेख छान्दोग्य में है - 8.11. इस विषय में बृहदा० 1.15.20 भी देखने योग्य है ।
कठोपनिषद् 1.3.10-11.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org