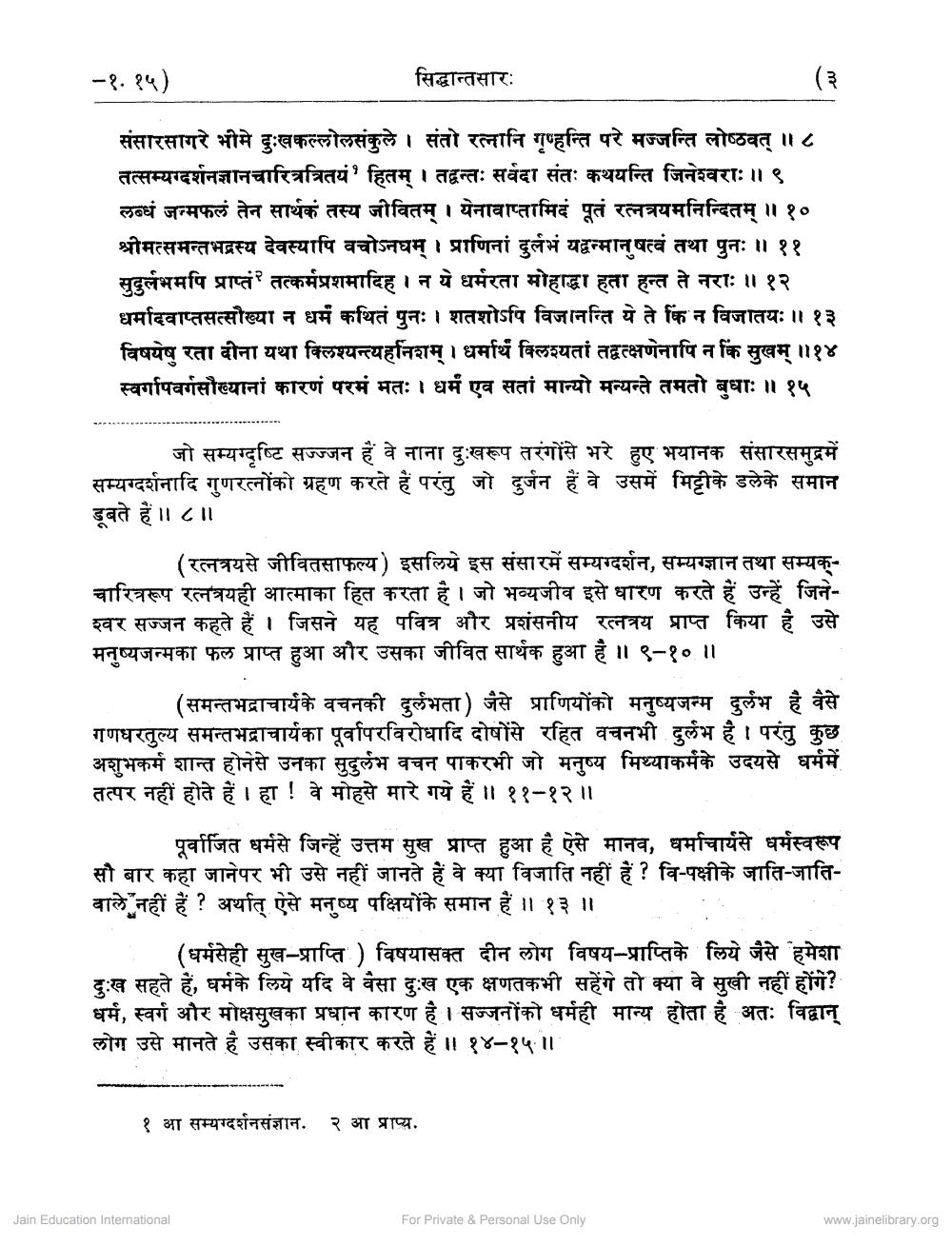________________
- १. १५)
सिद्धान्तसारः
(३
संसारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकुले । संतो रत्नानि गृण्हन्ति परे मज्जन्ति लोष्ठवत् ॥ ८ तत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रितयं हितम् । तद्वन्तः सर्वदा संतः कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ९ लब्धं जन्मफलं तेन सार्थकं तस्य जीवितम् । येनावाप्तामिदं पूतं रत्नत्रयमनिन्दितम् ॥ १० श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघम् । प्राणिनां दुर्लभं यद्वन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥ ११ सुदुर्लभमपि प्राप्तं तत्कर्मप्रशमादिह । न ये धर्मरता मोहाद्धा हता हन्त ते नराः ॥ १२ धर्मादवाप्तसत्सौख्या न धर्मं कथितं पुनः । शतशोऽपि विजानन्ति ये ते किं न विजातयः ॥ १३ विषयेषु रता दीना यथा क्लिश्यन्त्यर्हानशम् । धर्मार्थं क्लिश्यतां तद्वत्क्षणेनापि न कि सुखम् ॥१४ स्वर्गापवर्गसौख्यानां कारणं परमं मतः । धर्मं एव सतां मान्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः ॥ १५
जो सम्यग्दृष्टि सज्ज्जन हैं वे नाना दुःखरूप तरंगोंसे भरे हुए भयानक संसारसमुद्र में सम्यग्दर्शनादि गुणरत्नोंको ग्रहण करते हैं परंतु जो दुर्जन हैं वे उसमें मिट्टीके डलेके समान डूबते हैं ॥ ८ ॥
( रत्नत्रय से जीवितसाफल्य ) इसलिये इस संसारमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयही आत्माका हित करता है । जो भव्यजीव इसे धारण करते हैं उन्हें जिनेश्वर सज्जन कहते हैं । जिसने यह पवित्र और प्रशंसनीय रत्नत्रय प्राप्त किया है उसे मनुष्यजन्मका फल प्राप्त हुआ और उसका जीवित सार्थक हुआ है ॥ ९-१० ॥
(समन्तभद्राचार्यके वचनकी दुर्लभता ) जैसे प्राणियोंको मनुष्यजन्म दुर्लभ है वैसे गणधरतुल्य समन्तभद्राचार्यका पूर्वापरविरोधादि दोषोंसे रहित वचनभी दुर्लभ है । परंतु कुछ अशुभकर्म शान्त होनेसे उनका सुदुर्लभ वचन पाकरभी जो मनुष्य मिथ्याकर्मके उदयसे धर्ममें तत्पर नहीं होते हैं । हा ! वे मोहसे मारे गये हैं ।। ११-१२ ॥
पूर्वार्जित धर्मसे जिन्हें उत्तम सुख प्राप्त हुआ है ऐसे मानव, धर्माचार्य से धर्मस्वरूप सौ बार कहा जानेपर भी उसे नहीं जानते हैं वे क्या विजाति नहीं हैं ? वि-पक्षीके जाति-जातिवाले नहीं हैं ? अर्थात् ऐसे मनुष्य पक्षियोंके समान हैं ॥ १३ ॥
( धर्मसेही सुख - प्राप्ति ) विषयासक्त दीन लोग विषय प्राप्तिके लिये जैसे हमेशा दुःख सहते हैं, धर्मके लिये यदि वे वैसा दुःख एक क्षणतकभी सहेंगे तो क्या वे सुखी नहीं होंगे? धर्म, स्वर्ग और मोक्षसुखका प्रधान कारण है । सज्जनों को धर्मही मान्य होता है अतः विद्वान् लोग उसे मानते है उसका स्वीकार करते हैं ।। १४-१५ ।।
१ आ सम्यग्दर्शनसंज्ञान. २ आ प्राप्य.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org