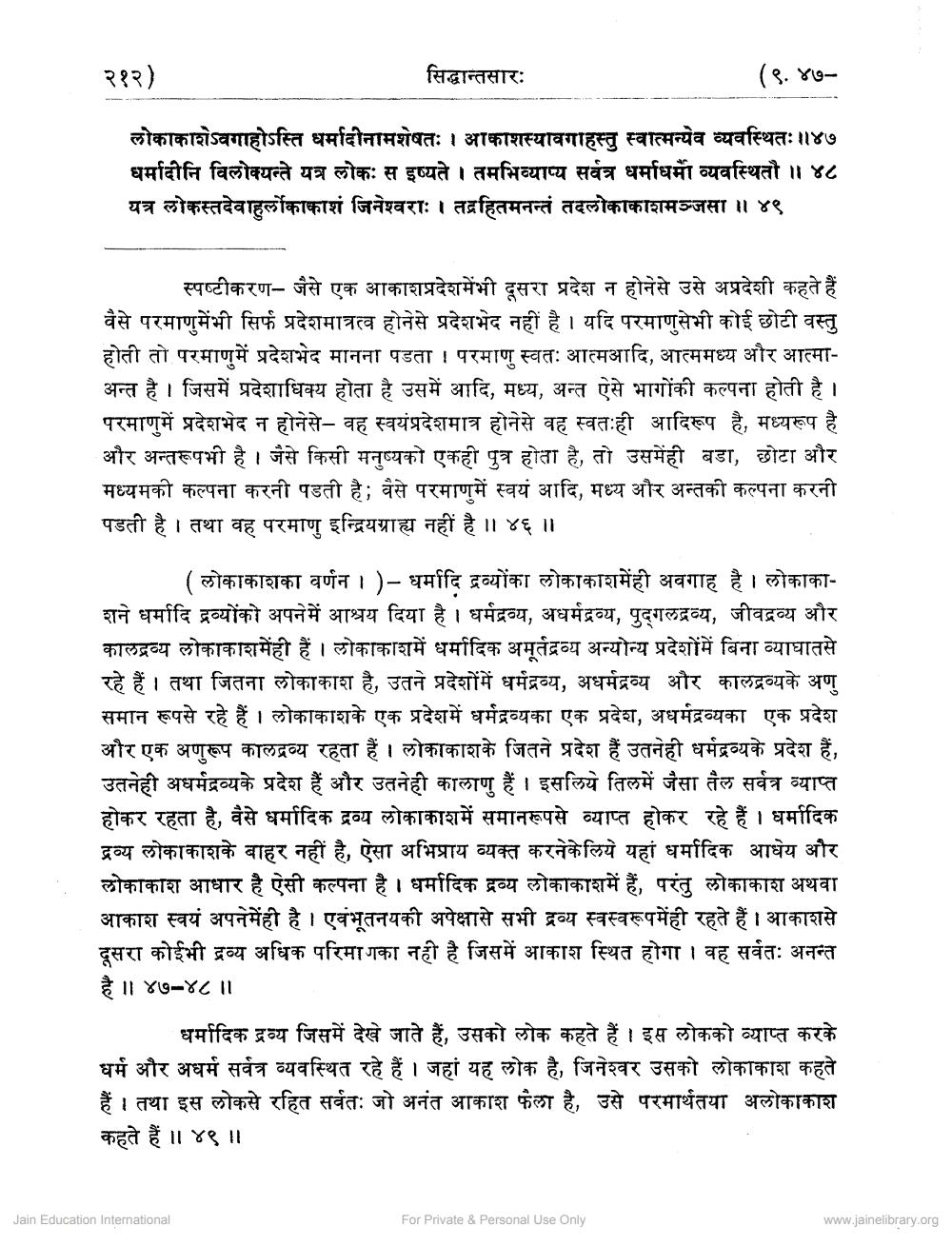________________
२१२)
सिद्धान्तसारः
(९. ४७
लोकाकाशेऽवगाहोऽस्ति धर्मादीनामशेषतः । आकाशस्यावगाहस्तु स्वात्मन्येव व्यवस्थितः॥४७ धर्मादीनि विलोक्यन्ते यत्र लोकः स इष्यते । तमभिव्याप्य सर्वत्र धर्माधर्मी व्यवस्थितौ ॥ ४८ यत्र लोकस्तदेवाहुलॊकाकाशं जिनेश्वराः । तद्रहितमनन्तं तदलोकाकाशमञ्जसा ॥ ४९
___ स्पष्टीकरण- जैसे एक आकाशप्रदेशमेंभी दूसरा प्रदेश न होनेसे उसे अप्रदेशी कहते हैं वैसे परमाणुमेंभी सिर्फ प्रदेशमात्रत्व होनेसे प्रदेशभेद नहीं है । यदि परमाणुसेभी कोई छोटी वस्तु होती तो परमाणु में प्रदेशभेद मानना पडता । परमाणु स्वतः आत्मआदि, आत्ममध्य और आत्माअन्त है। जिसमें प्रदेशाधिक्य होता है उसमें आदि, मध्य, अन्त ऐसे भागोंकी कल्पना होती है। परमाणुमें प्रदेशभेद न होनेसे- वह स्वयंप्रदेशमात्र होनेसे वह स्वतःही आदिरूप है, मध्यरूप है और अन्तरूपभी है । जैसे किसी मनुष्यको एकही पुत्र होता है, तो उसमेंही बडा, छोटा और मध्यमकी कल्पना करनी पडती है। वैसे परमाणुमें स्वयं आदि, मध्य और अन्तकी कल्पना करनी पडती है। तथा वह परमाण इन्द्रियग्राह्य नहीं है ।। ४६ ।।
( लोकाकाशका वर्णन । )- धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाशमेंही अवगाह है । लोकाकाशने धर्मादि द्रव्योंको अपने में आश्रय दिया है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य और कालद्रव्य लोकाकाशमेंही हैं । लोकाकाशमें धर्मादिक अमूर्तद्रव्य अन्योन्य प्रदेशोंमें बिना व्याघातसे रहे हैं। तथा जितना लोकाकाश है, उतने प्रदेशोंमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्यके अणु समान रूपसे रहे हैं । लोकाकाशके एक प्रदेशमें धर्मद्रव्यका एक प्रदेश, अधर्मद्रव्यका एक प्रदेश और एक अणुरूप कालद्रव्य रहता हैं । लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतनेही धर्मद्रव्यके प्रदेश हैं, उतनेही अधर्मद्रव्यके प्रदेश हैं और उतनेही कालाणु हैं । इसलिये तिलमें जैसा तैल सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है, वैसे धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमें समानरूपसे व्याप्त होकर रहे हैं । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये यहां धर्मादिक आधेय और लोकाकाश आधार है ऐसी कल्पना है । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमें हैं, परंतु लोकाकाश अथवा आकाश स्वयं अपनेमेंही है । एवंभूतनयकी अपेक्षासे सभी द्रव्य स्वस्वरूपमेंही रहते हैं । आकाशसे दूसरा कोईभी द्रव्य अधिक परिमागका नही है जिसमें आकाश स्थित होगा । वह सर्वतः अनन्त है ॥ ४७-४८॥
धर्मादिक द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं, उसको लोक कहते हैं । इस लोकको व्याप्त करके धर्म और अधर्म सर्वत्र व्यवस्थित रहे हैं । जहां यह लोक है, जिनेश्वर उसको लोकाकाश कहते हैं । तथा इस लोकसे रहित सर्वतः जो अनंत आकाश फैला है, उसे परमार्थतया अलोकाकाश कहते हैं ।। ४९ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org