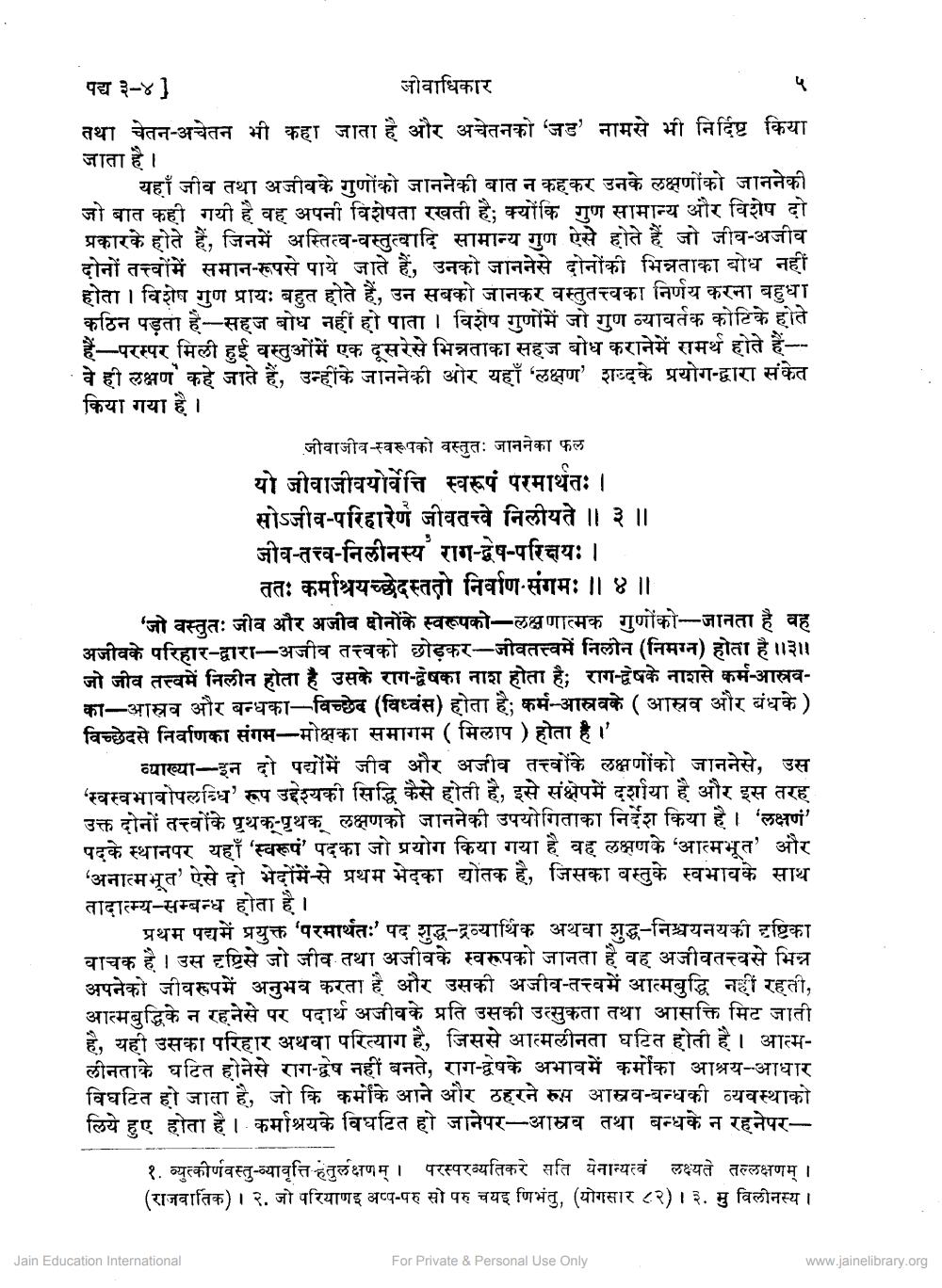________________
पद्य ३-४ ]
जीवाधिकार
तथा चेतन-अचेतन भी कहा जाता है और अचेतनको 'जड' नामसे भी निर्दिष्ट किया जाता है।
यहाँ जीव तथा अजीवके गुणोंको जानने की बात न कहकर उनके लक्षणोंको जाननेकी जो बात कही गयी है वह अपनी विशेषता रखती है; क्योंकि गुण सामान्य और विशेष दो प्रकारके होते हैं, जिनमें अस्तित्व-वस्तुत्वादि सामान्य गुण ऐसे होते हैं जो जीव-अजीव दोनों तत्त्वोंमें समान रूपसे पाये जाते हैं, उनको जाननेसे दोनोंकी भिन्नताका बोध नहीं होता । विशेष गुण प्रायः बहुत होते हैं, उन सबको जानकर वस्तुतत्त्वका निर्णय करना बहुधा कठिन पड़ता है - सहज बोध नहीं हो पाता । विशेष गुणोंमें जो गुण व्यावर्तक कोटिके होते हैं - परस्पर मिली हुई वस्तुओं में एक दूसरे से भिन्नताका सहज बोध करानेमें रामर्थ होते हैं-ही लक्षण' कहे जाते हैं, उन्हींके जानने की ओर यहाँ 'लक्षण' शब्दके प्रयोग द्वारा संकेत किया गया है ।
जीवाजीव-स्वरूपको वस्तुतः जाननेका फल यो जीवाजीवयोर्वेत्ति स्वरूपं परमार्थतः । सोऽजीव - परिहारेण जीवतत्त्वे निलीयते ॥ ३॥ ata-तव-निलीनस्य राग-द्वेष- परिक्षयः । ततः कर्माश्रयच्छेदस्ततो निर्वाण - संगमः ॥ ४ ॥
'जो वस्तुतः जीव और अजीव दोनोंके स्वरूपको - लक्षणात्मक गुणोंको-जानता है वह अजीवके परिहार-द्वारा- अजीव तत्त्वको छोड़कर - जीवतत्त्वमें निलोन (निमग्न) होता है ॥३॥ जो जीव तत्वमें निलीन होता है उसके राग-द्वेषका नाश होता है; राग-द्वेषके नाशसे कर्म - आस्रवका - आस्रव और बन्धका - विच्छेद ( विध्वंस) होता है; कर्म-आस्रवके ( आस्रव और बंधके ) विच्छेद से निर्वाणका संगम - मोक्षका समागम ( मिलाप ) होता है ।'
व्याख्या- इन दो पद्योंमें जीव और अजीव तत्त्वोंके लक्षणोंको जाननेसे, उस 'स्वस्वभावोपलब्धि' रूप उद्देश्यकी सिद्धि कैसे होती है, इसे संक्षेपमें दर्शाया है और इस तरह उक्त दोनों तत्त्वोंके पृथक-पृथक लक्षणको जाननेकी उपयोगिताका निर्देश किया है। 'लक्षणं' पदके स्थानपर यहाँ 'स्वरूपं' पदका जो प्रयोग किया गया है वह लक्षण के 'आत्मभूत' और 'अनात्मभूत' ऐसे दो भेदोंमें से प्रथम भेदका द्योतक है, जिसका वस्तुके स्वभाव के साथ तादात्म्य - सम्बन्ध होता है ।
प्रथम पद्य में प्रयुक्त 'परमार्थतः ' पद शुद्ध-द्रव्यार्थिक अथवा शुद्ध-निश्चयन की दृष्टिका वाचक है । उस दृष्टिसे जो जीव तथा अजीवके स्वरूपको जानता है वह अजीवतत्त्वसे भिन्न अपनेको जीवरूपमें अनुभव करता है और उसकी अजीव तत्त्वमें आत्मबुद्धि नहीं रहती, आत्मबुद्धि न रहने से पर पदार्थ अजीव के प्रति उसकी उत्सुकता तथा आसक्ति मिट जाती है, यही उसका परिहार अथवा परित्याग है, जिससे आत्मलीनता घटित होती है । आत्मलीनता घटित होनेसे राग-द्वेष नहीं बनते, राग-द्वेषके अभाव में कर्मोका आश्रय-आधार विघटित हो जाता है, जो कि कर्मोंके आने और ठहरने रूम आस्रव बन्धकी व्यवस्थाको लिये 'हुए होता है। कर्माश्रयके विघटित हो जानेपर - आम्रव तथा बन्धके न रहनेपर
१. व्युत्कीर्ण वस्तु - व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम् । परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम् । (राजवार्तिक) । २. जो परियाणइ अप्प पर सो परु चयइ णिभंतु, (योगसार ८२ ) । ३. मु विलीनस्य ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org