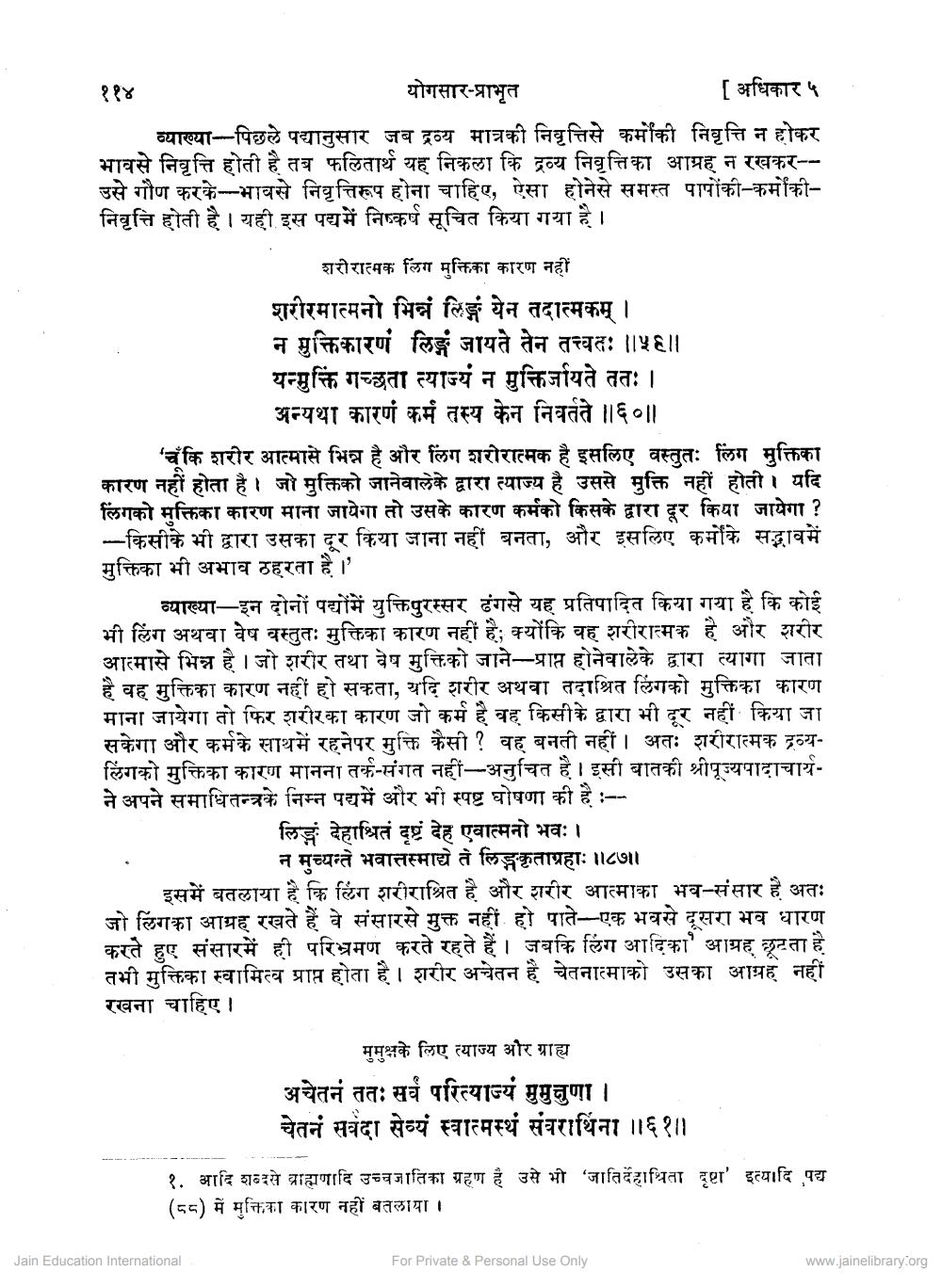________________
योगसार-प्राभृत
[ अधिकार ५ व्याख्या-पिछले पद्यानुसार जब द्रव्य मात्रकी निवृत्तिसे कर्मोकी निवृत्ति न होकर भावसे निवृत्ति होती है तब फलितार्थ यह निकला कि द्रव्य निवृत्ति का आग्रह न रखकर-- उसे गौण करके-भावसे निवृत्तिरूप होना चाहिए, ऐसा होनेसे समस्त पापोंकी-कर्मोकीनिवृत्ति होती है। यही इस पद्य में निष्कर्ष सूचित किया गया है।
शरीरात्मक लिंग मुक्तिका कारण नहीं शरीरमात्मनो भिन्न लिङ्गं येन तदात्मकम् । न मुक्तिकारणं लिङ्ग जायते तेन तत्त्वतः ॥५६।। यन्मुक्तिं गच्छता त्याज्यं न मुक्तिर्जायते ततः ।
अन्यथा कारणं कर्म तस्य केन निवर्तते ॥६०॥ 'चंकि शरीर आत्मासे भिन्न है और लिंग शरीरात्मक है इसलिए वस्तुतः लिंग मुक्तिका कारण नहीं होता है। जो मुक्तिको जानेवालेके द्वारा त्याज्य है उससे मुक्ति नहीं होती। यदि लिंगको मुक्तिका कारण माना जायेगा तो उसके कारण कर्मको किसके द्वारा दूर किया जायेगा ?
-किसीके भी द्वारा उसका दूर किया जाना नहीं बनता, और इसलिए कर्मोंके सद्भावमें मुक्तिका भी अभाव ठहरता है।'
व्याख्या-इन दोनों पद्योंमें युक्तिपुरस्सर ढंगसे यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी लिंग अथवा वेष वस्तुतः मुक्तिका कारण नहीं है क्योंकि वह शरीरात्मक है और शरीर आत्मासे भिन्न है । जो शरीर तथा वेष मुक्तिको जाने-प्राप्त होनेवालेके द्वारा त्यागा जाता है वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता, यदि शरीर अथवा तदाश्रित लिंगको मुक्तिका कारण माना जायेगा तो फिर शरीरका कारण जो कर्म है वह किसीके द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकेगा और कर्म के साथमें रहनेपर मुक्ति कैसी ? वह बनती नहीं। अतः शरीरात्मक द्रव्यलिंगको मुक्तिका कारण मानना तर्क-संगत नहीं-अनुचित है। इसी बातकी श्रीपूज्यपादाचार्यने अपने समाधितन्त्रके निम्न पद्यमें और भी स्पष्ट घोषणा की है :--
लिङ्गं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः ।
न मुच्यन्ते भवात्तस्माद्ये ते लिङ्गकृताग्रहाः ॥८७॥ इसमें बतलाया है कि लिंग शरीराश्रित है और शरीर आत्माका भव-संसार है अतः जो लिंगका आग्रह रखते हैं वे संसारसे मुक्त नहीं हो पाते-एक भवसे दूसरा भव धारण करते हुए संसारमें ही परिभ्रमण करते रहते हैं। जबकि लिंग आदिका' आग्रह छूटता है तभी मुक्तिका स्वामित्व प्राप्त होता है। शरीर अचेतन है चेतनात्माको उसका आग्रह नहीं रखना चाहिए।
मुमुक्षके लिए त्याज्य और ग्राह्य अचेतनं ततः सर्व परित्याज्यं मुमुक्षुणा । चेतनं सर्वदा सेव्यं स्वात्मस्थं संवरार्थिना ॥६१।।
१. आदि शब्दसे ब्राह्मणादि उच्चजातिका ग्रहण है उसे भी 'जातिदेहाथिता दृष्टा' इत्यादि पद्य (८८) में मुक्तिका कारण नहीं बतलाया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org