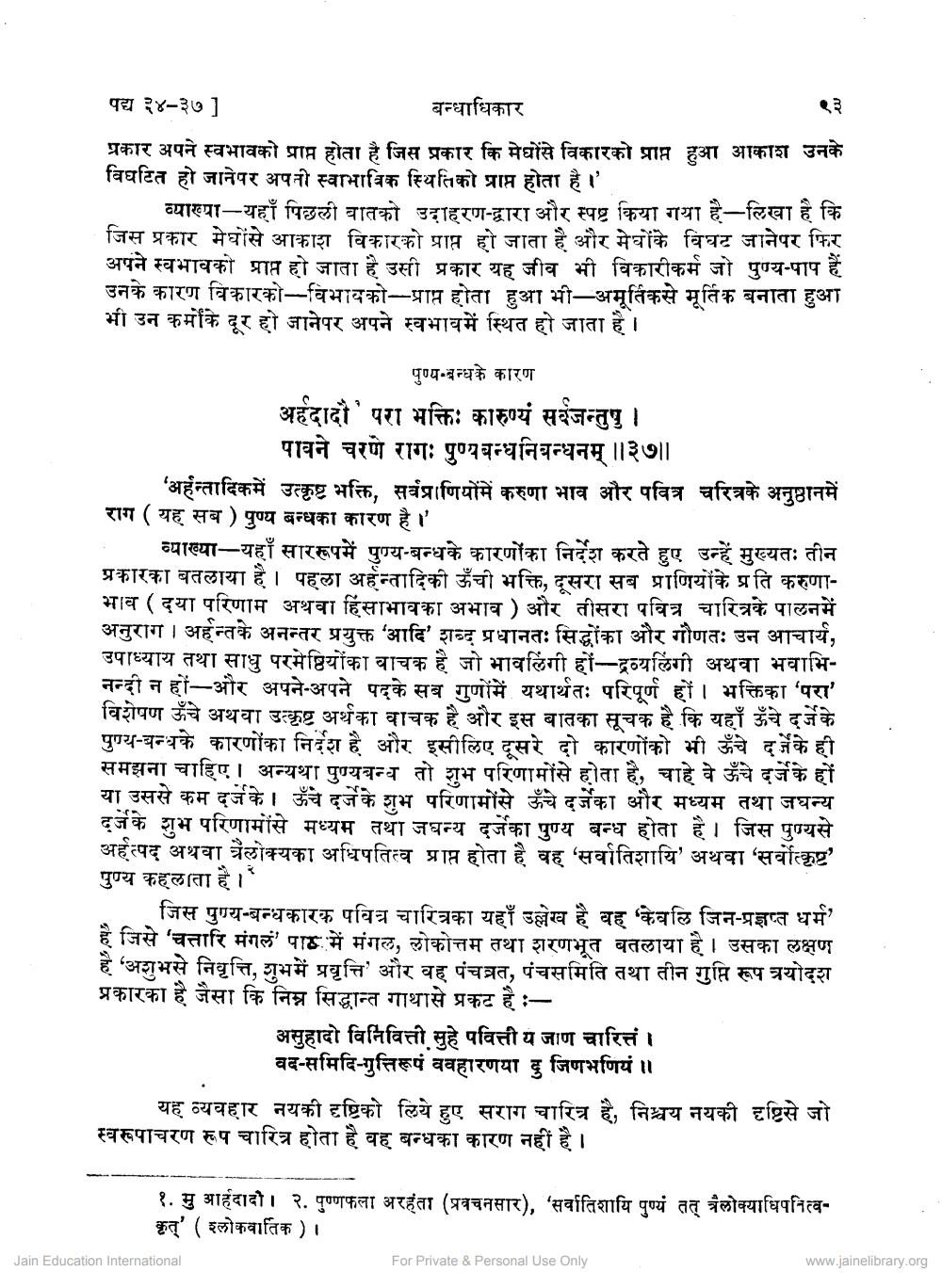________________
पद्य ३४-३७ ]
बन्धाधिकार
९३
प्रकार अपने स्वभावको प्राप्त होता है जिस प्रकार कि मेघोंसे विकारको प्राप्त हुआ आकाश उनके विघटित हो जाने पर अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त होता है ।'
व्याख्या - यहाँ पिछली बातको उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया गया है- लिखा है कि जिस प्रकार मेघोंसे आकाश विकारको प्राप्त हो जाता है और मेवोंके विघट जानेपर फिर अपने स्वभावको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार यह जीव भी विकारीकर्म जो पुण्य-पाप हैं। उनके कारण विकारको -विभावको प्राप्त होता हुआ भी— अमूर्तिकसे मूर्तिक बनाता हुआ भी उन कर्मोंके दूर हो जानेपर अपने स्वभावमें स्थित हो जाता है ।
पुण्य-बन्धके कारण
अर्हदाद' परा भक्तिः कारुण्यं सर्वजन्तुषु । पावने चरणे रागः पुण्यबन्धनिबन्धनम् ||३७||
'अर्हन्तादिकमें उत्कृष्ट भक्ति, सर्वप्राणियों में करुणा भाव और पवित्र चरित्रके अनुष्ठानमें राग ( यह सब ) पुण्य बन्धका कारण है ।'
व्याख्या– यहाँ साररूपमें पुण्य बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए उन्हें मुख्यतः तीन प्रकारका बतलाया है। पहला अर्हन्तादिकी ऊँची भक्ति, दूसरा सब प्राणियों के प्रति करुणाभाव (दया परिणाम अथवा हिंसाभावका अभाव ) और तीसरा पवित्र चारित्रके पालनमें अनुराग | अर्हन्तके अनन्तर प्रयुक्त 'आदि' शब्द प्रधानतः सिद्धोंका और गौणतः उन आचार्य, उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठियोंका वाचक है जो भावलिंगी हों - द्रव्यलिंगी अथवा भवाभिनन्दी न हों - और अपने-अपने पदके सब गुणोंमें यथार्थतः परिपूर्ण हों । भक्तिका 'परा' विशेषण ऊँचे अथवा उत्कृष्ट अर्थका वाचक है और इस बातका सूचक है कि यहाँ ऊँचे दर्जे के पुण्य-बन्धके कारणोंका निर्देश है और इसीलिए दूसरे दो कारणोंको भी ऊँचे दर्जे के ही समझना चाहिए । अन्यथा पुण्यवन्व तो शुभ परिणामोंसे होता है, चाहे वे ऊँचे दर्जे के हों या उससे कम दर्ज के । ऊँचे दर्जे के शुभ परिणामोंसे ऊँचे दर्जेका और मध्यम तथा जघन्य दर्जे के शुभ परिणामोंसे मध्यम तथा जघन्य दर्जेका पुण्य बन्ध होता है । जिस पुण्यसे अर्हत्पद अथवा त्रैलोक्यका अधिपतित्व प्राप्त होता है वह 'सर्वातिशायि' अथवा 'सर्वोत्कृष्ट' पुण्य कहलाता है।
जिस पुण्य-बन्धकारक पवित्र चारित्रका यहाँ उल्लेख है वह 'केवलि जिन- प्रज्ञप्त धर्म' है जिसे ' चत्तारि मंगलं' पाठ में मंगल, लोकोत्तम तथा शरणभूत बतलाया है । उसका लक्षण • 'अशुभसे निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति' और वह पंचत्रत, पंचसमिति तथा तीन गुप्ति रूप त्रयोदश प्रकारका है जैसा कि निम्न सिद्धान्त गाथासे प्रकट है।
:
असुहादो विनिवित्ती सुहे पवित्तीय जाण चारितं । वद समिदि-गुत्तिरूपं ववहारणया दु जिणभणियं ॥
यह व्यवहार नयकी दृष्टिको लिये हुए सराग चारित्र है, निश्चय नयकी दृष्टिसे जो स्वरूपाचरण रूप चारित्र होता है वह बन्धका कारण नहीं है ।
Jain Education International
१. मु आदादौ । २. पुण्णफला अरता ( प्रवचनसार), 'सर्वातिशायि पुण्यं तत् त्रैलोक्याधिपतित्वकृत् ' ( श्लोकवार्तिक ) ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org