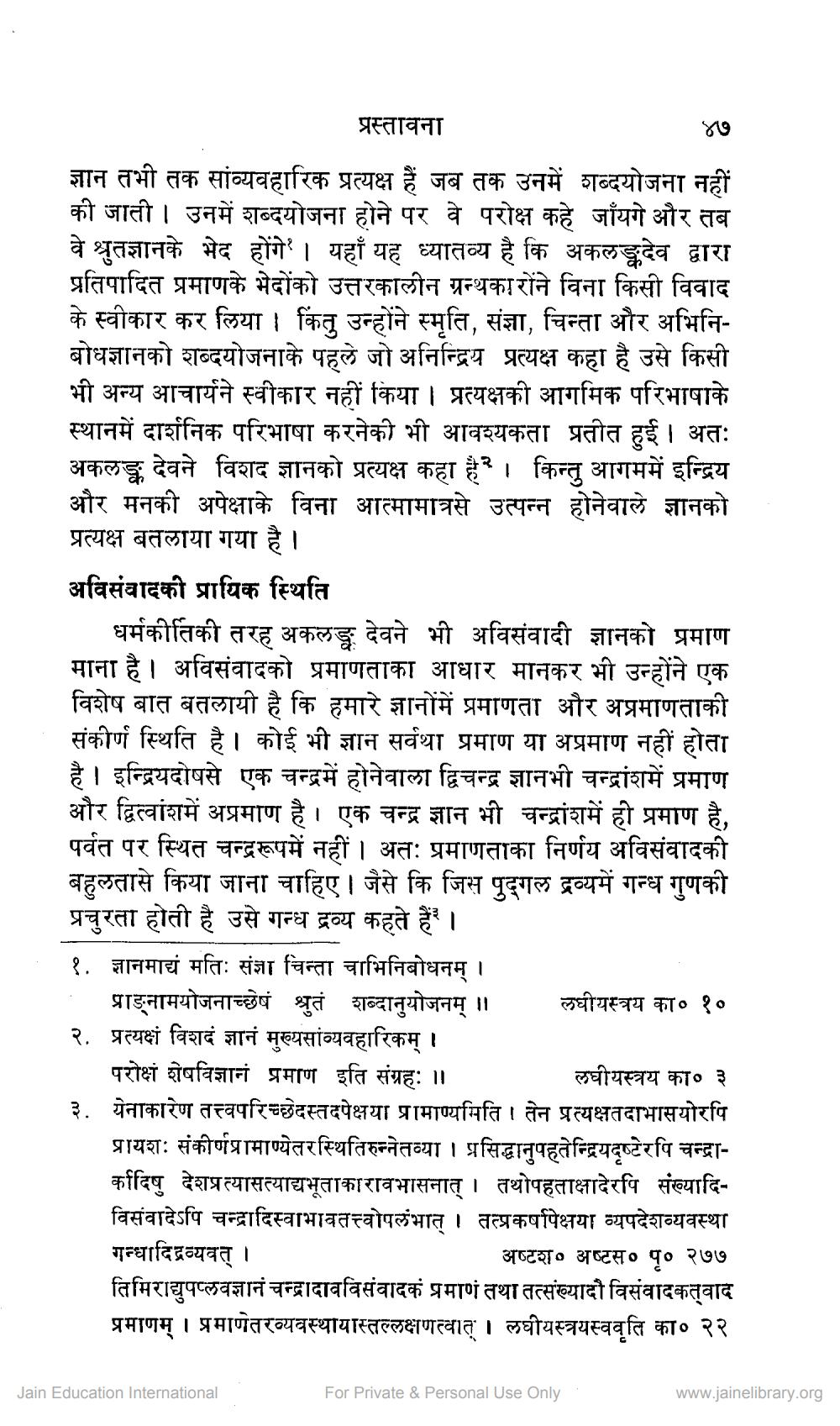________________
प्रस्तावना
४७
ज्ञान तभी तक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं जब तक उनमें शब्दयोजना नहीं की जाती। उनमें शब्दयोजना होने पर वे परोक्ष कहे जाँयगे और तब वे श्रुतज्ञानके भेद होंगे। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अकलङ्कदेव द्वारा प्रतिपादित प्रमाणके भेदोंको उत्तरकालीन ग्रन्थकारोंने विना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया। किंतु उन्होंने स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोधज्ञानको शब्दयोजनाके पहले जो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है उसे किसी भी अन्य आचार्यने स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्षकी आगमिक परिभाषाके स्थानमें दार्शनिक परिभाषा करनेकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः अकलङ्क देवने विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है। किन्तु आगममें इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाके विना आत्मामात्रसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष बतलाया गया है। अविसंवादकी प्रायिक स्थिति
धर्मकीर्तिकी तरह अकलङ्क देवने भी अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण माना है। अविसंवादको प्रमाणताका आधार मानकर भी उन्होंने एक विशेष बात बतलायी है कि हमारे ज्ञानोंमें प्रमाणता और अप्रमाणताकी संकीर्ण स्थिति है। कोई भी ज्ञान सर्वथा प्रमाण या अप्रमाण नहीं होता है। इन्द्रियदोषसे एक चन्द्रमें होनेवाला द्विचन्द्र ज्ञानभी चन्द्रांशमें प्रमाण और द्वित्वांशमें अप्रमाण है। एक चन्द्र ज्ञान भी चन्द्रांशमें ही प्रमाण है, पर्वत पर स्थित चन्द्ररूपमें नहीं। अतः प्रमाणताका निर्णय अविसंवादकी बहुलतासे किया जाना चाहिए। जैसे कि जिस पुद्गल द्रव्यमें गन्ध गुणकी प्रचुरता होती है उसे गन्ध द्रव्य कहते हैं। १. ज्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम् ।
प्राङ्नामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनम् ॥ लघीयस्त्रय का० १० २. प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसांव्यवहारिकम् । परोक्ष शेषविज्ञानं प्रमाण इति संग्रहः ॥
लघीयस्त्रय का० ३ ३. येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदस्तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभासयोरपि
प्रायशः संकीर्णप्रामाण्येतरस्थितिरुन्नेतव्या । प्रसिद्धानुपहतेन्द्रियदृष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्याद्यभूताकारावभासनात् । तथोपहताक्षादेरपि संख्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वाभावतत्त्वोपलंभात् । तत्प्रकर्षापेक्षया व्यपदेशव्यवस्था गन्धादिद्रव्यवत् ।
अष्टश० अष्टस० पृ० २७७ तिमिराद्युपप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकं प्रमाणं तथा तत्संख्यादौ विसंवादकत्वाद प्रमाणम् । प्रमाणेतरव्यवस्थायास्तल्लक्षणत्वात् । लघीयस्त्रयस्ववृति का० २२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org