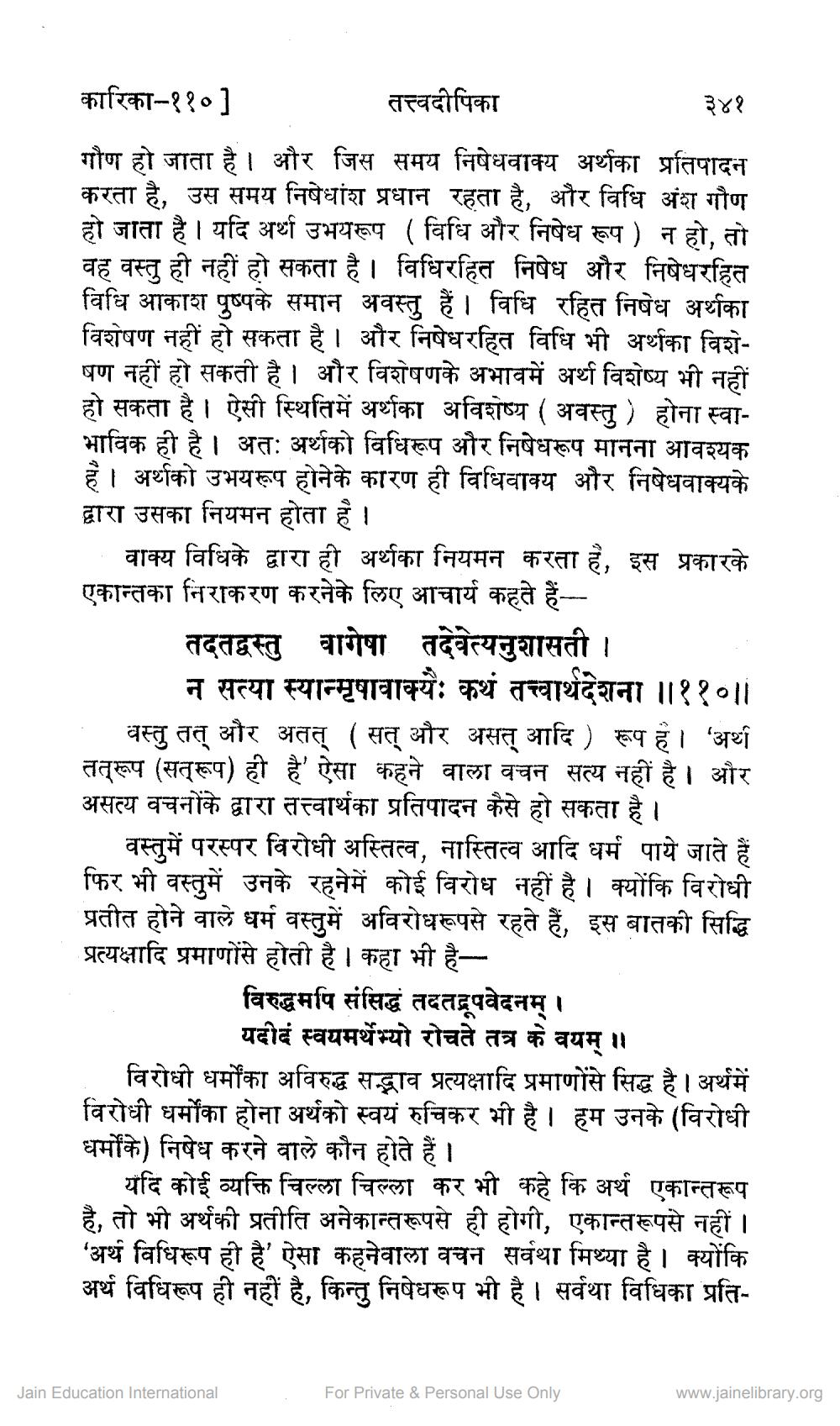________________
कारिका - ११०]
तत्त्वदीपिका
३४१
I
गौण हो जाता है । और जिस समय निषेधवाक्य अर्थका प्रतिपादन करता है, उस समय निषेधांश प्रधान रहता है, और विधि अंश गौण हो जाता है । यदि अर्थ उभयरूप ( विधि और निषेध रूप ) न हो, तो वह वस्तु ही नहीं हो सकता है । विधिरहित निषेध और निषेधरहित विधि आकाश पुष्पके समान अवस्तु हैं । विधि रहित निषेध अर्थका विशेषण नहीं हो सकता है । और निषेधरहित विधि भी अर्थका विशेषण नहीं हो सकती है । और विशेषणके अभाव में अर्थ विशेष्य भी नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में अर्थका अविशेष्य ( अवस्तु ) होना स्वाभाविक ही है । अतः अर्थको विधिरूप और निषेधरूप मानना आवश्यक है । अर्थको उभयरूप होनेके कारण ही विधिवाक्य और निषेधवाक्यके द्वारा उसका नियमन होता है ।
वाक्य विधिके द्वारा ही अर्थका नियमन करता है, इस प्रकारके एकान्तका निराकरण करनेके लिए आचार्य कहते हैं
तदतद्वस्तु वागेषा तदेवेत्यनुशासती ।
न सत्या स्यान्मृषावाक्यैः कथं तत्त्वार्थदेशना ॥ ११० ॥
वस्तु तत् और अतत् ( सत् और असत् आदि ) रूप है । 'अर्थ तत्रूप ( सत्रूप) ही है' ऐसा कहने वाला वचन सत्य नहीं है । और असत्य वचनोंके द्वारा तत्त्वार्थका प्रतिपादन कैसे हो सकता है ।
वस्तु परस्पर विरोधी अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्म पाये जाते हैं फिर भी वस्तुमें उनके रहनेमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म वस्तुमें अविरोधरूपसे रहते हैं, इस बातकी सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे होती है । कहा भी है
विरुद्धमपि संसिद्धं तदतद्रूपवेदनम् ।
यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् 11
I
विरोधी धर्मोंका अविरुद्ध सद्भाव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है | अर्थ में विरोधी धर्मोका होना अर्थको स्वयं रुचिकर भी है। हम उनके ( विरोधी धर्मोके) निषेध करने वाले कौन होते हैं ।
यदि कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर भी कहे कि अर्थ एकान्तरूप है, तो भी अर्थ की प्रतीति अनेकान्तरूपसे ही होगी, एकान्तरूपसे नहीं | 'अर्थ विधिरूप ही है' ऐसा कहनेवाला वचन सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि अर्थ विधिरूप ही नहीं है, किन्तु निषेधरूप भी है । सर्वथा विधिका प्रति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org