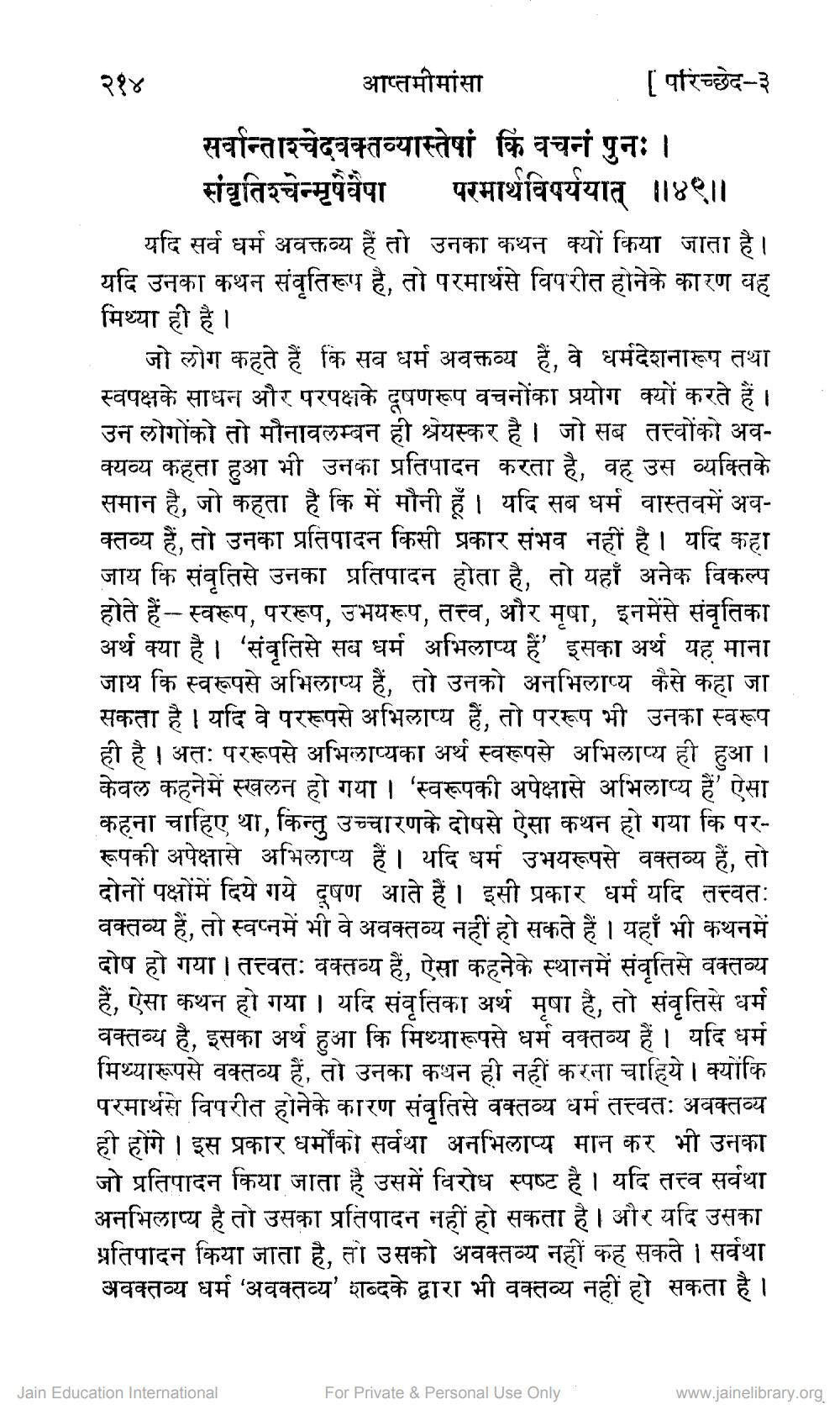________________
२१४ आप्तमीमांसा
[परिच्छेद-३ सर्वान्ताश्चेदवक्तव्यास्तेषां कि वचनं पुनः ।
संवृतिश्चेन्मृवैपा परमार्थविपर्ययात् ॥४९॥ यदि सर्व धर्म अवक्तव्य हैं तो उनका कथन क्यों किया जाता है। यदि उनका कथन संवृतिरूप है, तो परमार्थसे विपरीत होनेके कारण वह मिथ्या ही है।
जो लोग कहते हैं कि सब धर्म अवक्तव्य हैं, वे धर्मदेशनारूप तथा स्वपक्षके साधन और परपक्षके दूषणरूप वचनोंका प्रयोग क्यों करते हैं। उन लोगोंको तो मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर है। जो सब तत्त्वोंको अवक्यव्य कहता हुआ भी उनका प्रतिपादन करता है, वह उस व्यक्तिके समान है, जो कहता है कि में मौनी हूँ। यदि सब धर्म वास्तवमें अवक्तव्य हैं, तो उनका प्रतिपादन किसी प्रकार संभव नहीं है। यदि कहा जाय कि संवृतिसे उनका प्रतिपादन होता है, तो यहाँ अनेक विकल्प होते हैं- स्वरूप, पररूप, उभयरूप, तत्त्व, और मृषा, इनमेंसे संवृतिका अर्थ क्या है। 'संवृतिसे सब धर्म अभिलाप्य हैं' इसका अर्थ यह माना जाय कि स्वरूपसे अभिलाप्य हैं, तो उनको अनभिलाप्य कैसे कहा जा सकता है । यदि वे पररूपसे अभिलाप्य हैं, तो पररूप भी उनका स्वरूप ही है। अत: पररूपसे अभिलाप्यका अर्थ स्वरूपसे अभिलाप्य ही हआ। केवल कहने में स्खलन हो गया। 'स्वरूपकी अपेक्षासे अभिलाप्य हैं' ऐसा कहना चाहिए था, किन्तु उच्चारणके दोषसे ऐसा कथन हो गया कि पररूपकी अपेक्षासे अभिलाप्य हैं। यदि धर्म उभयरूपसे वक्तव्य हैं, तो दोनों पक्षोंमें दिये गये दूषण आते हैं। इसी प्रकार धर्म यदि तत्त्वतः वक्तव्य हैं, तो स्वप्नमें भी वे अवक्तव्य नहीं हो सकते हैं । यहाँ भी कथनमें दोष हो गया। तत्त्वतः वक्तव्य हैं, ऐसा कहनेके स्थानमें संवृतिसे वक्तव्य हैं, ऐसा कथन हो गया। यदि संवृतिका अर्थ मषा है, तो संवृतिसे धर्म वक्तव्य है, इसका अर्थ हुआ कि मिथ्यारूपसे धर्म वक्तव्य हैं। यदि धर्म मिथ्यारूपसे वक्तव्य हैं, तो उनका कथन ही नहीं करना चाहिये। क्योंकि परमार्थसे विपरीत होनेके कारण संवृतिसे वक्तव्य धर्म तत्त्वतः अवक्तव्य ही होंगे । इस प्रकार धर्मोको सर्वथा अनभिलाप्य मान कर भी उनका जो प्रतिपादन किया जाता है उसमें विरोध स्पष्ट है । यदि तत्त्व सर्वथा अनभिलाप्य है तो उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता है। और यदि उसका प्रतिपादन किया जाता है, तो उसको अवक्तव्य नहीं कह सकते । सर्वथा अवक्तव्य धर्म 'अवक्तव्य' शब्दके द्वारा भी वक्तव्य नहीं हो सकता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.