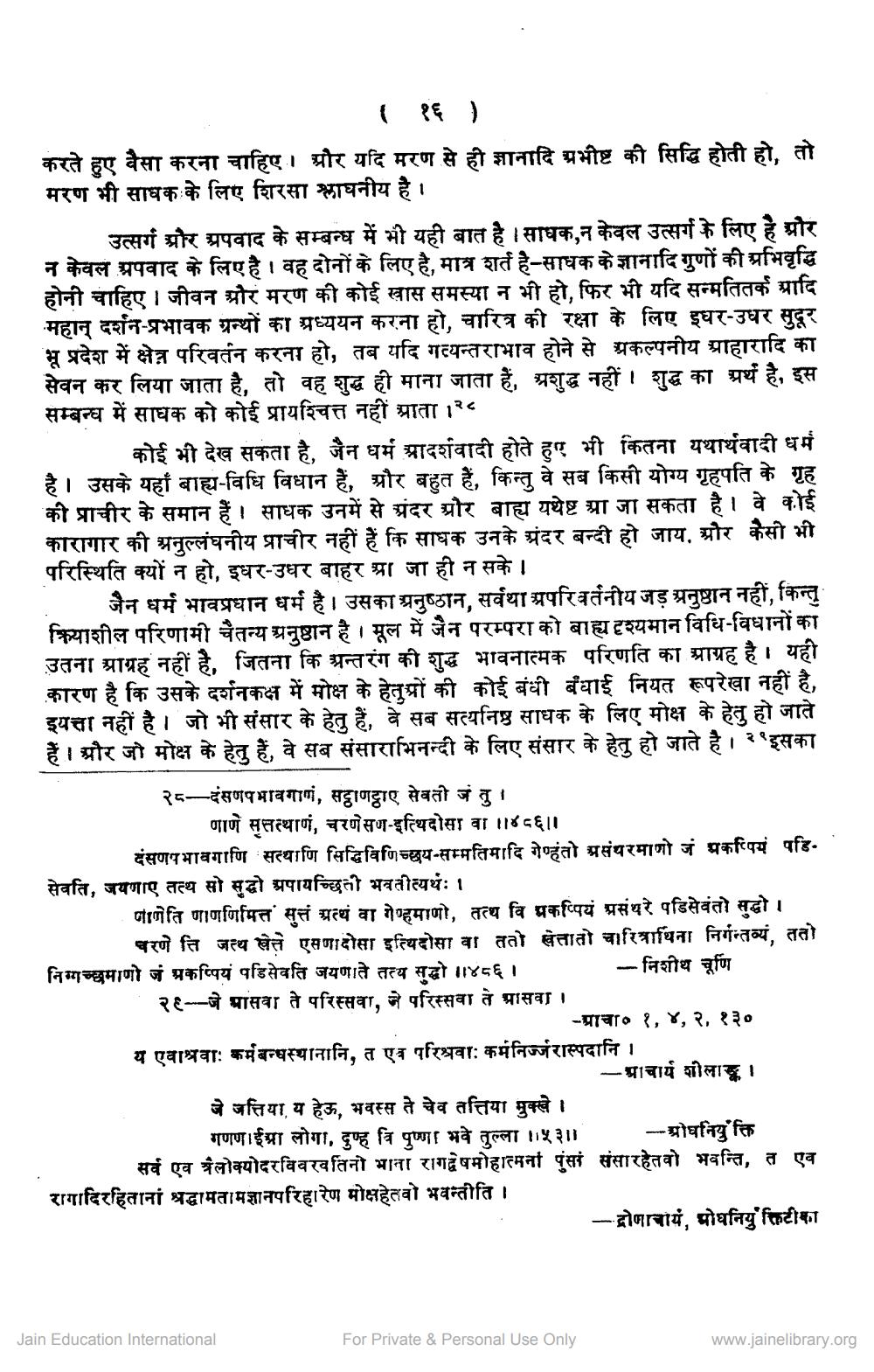________________
करते हुए वैसा करना चाहिए। और यदि मरण से ही ज्ञानादि अभीष्ट की सिद्धि होती हो, तो मरण भी साधक के लिए शिरसा श्लाघनीय है।
उत्सर्ग और अपवाद के सम्बन्ध में भी यही बात है । साधक,न केवल उत्सर्ग के लिए है और न केवल अपवाद के लिए है । वह दोनों के लिए है, मात्र शर्त है-साधक के ज्ञानादि गुणों की अभिवृद्धि होनी चाहिए । जीवन और मरण की कोई खास समस्या न भी हो, फिर भी यदि सन्मतितर्क आदि महान् दर्शन-प्रभावक ग्रन्थों का अध्ययन करना हो, चारित्र की रक्षा के लिए इधर-उधर सुदूर भू प्रदेश में क्षेत्र परिवर्तन करना हो, तब यदि गत्यन्तराभाव होने से अकल्पनीय आहारादि का सेवन कर लिया जाता है, तो वह शुद्ध ही माना जाता हैं, अशुद्ध नहीं। शुद्ध का अर्थ है, इस सम्बन्ध में साधक को कोई प्रायश्चित्त नहीं पाता ।२८
कोई भी देख सकता है, जैन धर्म आदर्शवादी होते हए भी कितना यथार्थवादी धर्म है। उसके यहाँ बाह्य-विधि विधान हैं, और बहुत हैं, किन्तु वे सब किसी योग्य गृहपति के गृह की प्राचीर के समान हैं। साधक उनमें से अंदर और बाह्य यथेष्ट आ जा सकता है। वे कोई कारागार की अनुल्लंघनीय प्राचीर नहीं हैं कि साधक उनके अंदर बन्दी हो जाय. और कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, इधर-उधर बाहर आ जा ही न सके ।
जैन धर्म भावप्रधान धर्म है। उसका अनुष्ठान, सर्वथा अपरिवर्तनीय जड़ अनुष्ठान नहीं, किन्तु क्रियाशील परिणामी चैतन्य अनुष्ठान है । मूल में जैन परम्परा को बाह्य दृश्यमान विधि-विधानों का उतना आग्रह नहीं है, जितना कि अन्तरंग की शुद्ध भावनात्मक परिणति का आग्रह है। यही कारण है कि उसके दर्शनकक्ष में मोक्ष के हेतुओं की कोई बंधी बंधाई नियत रूपरेखा नहीं है, इयत्ता नहीं है। जो भी संसार के हेतु हैं, वे सब सत्यनिष्ठ साधक के लिए मोक्ष के हेतु हो जाते हैं। और जो मोक्ष के हेतु हैं, वे सब संसाराभिनन्दी के लिए संसार के हेतु हो जाते है। २९इसका
२८-दसणपभावगाणं, सट्ठाणटाए सेवती जंतु ।
णाणे सत्तत्थाणं, चरणेसण-इत्थिदोसा वा ॥४८६॥ दसणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छय-सम्मतिमादि गेण्हतो असंथरमाणो जं प्रकप्पियं पडि. सेवति, जयणाए तत्थ सो सुद्धो अपायच्छिती भवतीत्यर्थः ।
जाणेति णाणणिमित्त सुत्तं प्रत्थं वा गेण्हमाणो, तत्थ वि प्रकप्पियं असंथरे पडिसेवंतो सुद्धो।
परणे त्ति जत्थ खेत्ते एसणादोसा इत्थिदोसा वा ततो खेत्तातो चारित्रार्थिना निर्गन्तव्यं, ततो निम्गच्छमाणो जं प्रकप्पियं पडिसेवति जयणाते तत्य सुद्धो ॥४८६।
-निशीथ चूर्णि २६-जे पासवा ते परिस्सवा, ने परिस्सवा ते प्रासवा ।
-प्राचा० १,४, २, १३० य एवाश्रवाः कर्मबन्धस्थानानि, त एव परिश्रवाः कर्मनिर्जरास्पदानि ।
-प्राचार्य शीलाङ्क। जे जत्तिया, य हेऊ, भवस्स ते चेव तत्तिया मुक्खे ।
गणणाईमा लोगा, दुण्ह वि पुण्णा भवे तुल्ला ॥५३॥ --प्रोपनियुक्ति सर्व एव त्रैलोक्योदरविवरवतिनो भाना रागद्वेषमोहात्मनों पुंसां संसारहेतवो भवन्ति, त एव रागादिरहितानां श्रद्धामतामज्ञानपरिहारेण मोक्षहेतवो भवन्तीति ।
-द्रोणाचार्य, मोधनियुक्तिटीका
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org