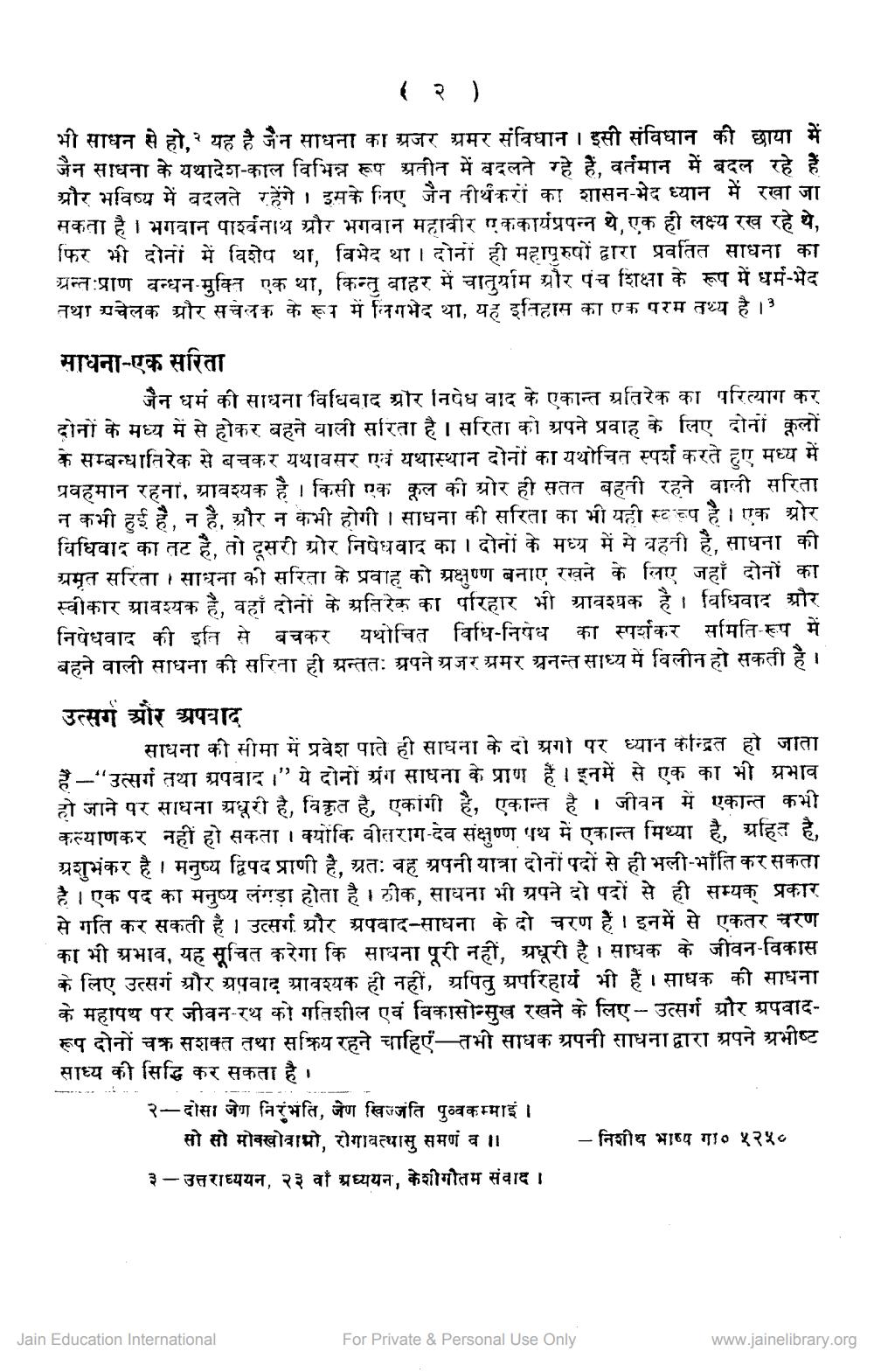________________
भी साधन से हो, यह है जैन साधना का अजर अमर संविधान । इसी संविधान की छाया में जैन साधना के यथादेश-काल विभिन्न रूप अतीत में बदलते रहे हैं, वर्तमान में बदल रहे हैं और भविष्य में बदलते रहेंगे। इसके लिए जैन तीर्थंकरों का शासन-भेद ध्यान में रखा जा सकता है । भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर एककार्यप्रपन्न थे, एक ही लक्ष्य रख रहे थे, फिर भी दोनों में विशेप था, विभेद था। दोनों ही महापुरुषों द्वारा प्रवर्तित साधना का अन्तःप्राण बन्धन-मुक्ति एक था, किन्तु बाहर में चातुर्याम और पंच शिक्षा के रूप में धर्म-भेद तथा अचेलक और सचेलक के रूप में लिंगभेद था, यह इतिहास का एक परम तथ्य है।
माधना-एक सरिता
जैन धर्म की साधना विधिवाद और निषेध वाद के एकान्त अतिरेक का परित्याग कर दोनों के मध्य में से होकर बहने वाली सरिता है । सरिता को अपने प्रवाह के लिए दोनों कूलों के सम्बन्धातिरेक से बचकर यथावसर एवं यथास्थान दोनों का यथोचित स्पर्श करते हुए मध्य में प्रवहमान रहना, यावश्यक है । किसी एक कूल की अोर ही सतत बहती रहने वाली सरिता न कभी हुई है, न है, और न कभी होगी । साधना की सरिता का भी यही स्वरूप है । एक अोर विधिवाद का तट है, तो दूसरी पोर निषेधवाद का । दोनों के मध्य में से बहती है, साधना की अमृत सरिता । साधना की सरिता के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जहाँ दोनों का स्वीकार आवश्यक है, वहाँ दोनों के अतिरेक का परिहार भी ग्रावश्यक है। विधिवाद और निषेधवाद की इति से बचकर यथोचित विधि-निषेध का स्पर्शकर समिति-रूप में बहने वाली साधना की सरिता ही अन्ततः अपने अजर अमर अनन्त साध्य में विलीन हो सकती है। उत्सर्ग और अपवाद
साधना की सीमा में प्रवेश पाते ही साधना के दो अगो पर ध्यान केन्द्रित हो जाता हैं-"उत्सर्ग तथा अपवाद ।' ये दोनों अंग साधना के प्राण हैं। इनमें से एक का भी प्रभाव हो जाने पर साधना अधूरी है, विकृत है, एकांगी है, एकान्त है । जीवन में एकान्त कभी कल्याणकर नहीं हो सकता । क्योंकि वीतराग-देव संक्षुण्ण पथ में एकान्त मिथ्या है, अहित है, अशुभंकर है। मनुष्य द्विपद प्राणी है, अतः वह अपनी यात्रा दोनों पदों से ही भली-भाँति कर सकता है । एक पद का मनुष्य लंगड़ा होता है। ठीक, साधना भी अपने दो पदों से ही सम्यक् प्रकार से गति कर सकती है । उत्सर्ग. और अपवाद-साधना के दो चरण हैं । इनमें से एकतर चरण का भी अभाव, यह सूचित करेगा कि साधना पूरी नहीं, अधूरी है। साधक के जीवन-विकास के लिए उत्सर्ग और अपवाद आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य भी हैं । साधक की साधना के महापथ पर जीवन-रथ को गतिशील एवं विकासोन्मुख रखने के लिए- उत्सर्ग और अपवादरूप दोनों चक्र सशक्त तथा सक्रिय रहने चाहिएं-तभी साधक अपनी साधना द्वारा अपने अभीष्ट साध्य की सिद्धि कर सकता है।
२-दोसा जेण निरंभति, जेण खिज्जति पुवकम्माई।
सो सो मोक्खोवामो, रोगावत्थासु समणं व ॥ - निशीथ भाष्य गा० ५२५० ३ - उत्तराध्ययन, २३ वा अध्ययन, केशीगौतम संवाद ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org