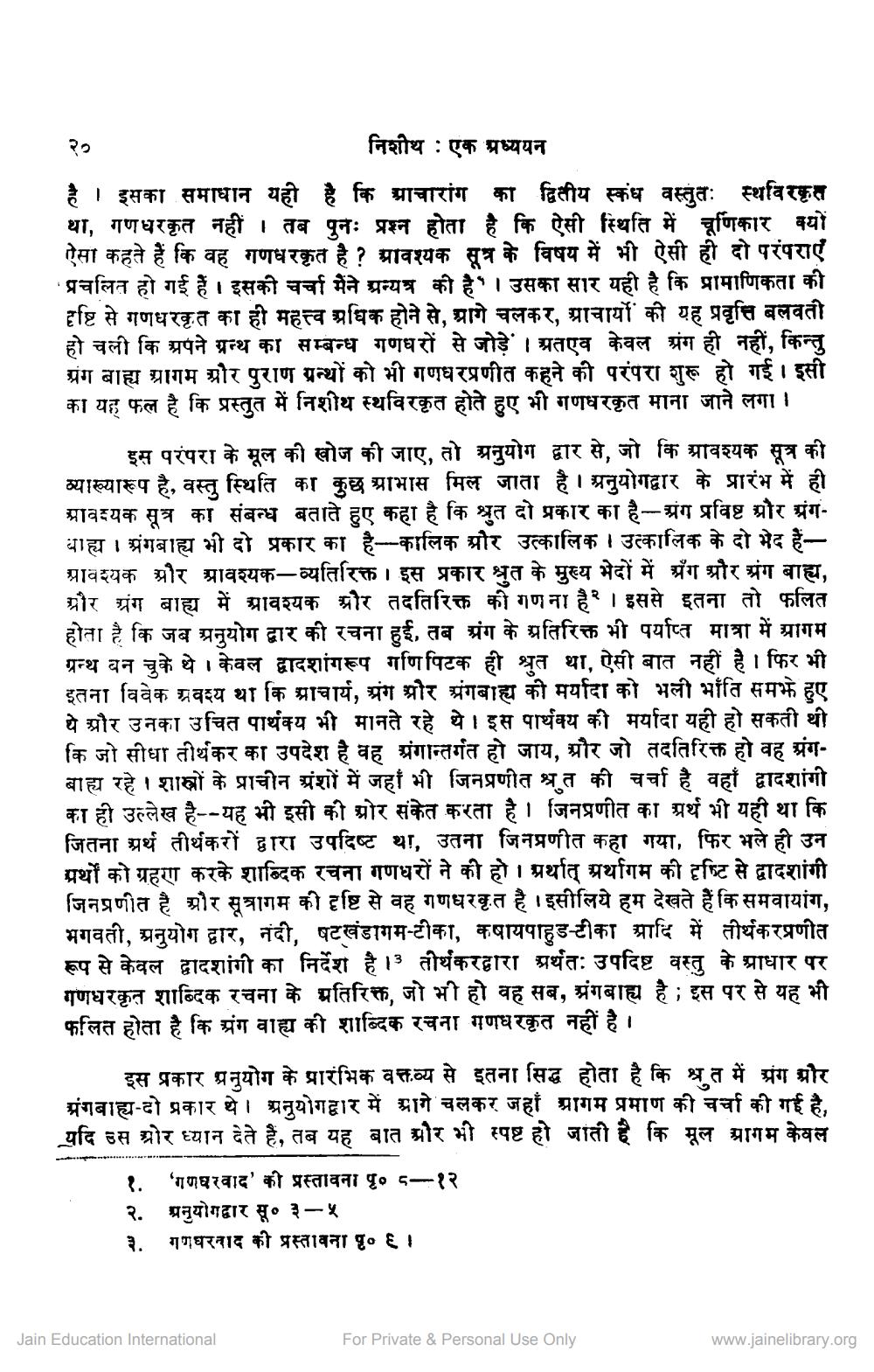________________
निशीथ : एक अध्ययन है । इसका समाधान यही है कि प्राचारांग का द्वितीय स्कंध वस्तुतः स्थविरकृत था, गणधरकृत नहीं । तब पुनः प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में चूर्णिकार क्यों ऐसा कहते हैं कि वह गणधरकृत है ? आवश्यक सूत्र के विषय में भी ऐसी ही दो परंपराएं प्रचलित हो गई हैं । इसकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है । उसका सार यही है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से गणधरकृत का ही महत्त्व अधिक होने से, आगे चलकर, प्राचार्यों की यह प्रवृत्ति बलवती हो चली कि अपने ग्रन्थ का सम्बन्ध गणधरों से जोड़ें । अतएव केवल अंग ही नहीं, किन्तु अंग बाह्य ग्रागम और पुराण ग्रन्थों को भी गणधरप्रणीत कहने की परंपरा शुरू हो गई। इसी का यह फल है कि प्रस्तुत में निशीथ स्थविरकृत होते हुए भी गणधरकृत माना जाने लगा।
इस परंपरा के मूल की खोज की जाए, तो अनुयोग द्वार से, जो कि आवश्यक सूत्र की व्याख्यारूप है, वस्तु स्थिति का कुछ प्राभास मिल जाता है । अनुयोगद्वार के प्रारंभ में ही प्रावश्यक सूत्र का संबन्ध बताते हुए कहा है कि श्रुत दो प्रकार का है-अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य । अंगबाह्य भी दो प्रकार का है-कालिक और उत्कालिक । उत्कालिक के दो भेद हैंअावश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त । इस प्रकार श्रुत के मुख्य भेदों में अंग और अंग बाह्य, पौर अंग बाह्य में आवश्यक और तदतिरिक्त की गणना है । इससे इतना तो फलित होता है कि जब अनुयोग द्वार की रचना हुई, तब अंग के अतिरिक्त भी पर्याप्त मात्रा में प्रागम ग्रन्थ बन चुके थे । केवल द्वादशांगरूप गणिपिटक ही श्रुत था, ऐसी बात नहीं है । फिर भी इतना विवेक अवश्य था कि प्राचार्य, अंग और अंगबाह्य की मर्यादा को भली भाँति समझे हुए थे और उनका उचित पार्थक्य भी मानते रहे थे। इस पार्थक्य की मर्यादा यही हो सकती थी कि जो सीधा तीर्थकर का उपदेश है वह अंगान्तर्गत हो जाय, और जो तदतिरिक्त हो वह अंगबाह्य रहे । शास्त्रों के प्राचीन अंशों में जहाँ भी जिनप्रणीत श्रुत की चर्चा है वहाँ द्वादशांगी का ही उल्लेख है--यह भी इसी की ओर संकेत करता है। जिनप्रणीत का अर्थ भी यही था कि जितना अर्थ तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट था, उतना जिनप्रणीत कहा गया, फिर भले ही उन प्रर्थों को ग्रहण करके शाब्दिक रचना गणधरों ने की हो । अर्थात् अर्थागम की दृष्टि से द्वादशांगी जिनप्रणीत है और सूत्रागम की दृष्टि से वह गणधरकृत है । इसीलिये हम देखते हैं कि समवायांग, भगवती, अनुयोग द्वार, नंदी, षटखंडागम-टीका, कषायपाहुड-टीका आदि में तीर्थकरप्रणीत रूप से केवल द्वादशांगी का निर्देश है। तीर्थकरद्वारा अर्थतः उपदिष्ट वस्तु के आधार पर गणधरकृत शाब्दिक रचना के अतिरिक्त, जो भी हो वह सब, अंगबाह्य है ; इस पर से यह भी फलित होता है कि अंग वाह्य की शाब्दिक रचना गणधरकृत नहीं है।
इस प्रकार अनुयोग के प्रारंभिक वक्तव्य से इतना सिद्ध होता है कि श्रु त में अंग और अंगबाह्य-दो प्रकार थे। अनुयोगद्वार में आगे चलकर जहाँ पागम प्रमाण की चर्चा की गई है, यदि उस ओर ध्यान देते हैं, तब यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि मूल आगम केवल
१. 'गणघरवाद' की प्रस्तावना पृ० ८-१२ २. प्रनयोगद्वार सू०३-५ ३. गणधरनाद की प्रस्तावना पृ०६ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org