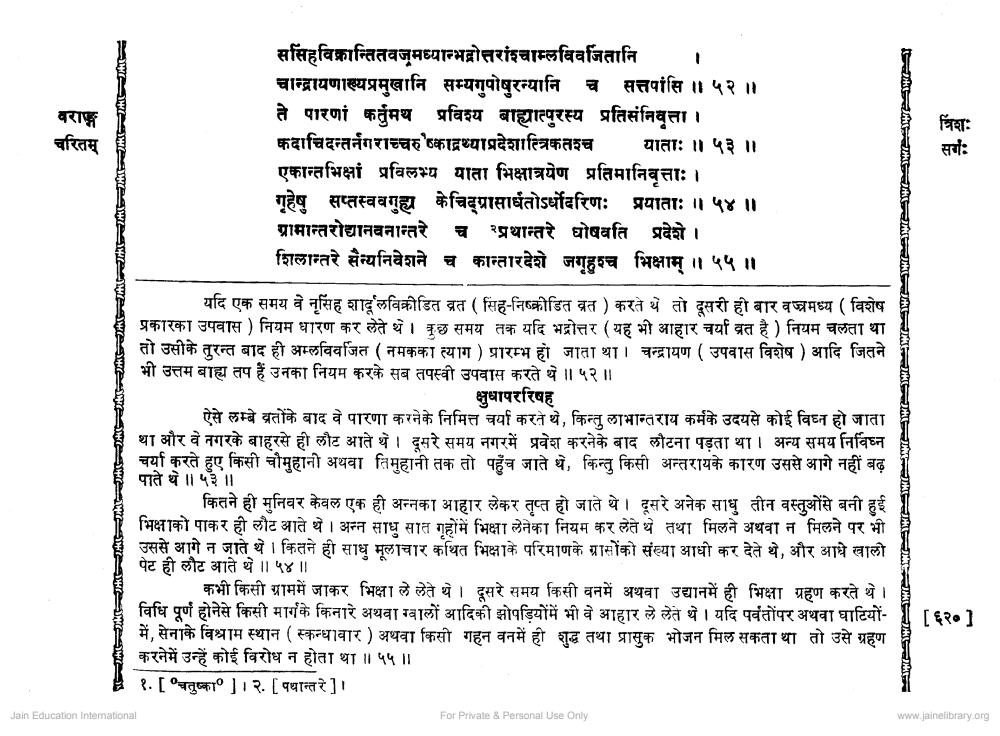________________
त्रिंशः
वराङ्ग चरितम्
ससिंहविक्रान्तितवजमध्यान्भवोत्तरांश्चाम्लविजितानि । चान्द्रायणाख्यप्रमुखानि सम्यगुपोषुरन्यानि च सत्तपांसि ॥ ५२ ॥ ते पारणां कर्तुमथ प्रविश्य बाह्यात्पुरस्य प्रतिसंनिवृत्ता। कदाचिदन्तनगराच्चरु'काद्रथ्याप्रदेशास्त्रिकतश्च याताः ॥ ५३॥ एकान्तभिक्षां प्रविलभ्य याता भिक्षात्रयेण प्रतिमानिवृत्ताः। गृहेषु सप्तस्ववगुह्य केचिद्ग्रासार्धतोऽ|दरिणः प्रयाताः ॥ ५४ ॥ ग्रामान्तरोद्यानवनान्तरे च प्रथान्तरे घोषवति प्रदेशे। शिलान्तरे सैन्यनिवेशने च कान्तारदेशे जगहश्च भिक्षाम् ॥ ५५॥
सर्गः
eHESHAHARASHParenese-we-e-
ASTRISTIANE
चUTUHAPURमनामन्यमान्य
यदि एक समय वे नृसिंह शार्दूलविक्रीडित व्रत (सिंह-निष्क्रीडित व्रत ) करते थे तो दूसरी ही बार वजमध्य (विशेष प्रकारका उपवास ) नियम धारण कर लेते थे। कुछ समय तक यदि भद्रोत्तर ( यह भी आहार चर्या व्रत है ) नियम चलता था तो उसीके तुरन्त बाद ही अम्लविवजित (नमकका त्याग) प्रारम्भ हो जाता था। चन्द्रायण ( उपवास विशेष ) आदि जितने भी उत्तम बाह्य तप हैं उनका नियम करके सब तपस्वी उपवास करते थे ।। ५२ ॥
क्षुधापररिषह ऐसे लम्बे व्रतोंके बाद वे पारणा करने के निमित्त चर्या करते थे, किन्तु लाभान्तराय कर्मके उदयसे कोई विघ्न हो जाता था और वे नगरके बाहरसे ही लौट आते थे। दुसरे समय नगरमें प्रवेश करनेके बाद लौटना पड़ता था। अन्य समय निर्विघ्न चर्या करते हुए किसी चौमुहानी अथवा तिमुहानी तक तो पहुँच जाते थे, किन्तु किसी अन्तरायके कारण उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे ।। ५३ ॥
कितने ही मुनिवर केवल एक ही अन्नका आहार लेकर तृप्त हो जाते थे। दूसरे अनेक साधु तीन वस्तुओंसे बनी हुई भिक्षाको पाकर ही लौट आते थे । अन्न साधु सात गहों में भिक्षा लेनेका नियम कर लेते थे तथा मिलने अथवा न मिलने पर भी
उससे आगे न जाते थे । कितने ही साधु मुलाचार कथित भिक्षाके परिमाणके ग्रासोंको संख्या आधी कर देते थे, और आधे खाली । पेट ही लौट आते थे ।। ५४ ॥
कभी किसी ग्राममें जाकर भिक्षा ले लेते थे। दूसरे समय किसी वनमें अथवा उद्यानमें ही भिक्षा ग्रहण करते थे। विधि पूर्ण होनेसे किसी मार्ग के किनारे अथवा ग्वालों आदिकी झोपड़ियोंमें भी वे आहार ले लेते थे । यदि पर्वतोंपर अथवा घाटियोंमें, सेनाके विश्राम स्थान (स्कन्धावार ) अथवा किसी गहन वनमें ही शुद्ध तथा प्रासुक भोजन मिल सकता था तो उसे ग्रहण करनेमें उन्हें कोई विरोध न होता था ॥ ५५ ॥ १. [°चतुष्का ] । २. [ पथान्तरे ] ।
[२०]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org