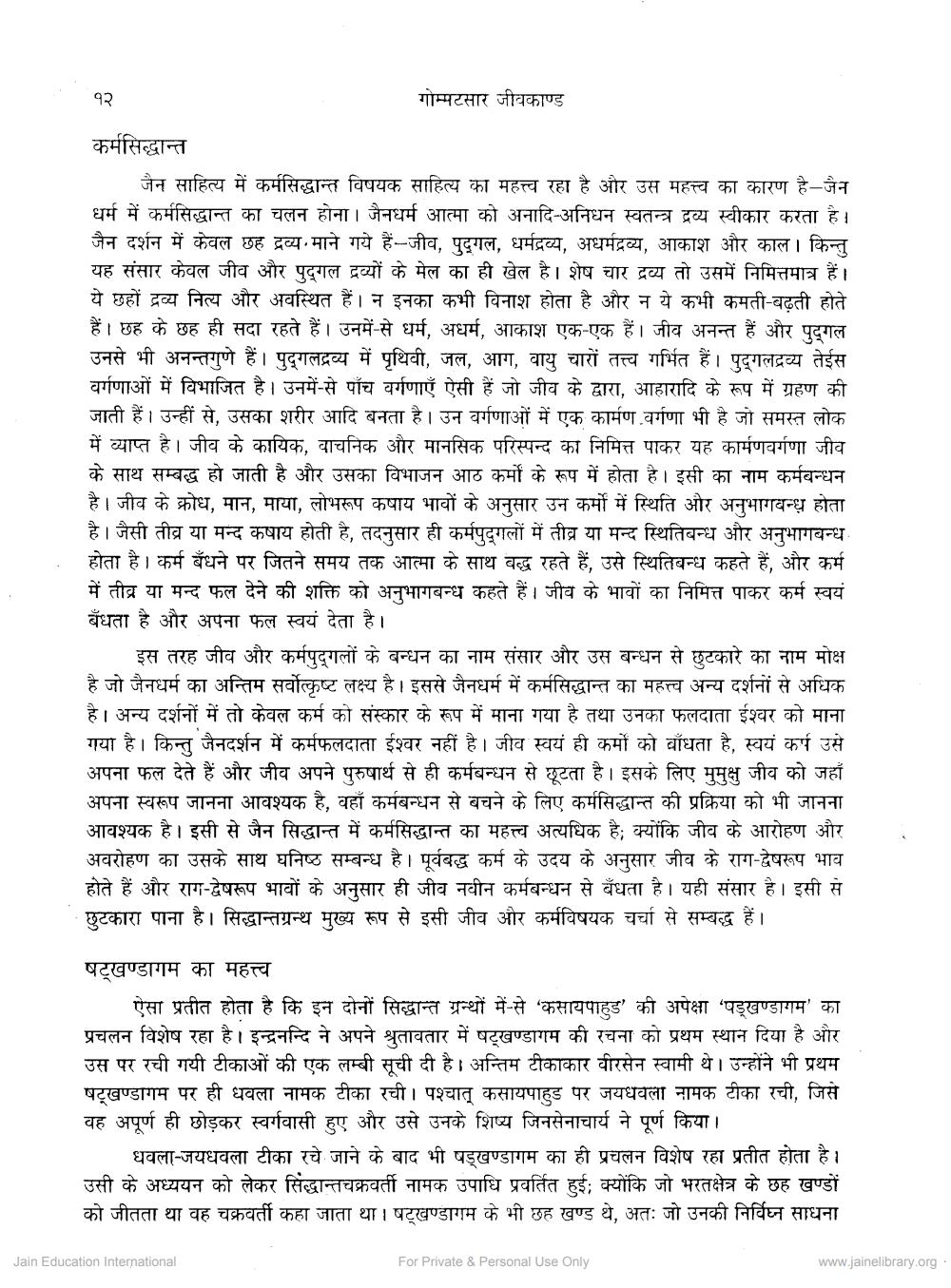________________
१२
गोम्मटसार जीवकाण्ड
कर्मसिद्धान्त
जैन साहित्य में कर्मसिद्धान्त विषयक साहित्य का महत्त्व रहा है और उस महत्त्व का कारण है- जैन धर्म में कर्मसिद्धान्त का चलन होना । जैनधर्म आत्मा को अनादि - अनिधन स्वतन्त्र द्रव्य स्वीकार करता है । जैन दर्शन में केवल छह द्रव्य माने गये हैं-जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काल । किन्तु यह संसार केवल जीव और पुद्गल द्रव्यों के मेल का ही खेल है। शेष चार द्रव्य तो उसमें निमित्तमात्र हैं । ये छहों द्रव्य नित्य और अवस्थित हैं । न इनका कभी विनाश होता है और न ये कभी कमती-बढ़ती होते हैं। छह के छह ही सदा रहते हैं । उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश एक-एक हैं। जीव अनन्त हैं और पुद्गल उनसे भी अनन्तगुणे हैं । पुद्गलद्रव्य में पृथिवी, जल, आग, वायु चारों तत्त्व गर्भित हैं । पुद्गलद्रव्य तेईस वर्गणाओं में विभाजित है। उनमें से पाँच वर्गणाएँ ऐसी हैं जो जीव के द्वारा, आहारादि के रूप में ग्रहण की जाती हैं। उन्हीं से, उसका शरीर आदि बनता है। उन वर्गणाओं में एक कार्मण वर्गणा भी है जो समस्त लोक में व्याप्त है । जीव के कायिक, वाचनिक और मानसिक परिस्पन्द का निमित्त पाकर यह कार्मणवर्गणा जीव के साथ सम्बद्ध हो जाती है और उसका विभाजन आठ कर्मों के रूप में होता है। इसी का नाम कर्मबन्धन है। जीव के क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय भावों के अनुसार उन कर्मों में स्थिति और अनुभागबन्ध होता है। जैसी तीव्र या मन्द कषाय होती है, तदनुसार ही कर्मपुद्गलों में तीव्र या मन्द स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धहोता है। कर्म बँधने पर जितने समय तक आत्मा के साथ बद्ध रहते हैं, उसे स्थितिबन्ध कहते हैं, और कर्म में तीव्र या मन्द फल देने की शक्ति को अनुभागबन्ध कहते हैं । जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म स्वयं बँधता है और अपना फल स्वयं देता है ।
इस तरह जीव और कर्मपुद्गलों के बन्धन का नाम संसार और उस बन्धन से छुटकारे का नाम मोक्ष है जो जैनधर्म का अन्तिम सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। इससे जैनधर्म में कर्मसिद्धान्त का महत्त्व अन्य दर्शनों से अधि है। अन्य दर्शनों में तो केवल कर्म को संस्कार के रूप में माना गया है तथा उनका फलदाता ईश्वर को माना गया है । किन्तु जैनदर्शन में कर्मफलदाता ईश्वर नहीं है । जीव स्वयं ही कर्मों को बाँधता है, स्वयं कर्म उसे अपना फल देते हैं और जीव अपने पुरुषार्थ से ही कर्मबन्धन से छूटता है। इसके लिए मुमुक्षु जीव को जहाँ अपना स्वरूप जानना आवश्यक है, वहाँ कर्मबन्धन से बचने के लिए कर्मसिद्धान्त की प्रक्रिया को भी जानना आवश्यक है। इसी से जैन सिद्धान्त में कर्मसिद्धान्त का महत्त्व अत्यधिक है; क्योंकि जीव के आरोहण और अवरोहण का उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पूर्वबद्ध कर्म के उदय के अनुसार जीव के राग-द्वेषरूप भाव होते हैं और राग-द्वेषरूप भावों के अनुसार ही जीव नवीन कर्मबन्धन से बँधता है । यही संसार है। इसी से छुटकारा पाना है । सिद्धान्तग्रन्थ मुख्य रूप से इसी जीव और कर्मविषयक चर्चा से सम्बद्ध हैं ।
षट्खण्डागम का महत्त्व
ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों सिद्धान्त ग्रन्थों में से 'कसायपाहुड' की अपेक्षा 'पडूखण्डागम' का प्रचलन विशेष रहा है। इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में षट्खण्डागम की रचना को प्रथम स्थान दिया है और उस पर रची गयी टीकाओं की एक लम्बी सूची दी है । अन्तिम टीकाकार वीरसेन स्वामी थे। उन्होंने भी प्रथम षट्खण्डागम पर ही धवला नामक टीका रची। पश्चात् कसायपाहुड पर जयधवला नामक टीका रची, जिसे वह अपूर्ण ही छोड़कर स्वर्गवासी हुए और उसे उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने पूर्ण किया ।
धवला - जयधवला टीका रचे जाने के बाद भी षड्खण्डागम का ही प्रचलन विशेष रहा प्रतीत होता है । उसी के अध्ययन को लेकर सिंद्धान्तचक्रवर्ती नामक उपाधि प्रवर्तित हुई; क्योंकि जो भरतक्षेत्र के छह खण्डों को जीतता था वह चक्रवर्ती कहा जाता था । षट्खण्डागम के भी छह खण्ड थे, अतः जो उनकी निर्विघ्न साधना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org