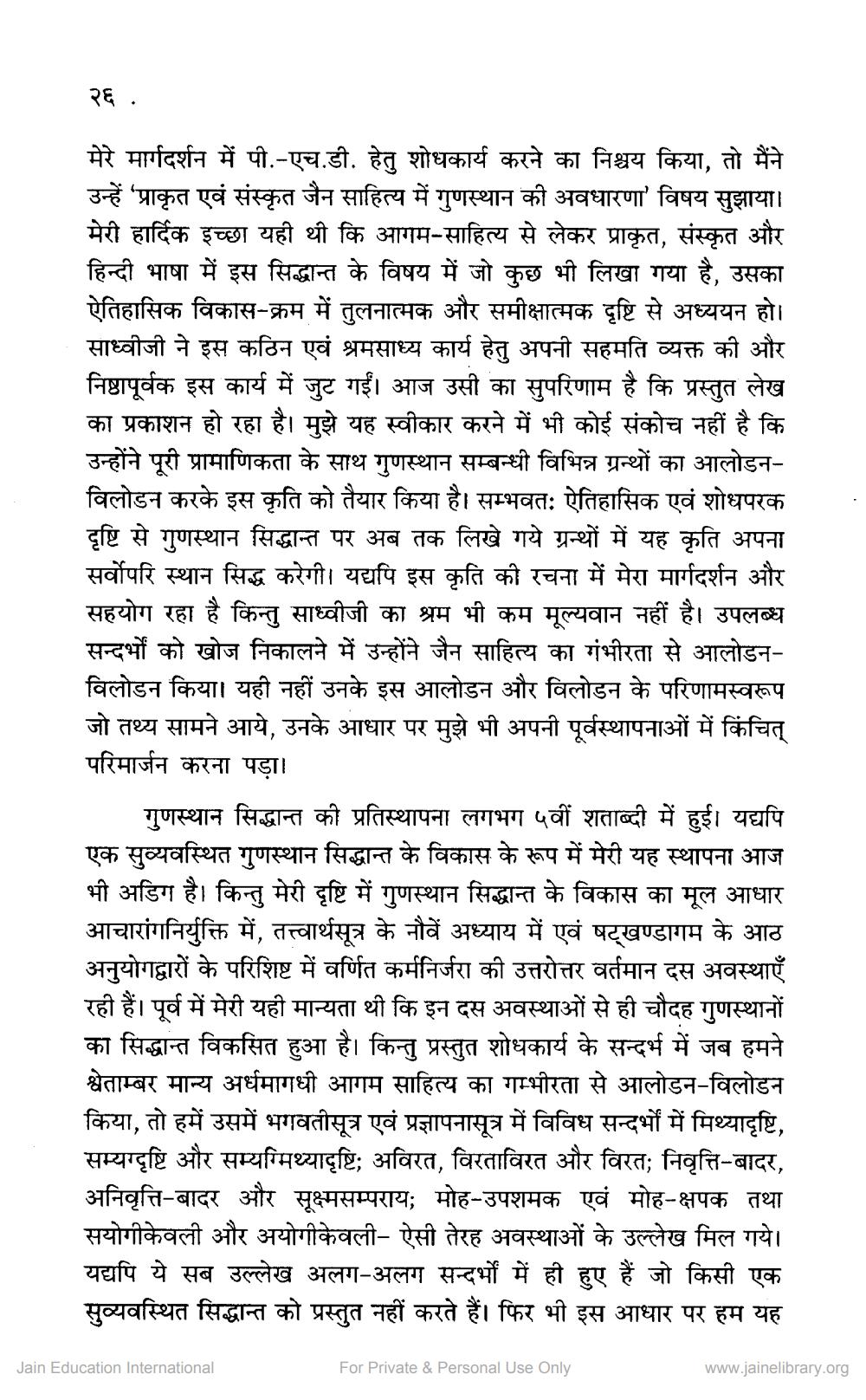________________
२६ .
मेरे मार्गदर्शन में पी.-एच.डी. हेतु शोधकार्य करने का निश्चय किया, तो मैंने उन्हें 'प्राकृत एवं संस्कृत जैन साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा' विषय सुझाया। मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि आगम-साहित्य से लेकर प्राकृत, संस्कृत और हिन्दी भाषा में इस सिद्धान्त के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है, उसका ऐतिहासिक विकास-क्रम में तुलनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से अध्ययन हो। साध्वीजी ने इस कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य हेतु अपनी सहमति व्यक्त की और निष्ठापूर्वक इस कार्य में जुट गईं। आज उसी का सुपरिणाम है कि प्रस्तुत लेख का प्रकाशन हो रहा है। मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ गुणस्थान सम्बन्धी विभिन्न ग्रन्थों का आलोडनविलोडन करके इस कृति को तैयार किया है। सम्भवतः ऐतिहासिक एवं शोधपरक दृष्टि से गुणस्थान सिद्धान्त पर अब तक लिखे गये ग्रन्थों में यह कृति अपना सर्वोपरि स्थान सिद्ध करेगी। यद्यपि इस कृति की रचना में मेरा मार्गदर्शन और सहयोग रहा है किन्तु साध्वीजी का श्रम भी कम मूल्यवान नहीं है। उपलब्ध सन्दर्भो को खोज निकालने में उन्होंने जैन साहित्य का गंभीरता से आलोडनविलोडन किया। यही नहीं उनके इस आलोडन और विलोडन के परिणामस्वरूप जो तथ्य सामने आये, उनके आधार पर मुझे भी अपनी पूर्वस्थापनाओं में किंचित् परिमार्जन करना पड़ा।
गुणस्थान सिद्धान्त की प्रतिस्थापना लगभग ५वीं शताब्दी में हुई। यद्यपि एक सुव्यवस्थित गुणस्थान सिद्धान्त के विकास के रूप में मेरी यह स्थापना आज भी अडिग है। किन्तु मेरी दृष्टि में गुणस्थान सिद्धान्त के विकास का मूल आधार आचारांगनियुक्ति में, तत्त्वार्थसूत्र के नौवें अध्याय में एवं षट्खण्डागम के आठ अनुयोगद्वारों के परिशिष्ट में वर्णित कर्मनिर्जरा की उत्तरोत्तर वर्तमान दस अवस्थाएँ रही हैं। पूर्व में मेरी यही मान्यता थी कि इन दस अवस्थाओं से ही चौदह गुणस्थानों का सिद्धान्त विकसित हुआ है। किन्तु प्रस्तुत शोधकार्य के सन्दर्भ में जब हमने श्वेताम्बर मान्य अर्धमागधी आगम साहित्य का गम्भीरता से आलोडन-विलोडन किया, तो हमें उसमें भगवतीसूत्र एवं प्रज्ञापनासूत्र में विविध सन्दर्भो में मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि; अविरत, विरताविरत और विरत; निवृत्ति-बादर, अनिवृत्ति-बादर और सूक्ष्मसम्पराय; मोह-उपशमक एवं मोह-क्षपक तथा सयोगीकेवली और अयोगीकेवली- ऐसी तेरह अवस्थाओं के उल्लेख मिल गये। यद्यपि ये सब उल्लेख अलग-अलग सन्दर्भो में ही हुए हैं जो किसी एक सुव्यवस्थित सिद्धान्त को प्रस्तुत नहीं करते हैं। फिर भी इस आधार पर हम यह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org