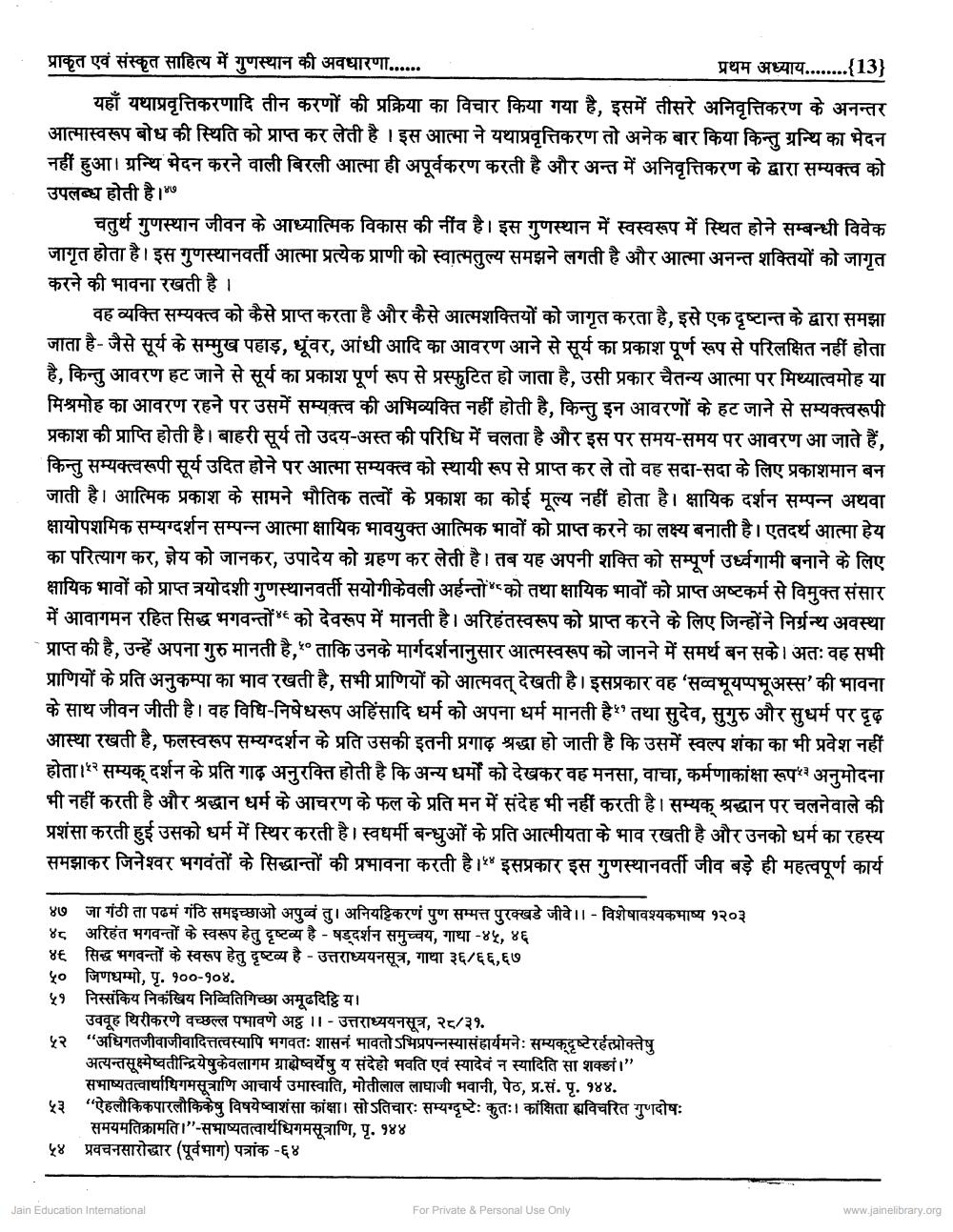________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
प्रथम अध्याय........{13} यहाँ यथाप्रवृत्तिकरणादि तीन करणों की प्रक्रिया का विचार किया गया है, इसमें तीसरे अनिवृत्तिकरण के अनन्तर आत्मास्वरूप बोध की स्थिति को प्राप्त कर लेती है । इस आत्मा ने यथाप्रवृत्तिकरण तो अनेक बार किया किन्तु ग्रन्थि का भेदन नहीं हुआ। ग्रन्थि भेदन करने वाली बिरली आत्मा ही अपूर्वकरण करती है और अन्त में अनिवृत्तिकरण के द्वारा सम्यक्त्व को उपलब्ध होती है।
चतुर्थ गुणस्थान जीवन के आध्यात्मिक विकास की नींव है। इस गुणस्थान में स्वस्वरूप में स्थित होने सम्बन्धी विवेक जागृत होता है। इस गुणस्थानवर्ती आत्मा प्रत्येक प्राणी को स्वात्मतुल्य समझने लगती है और आत्मा अनन्त शक्तियों को जागृत करने की भावना रखती है।
वह व्यक्ति सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त करता है और कैसे आत्मशक्तियों को जागृत करता है, इसे एक दृष्टान्त के द्वारा समझा जाता है- जैसे सूर्य के सम्मुख पहाड़,धूंवर, आंधी आदि का आवरण आने से सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होता है, किन्तु आवरण हट जाने से सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाता है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा पर मिथ्यात्वमोह या मिश्रमोह का आवरण रहने पर उसमें सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, किन्तु इन आवरणों के हट जाने से सम्यक्त्वरूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। बाहरी सूर्य तो उदय-अस्त की परिधि में चलता है और इस पर समय-समय पर आवरण आ जाते हैं, किन्तु सम्यक्त्वरूपी सूर्य उदित होने पर आत्मा सम्यक्त्व को स्थायी रूप से प्राप्त कर ले तो वह सदा-सदा के लिए प्रकाशमान बन जाती है। आत्मिक प्रकाश के सामने भौतिक तत्वों के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं होता है। क्षायिक दर्शन सम्पन्न अथवा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन सम्पन्न आत्मा क्षायिक भावयुक्त आत्मिक भावों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाती है। एतदर्थ आत्मा हेय का परित्याग कर, ज्ञेय को जानकर, उपादेय को ग्रहण कर लेती है। तब यह अपनी शक्ति को सम्पूर्ण उर्ध्वगामी बनाने के लिए क्षायिक भावों को प्राप्त त्रयोदशी गुणस्थानवर्ती सयोगीकेवली अर्हन्तों को तथा क्षायिक भावों को प्राप्त अष्टकर्म से विमुक्त संसार में आवागमन रहित सिद्ध भगवन्तों को देवरूप में मानती है। अरिहंतस्वरूप को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने निर्ग्रन्थ अवस्था प्राप्त की है, उन्हें अपना गुरु मानती है, ताकि उनके मार्गदर्शनानुसार आत्मस्वरूप को जानने में समर्थ बन सके। अतः वह सभी प्राणियों के प्रति अनुकम्पा का भाव रखती है, सभी प्राणियों को आत्मवत् देखती है। इसप्रकार वह 'सव्वभूयप्पभूअस्स' की भावना के साथ जीवन जीती है। वह विधि-निषेधरूप अहिंसादि धर्म को अपना धर्म मानती है" तथा सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ़ आस्था रखती है, फलस्वरूप सम्यग्दर्शन के प्रति उसकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है कि उसमें स्वल्प शंका का भी प्रवेश नहीं होता।२ सम्यक् दर्शन के प्रति गाढ़ अनुरक्ति होती है कि अन्य धर्मों को देखकर वह मनसा, वाचा, कर्मणाकांक्षा रूप३ अनुमोदना भी नहीं करती है और श्रद्धान धर्म के आचरण के फल के प्रति मन में संदेह भी नहीं करती है। सम्यक् श्रद्धान पर चलनेवाले की प्रशंसा करती हुई उसको धर्म में स्थिर करती है। स्वधर्मी बन्धुओं के प्रति आत्मीयता के भाव रखती है और उनको धर्म का रहस्य समझाकर जिनेश्वर भगवंतों के सिद्धान्तों की प्रभावना करती है। इसप्रकार इस गुणस्थानवी जीव बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य
४७ जा गंठी ता पढमं गंठि समइच्छाओ अपुलं तु। अनियट्टिकरणं पुण सम्मत्त पुरक्खडे जीवे।। - विशेषावश्यकभाष्य १२०३ ४८ अरिहंत भगवन्तों के स्वरूप हेतु दृष्टव्य है - षड्दर्शन समुच्चय, गाथा -४५, ४६ ४६ सिद्ध भगवन्तों के स्वरूप हेतु दृष्टव्य है - उत्तराध्ययनसूत्र, गाथा ३६/६६,६७
जिणधम्मो, पृ. १००-१०४. ५१ निस्संकिय निकंखिय निवितिगिच्छा अमूढदिट्ठिय।
उववूह थिरीकरणे वच्छल्ल पभावणे अट्ठ ।। - उत्तराध्ययनसूत्र, २८/३१. "अधिगतजीवाजीवादित्तत्वस्यापि भगवतः शासनं भावतोऽभिप्रपन्नस्यासंहार्यमनेः सम्यकदृष्टेरर्हत्प्रोक्तेषु अत्यन्तसूक्ष्मेष्वतीन्द्रियेषुकेवलागम ग्राह्येष्वर्थेषु य संदेहो भवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा शक्ङा।"
सभाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्राणि आचार्य उमास्वाति, मोतीलाल लाघाजी भवानी, पेठ, प्र.सं. पृ. १४४. ५३ "ऐहलौकिकपारलौकिकेषु विषयेष्वाशंसा कांक्षा। सोऽतिचारः सम्यग्दृष्टेः कुतः। कांक्षिता ह्यविचरित गुणदोषः
समयमतिक्रामति।"-सभाष्यतत्वार्थधिगमसूत्राणि, पृ. १४४ ५४ प्रवचनसारोद्धार (पूर्वभाग) पत्रांक -६४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org