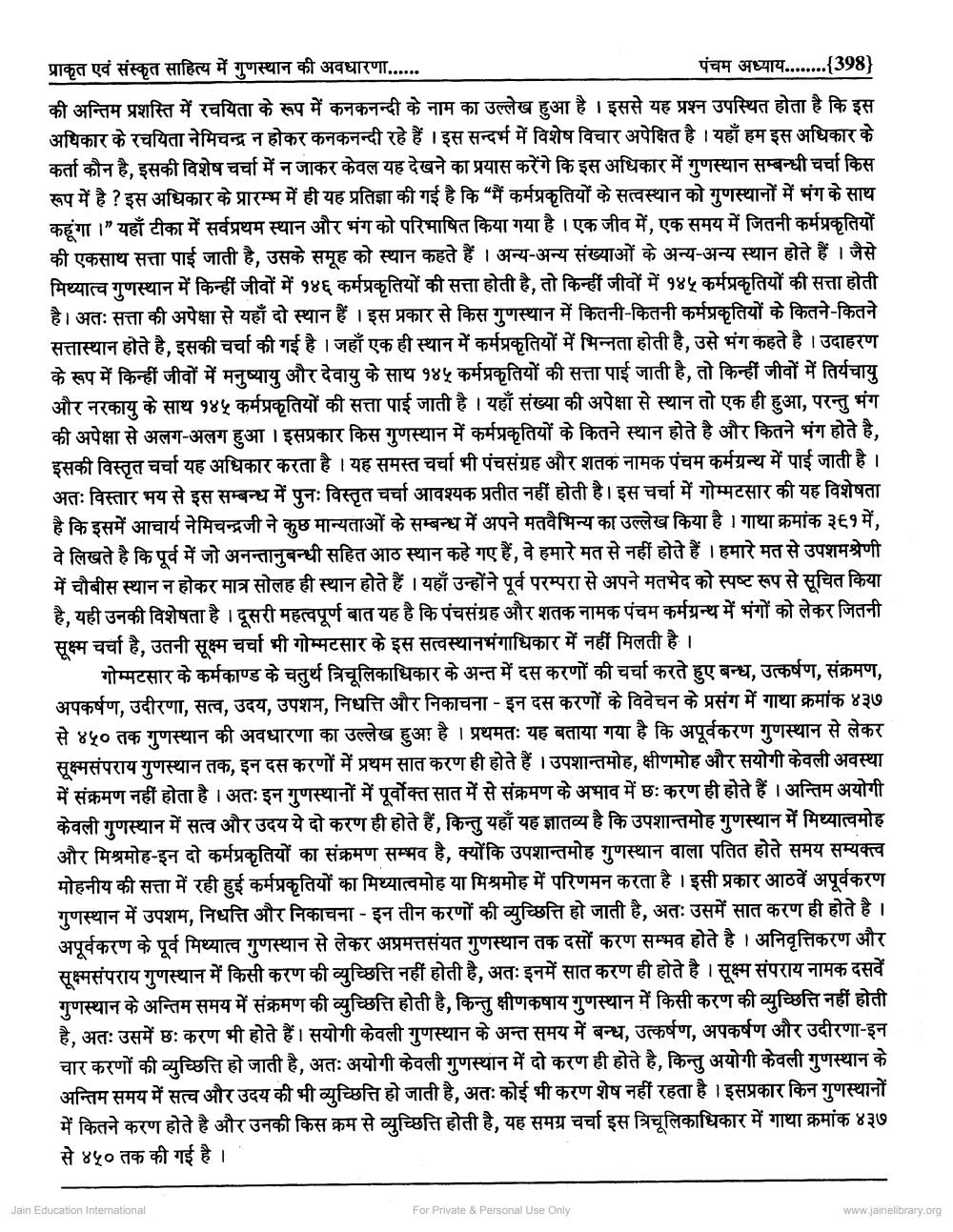________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
पंचम अध्याय........{398} की अन्तिम प्रशस्ति में रचयिता के रूप में कनकनन्दी के नाम का उल्लेख हुआ है। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस अधिकार के रचयिता नेमिचन्द्र न होकर कनकनन्दी रहे हैं । इस सन्दर्भ में विशेष विचार अपेक्षित है । यहाँ हम इस अधिकार के कर्ता कौन है, इसकी विशेष चर्चा में न जाकर केवल यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस अधिकार में गुणस्थान सम्बन्धी चर्चा किस रूप में है ? इस अधिकार के प्रारम्भ में ही यह प्रतिज्ञा की गई है कि “मैं कर्मप्रकृतियों के सत्वस्थान को गुणस्थानों में भंग के साथ कहूंगा।" यहाँ टीका में सर्वप्रथम स्थान और भंग को परिभाषित किया गया है । एक जीव में, एक समय में जितनी कर्मप्रकृतियों की एकसाथ सत्ता पाई जाती है, उसके समूह को स्थान कहते हैं । अन्य-अन्य संख्याओं के अन्य-अन्य स्थान होते हैं । जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में किन्हीं जीवों में १४६ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है, तो किन्हीं जीवों में १४५ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है। अतः सत्ता की अपेक्षा से यहाँ दो स्थान हैं । इस प्रकार से किस गुणस्थान में कितनी-कितनी कर्मप्रकृतियों के कितने-कितने सत्तास्थान होते है, इसकी चर्चा की गई है । जहाँ एक ही स्थान में कर्मप्रकृतियों में भिन्नता होती है, उसे भंग कहते है। उदाहरण के रूप में किन्हीं जीवों में मनुष्यायु और देवायु के साथ १४५ कर्मप्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है, तो किन्हीं जीवों में तिर्यचायु और नरकायु के साथ १४५ कर्मप्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है । यहाँ संख्या की अपेक्षा से स्थान तो एक ही हुआ, परन्तु मंग की अपेक्षा से अलग-अलग हुआ। इसप्रकार किस गुणस्थान में कर्मप्रकृतियों के कितने स्थान होते है और कितने भंग होते है, इसकी विस्तृत चर्चा यह अधिकार करता है । यह समस्त चर्चा भी पंचसंग्रह और शतक नामक पंचम कर्मग्रन्थ में पाई जाती है। अतः विस्तार भय से इस सम्बन्ध में पुनः विस्तृत चर्चा आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। इस चर्चा में गोम्मटसार की यह विशेषता है कि इसमें आचार्य नेमिचन्द्रजी ने कुछ मान्यताओं के सम्बन्ध में अपने मतवैभिन्य का उल्लेख किया है । गाथा क्रमांक ३६१ में, वे लिखते है कि पूर्व में जो अनन्तानुबन्धी सहित आठ स्थान कहे गए हैं, वे हमारे मत से नहीं होते हैं । हमारे मत से उपशमश्रेणी में चौबीस स्थान न होकर मात्र सोलह ही स्थान होते हैं । यहाँ उन्होंने पूर्व परम्परा से अपने मतभेद को स्पष्ट रूप से सूचित किया है, यही उनकी विशेषता है । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचसंग्रह और शतक नामक पंचम कर्मग्रन्थ में भंगों को लेकर जितनी सूक्ष्म चर्चा है, उतनी सूक्ष्म चर्चा भी गोम्मटसार के इस सत्वस्थानभंगाधिकार में नहीं मिलती है। ___गोम्मटसार के कर्मकाण्ड के चतुर्थ त्रिचूलिकाधिकार के अन्त में दस करणों की चर्चा करते हुए बन्ध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीरणा, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति और निकाचना - इन दस करणों के विवेचन के प्रसंग में गाथा क्रमांक ४३७ से ४५० तक गुणस्थान की अवधारणा का उल्लेख हुआ है । प्रथमतः यह बताया गया है कि अपूर्वकरण गुणस्थान से लेकर सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान तक, इन दस करणों में प्रथम सात करण ही होते हैं । उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली अवस्था में संक्रमण नहीं होता है । अतः इन गुणस्थानों में पूर्वोक्त सात में से संक्रमण के अभाव में छः करण ही होते हैं । अन्तिम अयोगी केवली गुणस्थान में सत्व और उदय ये दो करण ही होते हैं, किन्तु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उपशान्तमोह गुणस्थान में मिथ्यात्वमोह
और मिश्रमोह-इन दो कर्मप्रकृतियों का संक्रमण सम्भव है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान वाला पतित होते समय सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता में रही हुई कर्मप्रकृतियों का मिथ्यात्वमोह या मिश्रमोह में परिणमन करता है । इसी प्रकार आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान में उपशम, निधत्ति और निकाचना - इन तीन करणों की व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः उसमें सात करण ही होते है । अपूर्वकरण के पूर्व मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक दसों करण सम्भव होते है । अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में किसी करण की व्युच्छित्ति नहीं होती है, अतः इनमें सात करण ही होते है । सूक्ष्म संपराय नामक दसवें गुणस्थान के अन्तिम समय में संक्रमण की व्युच्छित्ति होती है, किन्तु क्षीणकषाय गुणस्थान में किसी करण की व्युच्छित्ति नहीं होती है, अतः उसमें छः करण भी होते हैं। सयोगी केवली गुणस्थान के अन्त समय में बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण और उदीरणा-इन चार करणों की व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः अयोगी केवली गुणस्थान में दो करण ही होते है, किन्तु अयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय में सत्व और उदय की भी व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः कोई भी करण शेष नहीं रहता है । इसप्रकार किन गुणस्थानों में कितने करण होते है और उनकी किस क्रम से व्युच्छित्ति होती है, यह समग्र चर्चा इस त्रिचूलिकाधिकार में गाथा क्रमांक ४३७ से ४५० तक की गई है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org