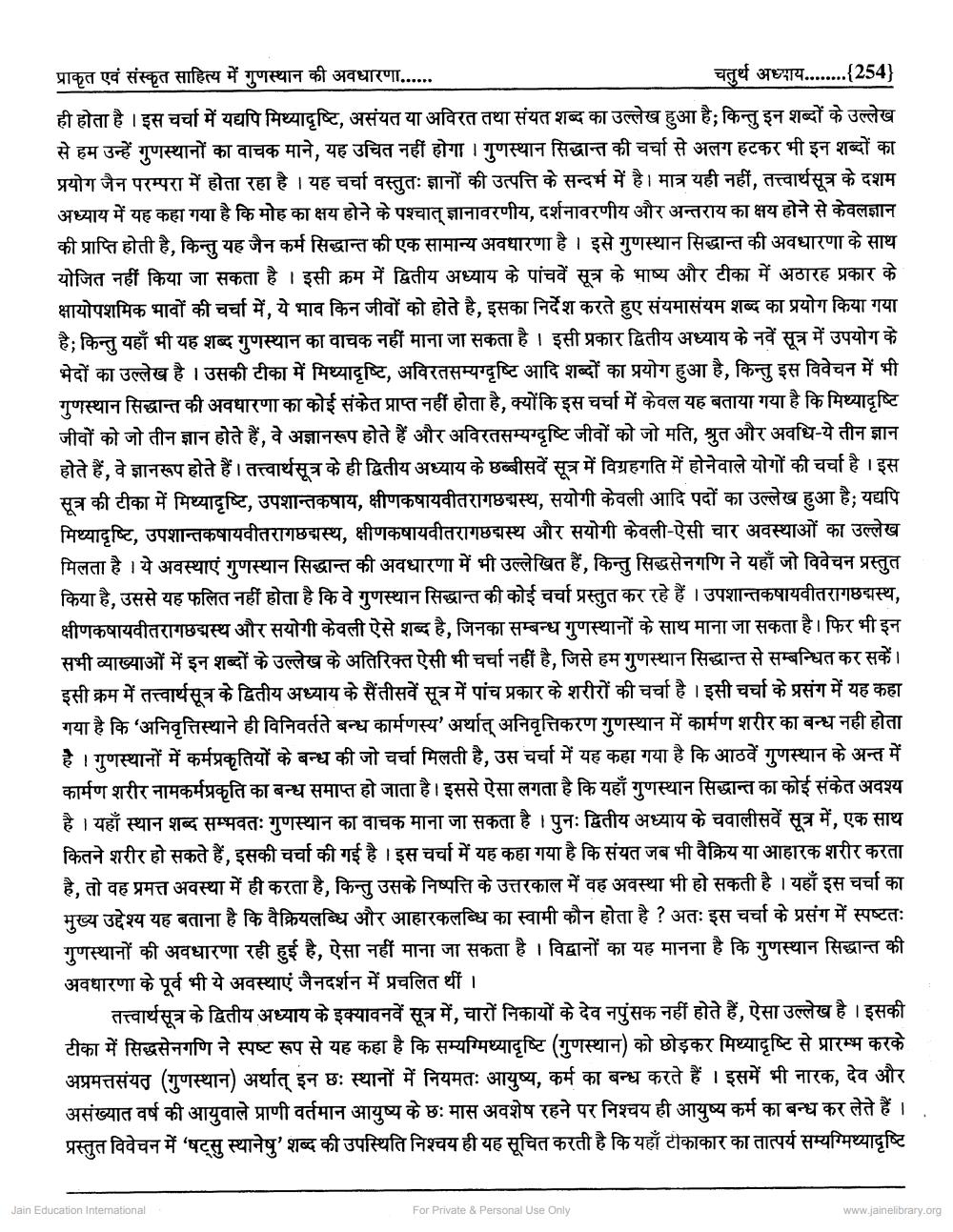________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा...
चतुर्थ अध्याय........{254)
ही होता है । इस चर्चा में यद्यपि मिथ्यादृष्टि, असंयत या अविरत तथा संयत शब्द का उल्लेख हुआ है; किन्तु इन शब्दों के उल्लेख से हम उन्हें गुणस्थानों का वाचक माने, यह उचित नहीं होगा । गुणस्थान सिद्धान्त की चर्चा से अलग हटकर भी इन शब्दों का प्रयोग जैन परम्परा में होता रहा है । यह चर्चा वस्तुतः ज्ञानों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में है। मात्र यही नहीं, तत्त्वार्थसूत्र के दशम अध्याय में यह कहा गया है कि मोह का क्षय होने के पश्चात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय का क्षय होने से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, किन्तु यह जैन कर्म सिद्धान्त की एक सामान्य अवधारणा है । इसे गुणस्थान सिद्धान्त की अवधारणा के साथ योजित नहीं किया जा सकता है । इसी क्रम में द्वितीय अध्याय के पांचवें सूत्र के भाष्य और टीका में अठारह प्रकार के क्षायोपशमिक भावों की चर्चा में, ये भाव किन जीवों को होते है, इसका निर्देश करते हुए संयमासंयम शब्द का प्रयोग किया गया है; किन्तु यहाँ भी यह शब्द गुणस्थान का वाचक नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार द्वितीय अध्याय के नवें सूत्र में उपयोग के भेदों का उल्लेख है । उसकी टीका में मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन्तु इस विवेचन में भी गुणस्थान सिद्धान्त की अवधारणा का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस चर्चा में केवल यह बताया गया है कि मिथ्यादृष्टि जीवों को जो तीन ज्ञान होते हैं, वे अज्ञानरूप होते हैं और अविरतसम्यग्दृष्टि जीवों को जो मति, श्रुत और अवधि-ये तीन ज्ञान होते हैं, वे ज्ञानरूप होते हैं। तत्त्वार्थसूत्र के ही द्वितीय अध्याय के छब्बीसवें सूत्र में विग्रहगति में होनेवाले योगों की चर्चा है । इस सूत्र की टीका में मिथ्यादृष्टि, उपशान्तकषाय, क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ, सयोगी केवली आदि पदों का उल्लेख हुआ है; यद्यपि मिथ्यादृष्टि, उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थ, क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ और सयोगी केवली-ऐसी चार अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है । ये अवस्थाएं गुणस्थान सिद्धान्त की अवधारणा में भी उल्लेखित हैं, किन्तु सिद्धसेनगणि ने यहाँ जो विवेचन प्रस्तुत किया है, उससे यह फलित नहीं होता है कि वे गुणस्थान सिद्धान्त की कोई चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं । उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थ, क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ और सयोगी केवली ऐसे शब्द है, जिनका सम्बन्ध गुणस्थानों के साथ माना जा सकता है। फिर भी इन सभी व्याख्याओं में इन शब्दों के उल्लेख के अतिरिक्त ऐसी भी चर्चा नहीं है, जिसे हम गणस्थान सिद्धान्त से सम्बन्धित कर सकें। इसी क्रम में तत्त्वार्थसूत्र के द्वितीय अध्याय के सैंतीसवें सूत्र में पांच प्रकार के शरीरों की चर्चा है । इसी चर्चा के प्रसंग में यह कहा गया है कि 'अनिवृत्तिस्थाने ही विनिवर्तते बन्ध कार्मणस्य' अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में कार्मण शरीर का बन्ध नही होता है । गुणस्थानों में कर्मप्रकृतियों के बन्ध की जो चर्चा मिलती है, उस चर्चा में यह कहा गया है कि आठवें गुणस्थान के अन्त में कार्मण शरीर नामकर्मप्रकृति का बन्ध समाप्त हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ गुणस्थान सिद्धान्त का कोई संकेत अवश्य है । यहाँ स्थान शब्द सम्भवतः गुणस्थान का वाचक माना जा सकता है । पुनः द्वितीय अध्याय के चवालीसवें सूत्र में, एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, इसकी चर्चा की गई है । इस चर्चा में यह कहा गया है कि संयत जब भी वैक्रिय या आहारक शरीर करता है, तो वह प्रमत्त अवस्था में ही करता है, किन्तु उसके निष्पत्ति के उत्तरकाल में वह अवस्था भी हो सकती है । यहाँ इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि वैक्रियलब्धि और आहारकलब्धि का स्वामी कौन होता है ? अतः इस चर्चा के प्रसंग में स्पष्टतः गुणस्थानों की अवधारणा रही हुई है, ऐसा नहीं माना जा सकता है । विद्वानों का यह मानना है कि गुणस्थान सिद्धान्त की अवधारणा के पूर्व भी ये अवस्थाएं जैनदर्शन में प्रचलित थीं।
तत्त्वार्थसूत्र के द्वितीय अध्याय के इक्यावनवें सूत्र में, चारों निकायों के देव नपुंसक नहीं होते हैं, ऐसा उल्लेख है । इसकी टीका में सिद्धसेनगणि ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि (गुणस्थान) को छोड़कर मिथ्यादृष्टि से प्रारम्भ करके अप्रमत्तसंयत (गुणस्थान) अर्थात् इन छः स्थानों में नियमतः आयुष्य, कर्म का बन्ध करते हैं । इसमें भी नारक, देव और असंख्यात वर्ष की आयुवाले प्राणी वर्तमान आयुष्य के छः मास अवशेष रहने पर निश्चय ही आयुष्य कर्म का बन्ध कर लेते हैं । प्रस्तुत विवेचन में 'षट्सु स्थानेषु' शब्द की उपस्थिति निश्चय ही यह सूचित करती है कि यहाँ टीकाकार का तात्पर्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org