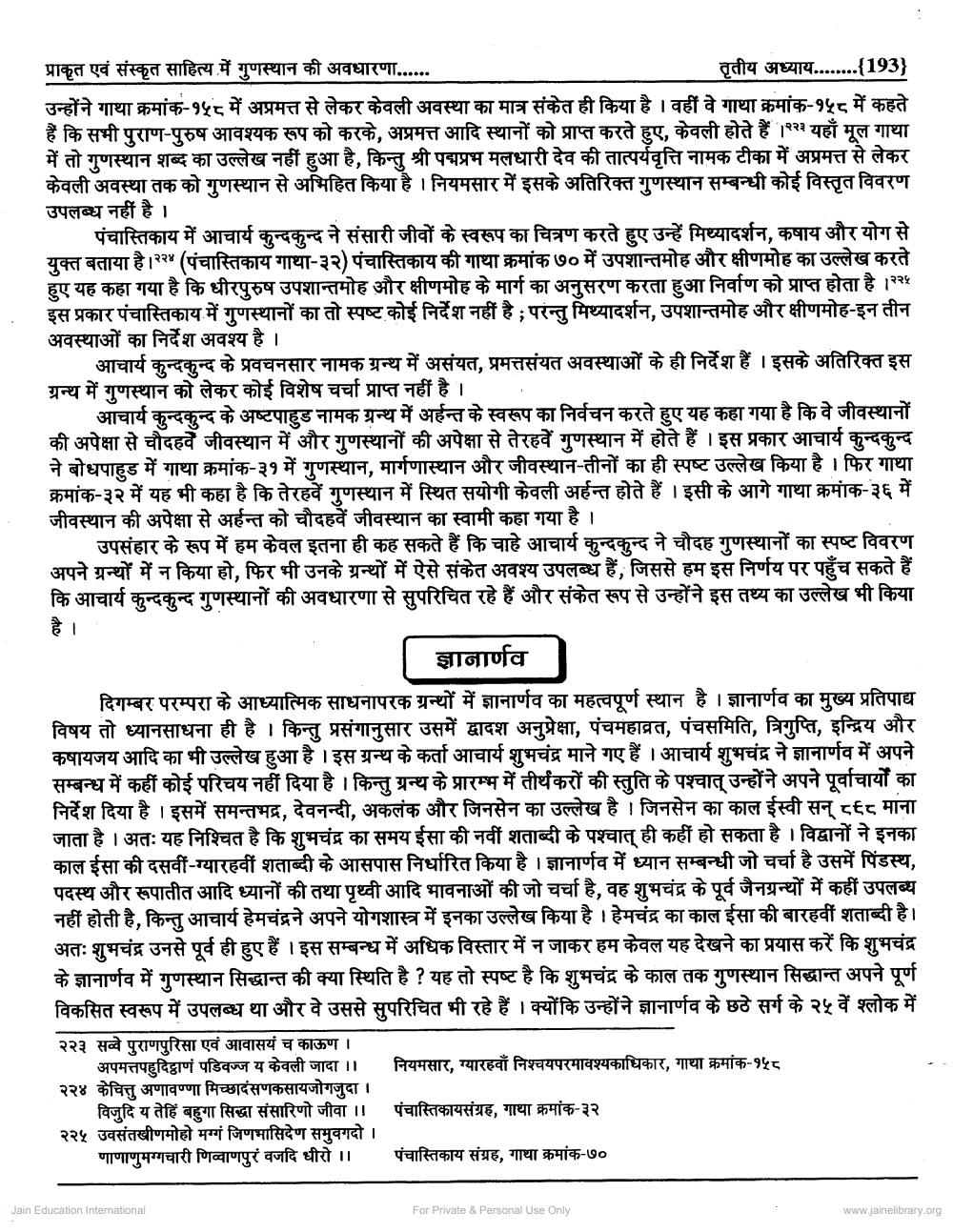________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
तृतीय अध्याय........{193} उन्होंने गाथा क्रमांक-१५८ में अप्रमत्त से लेकर केवली अवस्था का मात्र संकेत ही किया है । वहीं वे गाथा क्रमांक-१५८ में कहते हैं कि सभी पुराण-पुरुष आवश्यक रूप को करके, अप्रमत्त आदि स्थानों को प्राप्त करते हुए, केवली होते हैं ।२२३ यहाँ मूल गाथा में तो गुणस्थान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु श्री पद्मप्रभ मलधारी देव की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में अप्रमत्त से लेकर केवली अवस्था तक को गुणस्थान से अभिहित किया है । नियमसार में इसके अतिरिक्त गुणस्थान सम्बन्धी कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
पंचास्तिकाय में आचार्य कुन्दकुन्द ने संसारी जीवों के स्वरूप का चित्रण करते हुए उन्हें मिथ्यादर्शन, कषाय और योग से युक्त बताया है। २२४ (पंचास्तिकाय गाथा-३२) पंचास्तिकाय की गाथा क्रमांक ७० में उपशान्तमोह और क्षीणमोह का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि धीरपुरुष उपशान्तमोह और क्षीणमोह के मार्ग का अनुसरण करता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है । २२५ इस प्रकार पंचास्तिकाय में गुणस्थानों का तो स्पष्ट कोई निर्देश नहीं है; परन्तु मिथ्यादर्शन, उपशान्तमोह और क्षीणमोह-इन तीन अवस्थाओं का निर्देश अवश्य है ।
आचार्य कुन्दकुन्द के प्रवचनसार नामक ग्रन्थ में असंयत, प्रमत्तसंयत अवस्थाओं के ही निर्देश हैं । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में गुणस्थान को लेकर कोई विशेष चर्चा प्राप्त नहीं है।
आचार्य कुन्दकुन्द के अष्टपाहुड नामक ग्रन्थ में अर्हन्त के स्वरूप का निर्वचन करते हुए यह कहा गया है कि वे जीवस्थानों की अपेक्षा से चौदहवें जीवस्थान में और गुणस्थानों की अपेक्षा से तेरहवें गुणस्थान में होते हैं । इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द ने बोधपाहुड में गाथा क्रमांक-३१ में गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवस्थान-तीनों का ही स्पष्ट उल्लेख किया है । फिर गाथा क्रमांक-३२ में यह भी कहा है कि तेरहवें गुणस्थान में स्थित सयोगी केवली अर्हन्त होते हैं । इसी के आगे गाथा क्रमांक-३६ में जीवस्थान की अपेक्षा से अर्हन्त को चौदहवें जीवस्थान का स्वामी कहा गया है।
उपसंहार के रूप में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि चाहे आचार्य कुन्दकुन्द ने चौदह गुणस्थानों का स्पष्ट विवरण अपने ग्रन्थों में न किया हो, फिर भी उनके ग्रन्थों में ऐसे संकेत अवश्य उपलब्ध हैं, जिससे हम इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि आचार्य कुन्दकुन्द गुणस्थानों की अवधारणा से सुपरिचित रहे हैं और संकेत रूप से उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख भी किया
| ज्ञानार्णव । दिगम्बर परम्परा के आध्यात्मिक साधनापरक ग्रन्थों में ज्ञानार्णव का महत्वपूर्ण स्थान है । ज्ञानार्णव का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो ध्यानसाधना ही है । किन्तु प्रसंगानुसार उसमें द्वादश अनुप्रेक्षा, पंचमहाव्रत, पंचसमिति, त्रिगुप्ति, इन्द्रिय और कषायजय आदि का भी उल्लेख हुआ है । इस ग्रन्थ के कर्ता आचार्य शुभचंद्र माने गए हैं । आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में अपने सम्बन्ध में कहीं कोई परिचय नहीं दिया है। किन्तु ग्रन्थ के प्रारम्भ में तीर्थंकरों की स्तुति के पश्चात् उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों का निर्देश दिया है । इसमें समन्तभद्र, देवनन्दी, अकलंक और जिनसेन का उल्लेख है । जिनसेन का काल ईस्वी सन् ८६८ माना जाता है । अतः यह निश्चित है कि शुभचंद्र का समय ईसा की नवीं शताब्दी के पश्चात् ही कहीं हो सकता है । विद्वानों ने इनका काल ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास निर्धारित किया है । ज्ञानार्णव में ध्यान सम्बन्धी जो चर्चा है उसमें पिंडस्थ,
आदि ध्यानों की तथा पृथ्वी आदि भावनाओं की जो चर्चा है, वह शुभचंद्र के पूर्व जैनग्रन्थों में कहीं उपलब्ध नहीं होती है, किन्तु आचार्य हेमचंद्रने अपने योगशास्त्र में इनका उल्लेख किया है । हेमचंद्र का काल ईसा की बारहवीं शताब्दी है। अतः शुभचंद्र उनसे पूर्व ही हुए हैं । इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार में न जाकर हम केवल यह देखने का प्रयास करें कि शुभचंद्र के ज्ञानार्णव में गुणस्थान सिद्धान्त की क्या स्थिति है ? यह तो स्पष्ट है कि शुभचंद्र के काल तक गुणस्थान सिद्धान्त अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में उपलब्ध था और वे उससे सुपरिचित भी रहे हैं । क्योंकि उन्होंने ज्ञानार्णव के छठे सर्ग के २५ वें श्लोक में २२३ सव्वे पुराणपुरिसा एवं आवासयं च काऊण ।
___ अपमत्तपहुदिट्ठाणं पडिवज्ज य केवली जादा ।। नियमसार, ग्यारहवाँ निश्चयपरमावश्यकाधिकार, गाथा क्रमांक-१५८ २२४ केचित्तु अणावण्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा।
विजुदि य तेहिं बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा ।। पंचास्तिकायसंग्रह, गाथा क्रमांक-३२ २२५ उवसंतखीणमोहो मग्गं जिणभासिदेण समुवगदो ।
णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि धीरो ।। पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा क्रमांक-७०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
.
www.jainelibrary.org