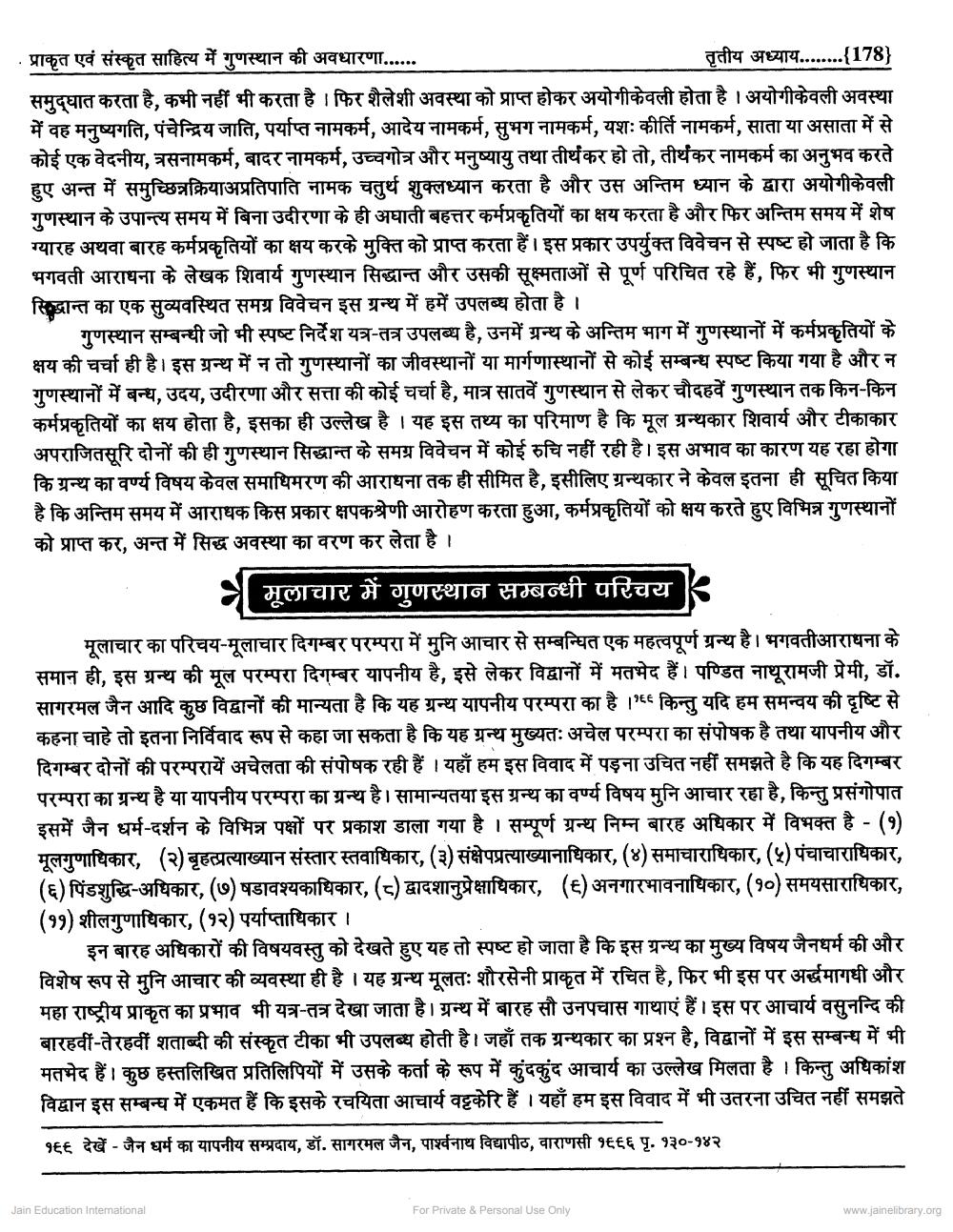________________
. प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
तृतीय अध्याय........{178} समुद्घात करता है, कभी नहीं भी करता है । फिर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होकर अयोगीकेवली होता है । अयोगीकेवली अवस्था में वह मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, पर्याप्त नामकर्म, आदेय नामकर्म, सुभग नामकर्म, यशः कीर्ति नामकर्म, साता या असाता में से कोई एक वेदनीय, त्रसनामकर्म, बादर नामकर्म, उच्चगोत्र और मनुष्यायु तथा तीर्थकर हो तो, तीर्थकर नामकर्म का अनुभव करते हुए अन्त में समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाति नामक चतुर्थ शुक्लध्यान करता है और उस अन्तिम ध्यान के द्वारा अयोगीकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय में बिना उदीरणा के ही अघाती बहत्तर कर्मप्रकृतियों का क्षय करता है और फिर अन्तिम समय में शेष ग्यारह अथवा बारह कर्मप्रकृतियों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करता हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवती आराधना के लेखक शिवार्य गुणस्थान सिद्धान्त और उसकी सूक्ष्मताओं से पूर्ण परिचित रहे हैं, फिर भी गुणस्थान सिद्धान्त का एक सुव्यवस्थित समग्र विवेचन इस ग्रन्थ में हमें उपलब्ध होता है।
गुणस्थान सम्बन्धी जो भी स्पष्ट निर्देश यत्र-तत्र उपलब्ध है, उनमें ग्रन्थ के अन्तिम भाग में गुणस्थानों में कर्मप्रकृतियों के क्षय की चर्चा ही है। इस ग्रन्थ में न तो गुणस्थानों का जीवस्थानों या मार्गणास्थानों से कोई सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है और न गुणस्थानों में बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता की कोई चर्चा है, मात्र सातवें गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक किन-किन कर्मप्रकृतियों का क्षय होता है, इसका ही उल्लेख है । यह इस तथ्य का परिमाण है कि मूल ग्रन्थकार शिवार्य और टीकाकार अपराजितसूरि दोनों की ही गुणस्थान सिद्धान्त के समग्र विवेचन में कोई रुचि नहीं रही है। इस अभाव का कि ग्रन्थ का वर्ण्य विषय केवल समाधिमरण की आराधना तक ही सीमित है, इसीलिए ग्रन्थकार ने केवल इतना ही सचित किय है कि अन्तिम समय में आराधक किस प्रकार क्षपकश्रेणी आरोहण करता हुआ, कर्मप्रकृतियों को क्षय करते हुए विभिन्न गुणस्थानों को प्राप्त कर, अन्त में सिद्ध अवस्था का वरण कर लेता है।
नमूलाचार में गुणस्थान सम्बन्धी परिचय :
मूलाचार का परिचय-मूलाचार दिगम्बर परम्परा में मुनि आचार से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। भगवतीआराधना के समान ही, इस ग्रन्थ की मूल परम्परा दिगम्बर यापनीय है, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। पण्डित नाथूरामजी प्रेमी, डॉ. सागरमल जैन आदि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह ग्रन्थ यापनीय परम्परा का है । ६६ किन्तु यदि हम समन्वय की दृष्टि से कहना चाहे तो इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ मुख्यतः अचेल परम्परा का संपोषक है तथा यापनीय और दिगम्बर दोनों की परम्परायें अचेलता की संपोषक रही हैं । यहाँ हम इस विवाद में पड़ना उचित नहीं समझते है कि यह दिगम्बर परम्परा का ग्रन्थ है या यापनीय परम्परा का ग्रन्थ है। सामान्यतया इस ग्रन्थ का वर्ण्य विषय मुनि आचार रहा है, किन्तु प्रसंगोपात इसमें जैन धर्म-दर्शन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । सम्पूर्ण ग्रन्थ निम्न बारह अधिकार में विभक्त है - (१) मूलगुणाधिकार, (२) बृहत्प्रत्याख्यान संस्तार स्तवाधिकार, (३) संक्षेपप्रत्याख्यानाधिकार, (४) समाचाराधिकार, (५) पंचाचाराधिकार, (६)पिंडशुद्धि-अधिकार, (७) षडावश्यकाधिकार, (८) द्वादशानुप्रेक्षाधिकार, (E) अनगारभावनाधिकार, (१०) समयसाराधिकार, (११) शीलगुणाधिकार, (१२) पर्याप्ताधिकार ।
इन बारह अधिकारों की विषयवस्तु को देखते हुए यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थ का मुख्य विषय जैनधर्म की और विशेष रूप से मुनि आचार की व्यवस्था ही है । यह ग्रन्थ मूलतः शौरसेनी प्राकृत में रचित है, फिर भी इस पर अर्द्धमागधी और महा राष्ट्रीय प्राकृत का प्रभाव भी यत्र-तत्र देखा जाता है। ग्रन्थ में बारह सौ उनपचास गाथाएं हैं। इस पर आचार्य वसुनन्दि की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी की संस्कृत टीका भी उपलब्ध होती है। जहाँ तक ग्रन्थकार का प्रश्न है, विद्वानों में इस सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। कुछ हस्तलिखित प्रतिलिपियों में उसके कर्ता के रूप में कुंदकुंद आचार्य का उल्लेख मिलता है । किन्तु अधिकांश विद्वान इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि इसके रचयिता आचार्य वट्टकेरि हैं । यहाँ हम इस विवाद में भी उतरना उचित नहीं समझते
१६६ देखें - जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय, डॉ. सागरमल जैन, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी १६६६ पृ. १३०-१४२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org