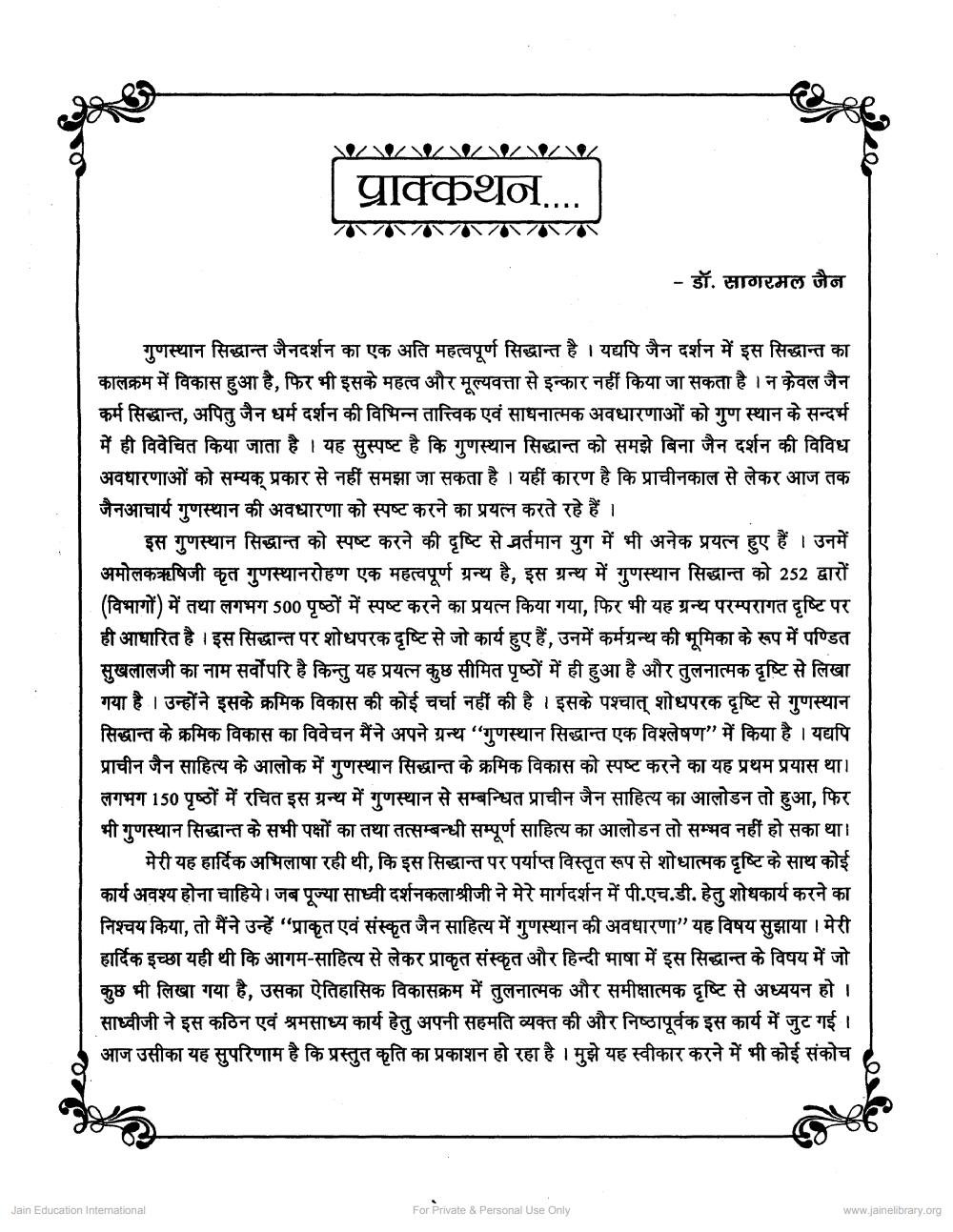________________
प्राक्कथन
Jain Education International
गुणस्थान सिद्धान्त जैनदर्शन का एक अति महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । यद्यपि जैन दर्शन में इस सिद्धान्त का कालक्रम में विकास हुआ है, फिर भी इसके महत्व और मूल्यवत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता है । न केवल जैन कर्म सिद्धान्त, अपितु जैन धर्म दर्शन की विभिन्न तात्त्विक एवं साधनात्मक अवधारणाओं को गुण स्थान के सन्दर्भ में ही विवेचित किया जाता है । यह सुस्पष्ट है कि गुणस्थान सिद्धान्त को समझे बिना जैन दर्शन की विविध अवधारणाओं को सम्यक् प्रकार से नहीं समझा जा सकता है । यहीं कारण है कि प्राचीनकाल से लेकर आज तक जैन आचार्य गुणस्थान की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते रहे हैं ।
इस गुणस्थान सिद्धान्त को स्पष्ट करने की दृष्टि से वर्तमान युग में भी अनेक प्रयत्न हुए हैं । उनमें अमोलकऋषिजी कृत गुणस्थानरोहण एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, इस ग्रन्थ में गुणस्थान सिद्धान्त को 252 द्वारों ( विभागों) में तथा लगभग 500 पृष्ठों में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया, फिर भी यह ग्रन्थ परम्परागत दृष्टि पर ही आधारित है । इस सिद्धान्त पर शोधपरक दृष्टि से जो कार्य हुए हैं, उनमें कर्मग्रन्थ की भूमिका के रूप में पण्डित सुखलालजी का नाम सर्वोपरि है किन्तु यह प्रयत्न कुछ सीमित पृष्ठों में ही हुआ है और तुलनात्मक दृष्टि से लिखा गया है । उन्होंने इसके क्रमिक विकास की कोई चर्चा नहीं की है । इसके पश्चात् शोधपरक दृष्टि से गुणस्थान सिद्धान्त के क्रमिक विकास का विवेचन मैंने अपने ग्रन्थ " गुणस्थान सिद्धान्त एक विश्लेषण" में किया है । यद्यपि प्राचीन जैन साहित्य के आलोक में गुणस्थान सिद्धान्त के क्रमिक विकास को स्पष्ट करने का यह प्रथम प्रयास था। लगभग 150 पृष्ठों में रचित इस ग्रन्थ में गुणस्थान से सम्बन्धित प्राचीन जैन साहित्य का आलोडन तो हुआ, फिर भी गुणस्थान सिद्धान्त के सभी पक्षों का तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का आलोडन तो सम्भव नहीं हो सका था। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा रही थी, कि इस सिद्धान्त पर पर्याप्त विस्तृत रूप से शोधात्मक दृष्टि के साथ कोई कार्य अवश्य होना चाहिये। जब पूज्या साध्वी दर्शनकला श्रीजी ने मेरे मार्गदर्शन में पी. एच. डी. हेतु शोधकार्य करने का निश्चय किया, तो मैंने उन्हें "प्राकृत एवं संस्कृत जैन साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा " यह विषय सुझाया । मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि आगम-साहित्य से लेकर प्राकृत संस्कृत और हिन्दी भाषा में इस सिद्धान्त के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है, उसका ऐतिहासिक विकासक्रम में तुलनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से अध्ययन हो । साध्वीजी ने इस कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य हेतु अपनी सहमति व्यक्त की और निष्ठापूर्वक इस कार्य में जुट गई । आज उसीका यह सुपरिणाम है कि प्रस्तुत कृति का प्रकाशन हो रहा है । मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई संकोच
डॉ. सागरमल जैन
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org