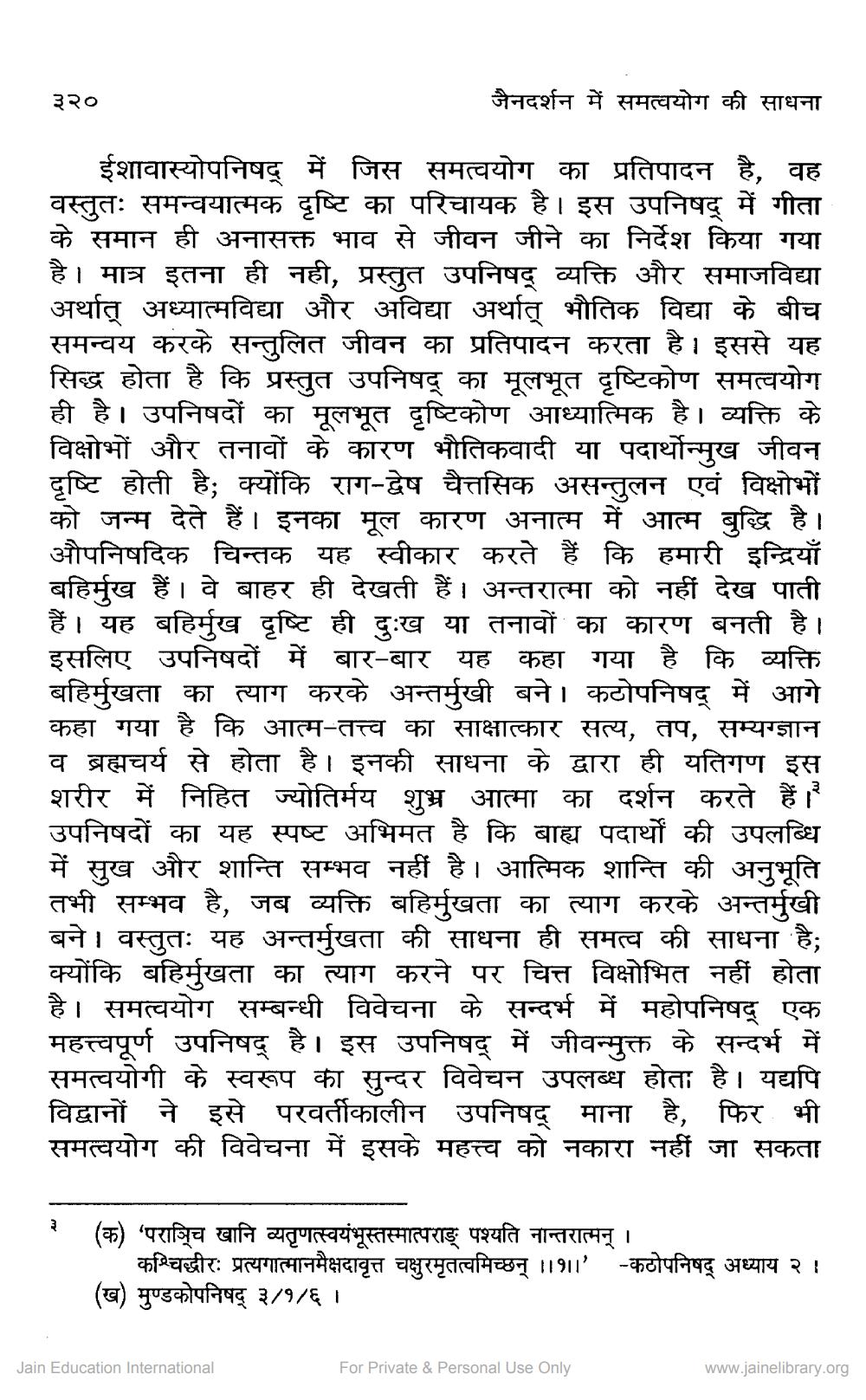________________
३२०
जैनदर्शन में समत्वयोग की साधना
ईशावास्योपनिषद् में जिस समत्वयोग का प्रतिपादन है, वह वस्तुतः समन्वयात्मक दृष्टि का परिचायक है। इस उपनिषद् में गीता के समान ही अनासक्त भाव से जीवन जीने का निर्देश किया गया है। मात्र इतना ही नही, प्रस्तुत उपनिषद् व्यक्ति और समाजविद्या अर्थात् अध्यात्मविद्या और अविद्या अर्थात् भौतिक विद्या के बीच समन्वय करके सन्तुलित जीवन का प्रतिपादन करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत उपनिषद् का मूलभूत दृष्टिकोण समत्वयोग ही है। उपनिषदों का मूलभूत दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। व्यक्ति के विक्षोभों और तनावों के कारण भौतिकवादी या पदार्थोन्मुख जीवन दृष्टि होती है; क्योंकि राग-द्वेष चैत्तसिक असन्तुलन एवं विक्षोभों को जन्म देते हैं। इनका मूल कारण अनात्म में आत्म बुद्धि है। औपनिषदिक चिन्तक यह स्वीकार करते हैं कि हमारी इन्द्रियाँ बहिर्मुख हैं। वे बाहर ही देखती हैं। अन्तरात्मा को नहीं देख पाती हैं। यह बहिर्मुख दृष्टि ही दुःख या तनावों का कारण बनती है। इसलिए उपनिषदों में बार-बार यह कहा गया है कि व्यक्ति बहिर्मुखता का त्याग करके अन्तर्मुखी बने। कठोपनिषद् में आगे कहा गया है कि आत्म-तत्त्व का साक्षात्कार सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान व ब्रह्मचर्य से होता है। इनकी साधना के द्वारा ही यतिगण इस शरीर में निहित ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा का दर्शन करते हैं। उपनिषदों का यह स्पष्ट अभिमत है कि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि में सुख और शान्ति सम्भव नहीं है। आत्मिक शान्ति की अनुभूति तभी सम्भव है, जब व्यक्ति बहिर्मुखता का त्याग करके अन्तर्मुखी बने। वस्तुतः यह अन्तर्मुखता की साधना ही समत्व की साधना है; क्योंकि बहिर्मुखता का त्याग करने पर चित्त विक्षोभित नहीं होता है। समत्वयोग सम्बन्धी विवेचना के सन्दर्भ में महोपनिषद् एक महत्त्वपूर्ण उपनिषद् है। इस उपनिषद् में जीवन्मुक्त के सन्दर्भ में समत्वयोगी के स्वरूप का सुन्दर विवेचन उपलब्ध होता है। यद्यपि विद्वानों ने इसे परवर्तीकालीन उपनिषद् माना है, फिर भी समत्वयोग की विवेचना में इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता
(क) 'पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन् ।।१।।' -कठोपनिषद् अध्याय २ । (ख) मुण्डकोपनिषद् ३/१/६ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org