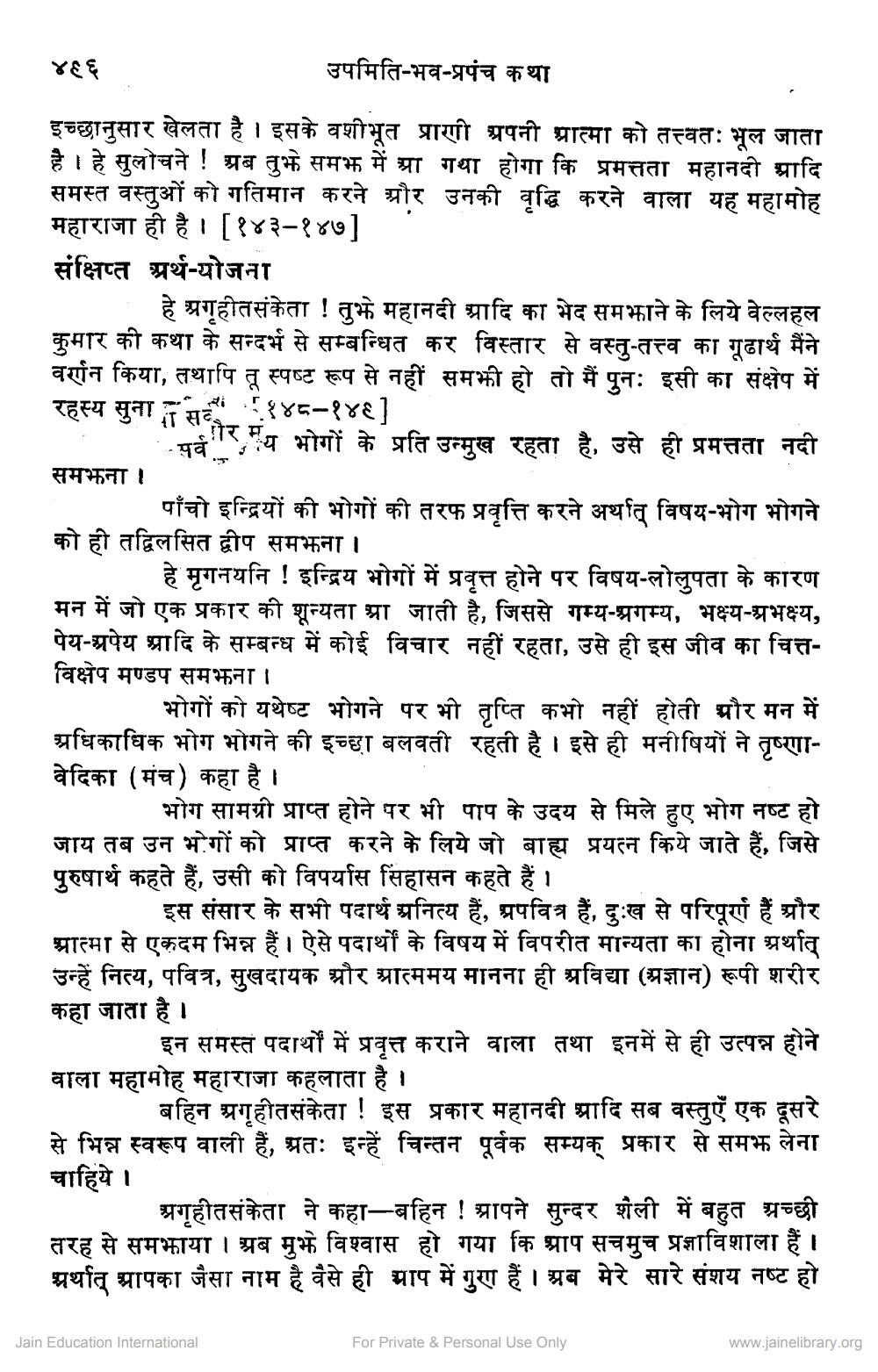________________
उपमिति-भव-प्रपंच कथा
इच्छानुसार खेलता है । इसके वशीभूत प्राणी अपनी प्रात्मा को तत्त्वतः भूल जाता है। हे सुलोचने ! अब तुझे समझ में आ गया होगा कि प्रमत्तता महानदी आदि समस्त वस्तुओं को गतिमान करने और उनकी वृद्धि करने वाला यह महामोह महाराजा ही है । [१४३-१४७] संक्षिप्त अर्थ-योजना
हे अगृहीतसंकेता ! तुझे महानदी आदि का भेद समझाने के लिये वेल्लहल कुमार की कथा के सन्दर्भ से सम्बन्धित कर विस्तार से वस्तु-तत्त्व का गूढार्थ मैंने वर्णन किया, तथापि तू स्पष्ट रूप से नहीं समझी हो तो मैं पुनः इसी का संक्षेप में रहस्य सुनासिर १४८-१४६]
पर्व पर मय भोगों के प्रति उन्मुख रहता है, उसे ही प्रमत्तता नदी समझना।
पाँचो इन्द्रियों की भोगों की तरफ प्रवृत्ति करने अर्थात् विषय-भोग भोगने को ही तद्विलसित द्वीप समझना।
हे मृगनयनि ! इन्द्रिय भोगों में प्रवृत्त होने पर विषय-लोलुपता के कारण मन में जो एक प्रकार की शून्यता आ जाती है, जिससे गम्य-अगम्य, भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय आदि के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं रहता, उसे ही इस जीव का चित्तविक्षेप मण्डप समझना।
__ भोगों को यथेष्ट भोगने पर भी तृप्ति कभी नहीं होती और मन में अधिकाधिक भोग भोगने की इच्छा बलवती रहती है। इसे ही मनीषियों ने तृष्णावेदिका (मंच) कहा है।
भोग सामग्री प्राप्त होने पर भी पाप के उदय से मिले हए भोग नष्ट हो जाय तब उन भोगों को प्राप्त करने के लिये जो बाह्य प्रयत्न किये जाते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को विपर्यास सिंहासन कहते हैं।
इस संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, अपवित्र हैं, दुःख से परिपूर्ण हैं और प्रात्मा से एकदम भिन्न हैं। ऐसे पदार्थों के विषय में विपरीत मान्यता का होना अर्थात् उन्हें नित्य, पवित्र, सुखदायक और आत्ममय मानना ही अविद्या (अज्ञान) रूपी शरीर कहा जाता है।
इन समस्त पदार्थों में प्रवृत्त कराने वाला तथा इनमें से ही उत्पन्न होने वाला महामोह महाराजा कहलाता है।
बहिन अगृहीतसंकेता ! इस प्रकार महानदी आदि सब वस्तुएँ एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाली हैं, अतः इन्हें चिन्तन पूर्वक सम्यक् प्रकार से समझ लेना चाहिये।
अगृहीतसंकेता ने कहा-बहिन ! आपने सुन्दर शैली में बहुत अच्छी तरह से समझाया । अब मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच प्रज्ञाविशाला हैं। अर्थात् आपका जैसा नाम है वैसे ही माप में गुण हैं । अब मेरे सारे संशय नष्ट हो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org