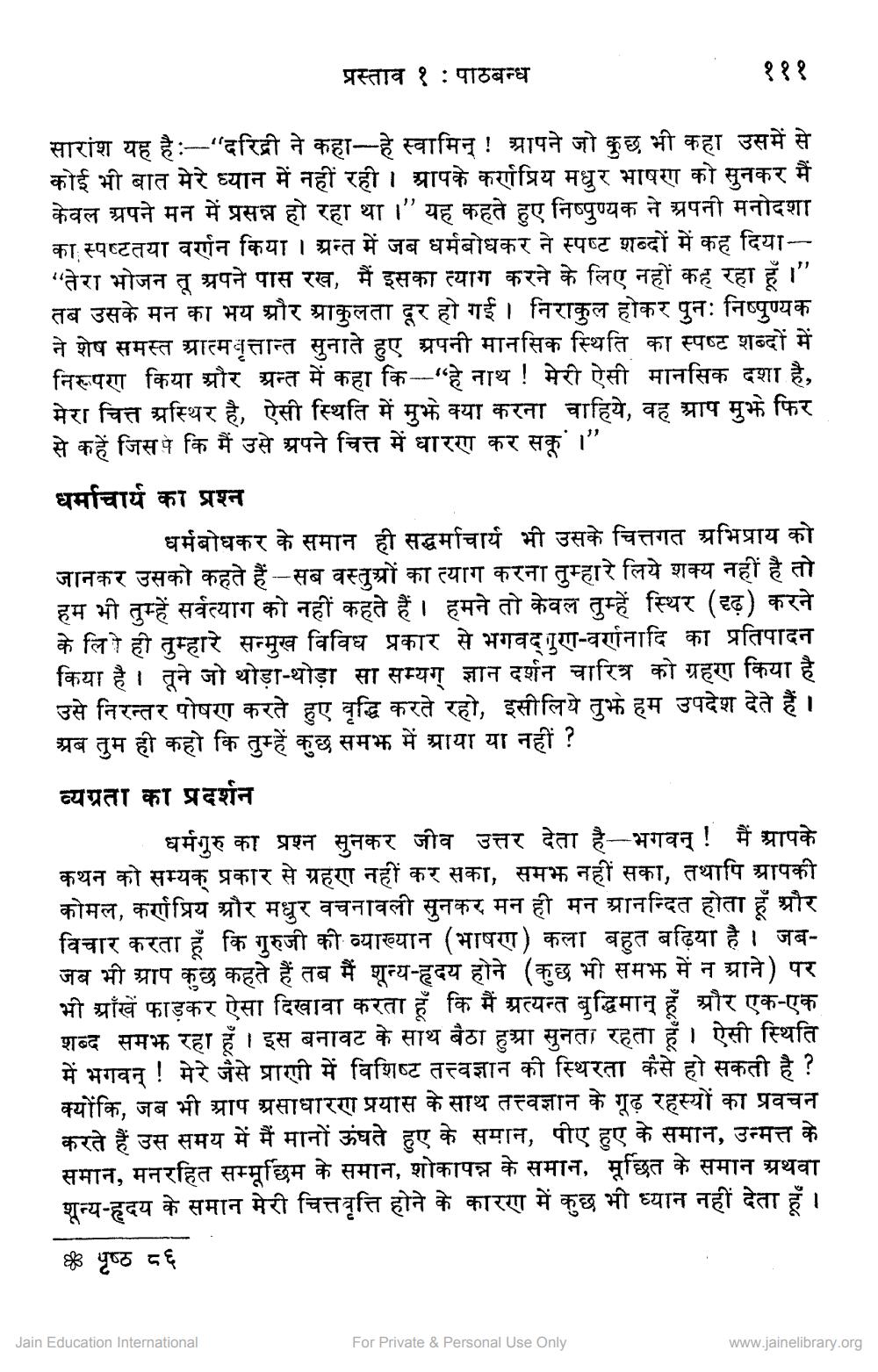________________
प्रस्ताव १ : पाठबन्ध
१११
सारांश यह है :-"दरिद्री ने कहा-हे स्वामिन् ! आपने जो कुछ भी कहा उसमें से कोई भी बात मेरे ध्यान में नहीं रही। आपके कर्णप्रिय मधुर भाषण को सुनकर मैं केवल अपने मन में प्रसन्न हो रहा था ।" यह कहते हुए निष्पुण्यक ने अपनी मनोदशा का स्पष्टतया वर्णन किया। अन्त में जब धर्मबोधकर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया"तेरा भोजन तू अपने पास रख, मैं इसका त्याग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ।" तब उसके मन का भय और आकुलता दूर हो गई। निराकुल होकर पुनः निष्पुण्यक ने शेष समस्त आत्मवृत्तान्त सुनाते हुए अपनी मानसिक स्थिति का स्पष्ट शब्दों में निरूपण किया और अन्त में कहा कि- "हे नाथ ! मेरी ऐसी मानसिक दशा है, मेरा चित्त अस्थिर है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये, वह आप मुझे फिर से कहें जिससे कि मैं उसे अपने चित्त में धारण कर सकू।" धर्माचार्य का प्रश्न
धर्मबोधकर के समान ही सद्धर्माचार्य भी उसके चित्तगत अभिप्राय को जानकर उसको कहते हैं-सब वस्तुओं का त्याग करना तुम्हारे लिये शक्य नहीं है तो हम भी तुम्हें सर्वत्याग को नहीं कहते हैं। हमने तो केवल तुम्हें स्थिर (दृढ़) करने के लिये ही तुम्हारे सन्मुख विविध प्रकार से भगवद् गुरण-वर्णनादि का प्रतिपादन किया है। तूने जो थोड़ा-थोड़ा सा सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र को ग्रहण किया है उसे निरन्तर पोषण करते हुए वृद्धि करते रहो, इसीलिये तुझे हम उपदेश देते हैं। अब तुम ही कहो कि तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं ? व्यग्रता का प्रदर्शन
धर्मगुरु का प्रश्न सुनकर जीव उत्तर देता है-भगवन् ! मैं आपके कथन को सम्यक् प्रकार से ग्रहण नहीं कर सका, समझ नहीं सका, तथापि आपकी कोमल, कर्णप्रिय और मधुर वचनावली सुनकर मन ही मन आनन्दित होता हूँ और विचार करता हूँ कि गुरुजी की व्याख्यान (भाषण) कला बहुत बढ़िया है। जबजब भी आप कुछ कहते हैं तब मैं शून्य-हृदय होने (कुछ भी समझ में न आने) पर भी आँखें फाड़कर ऐसा दिखावा करता हूँ कि मैं अत्यन्त बुद्धिमान् हूँ और एक-एक शब्द समझ रहा हूँ। इस बनावट के साथ बैठा हुआ सुनता रहता हूँ। ऐसी स्थिति में भगवन् ! मेरे जैसे प्राणी में विशिष्ट तत्त्वज्ञान की स्थिरता कैसे हो सकती है ? क्योंकि, जब भी आप असाधारण प्रयास के साथ तत्त्वज्ञान के गूढ़ रहस्यों का प्रवचन करते हैं उस समय में मैं मानों ऊंघते हुए के समान, पीए हुए के समान, उन्मत्त के समान, मनरहित सम्मूछिम के समान, शोकापन्न के समान, मूछित के समान अथवा शून्य-हृदय के समान मेरी चित्तवृत्ति होने के कारण में कुछ भी ध्यान नहीं देता हूँ। * पृष्ठ ८६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org