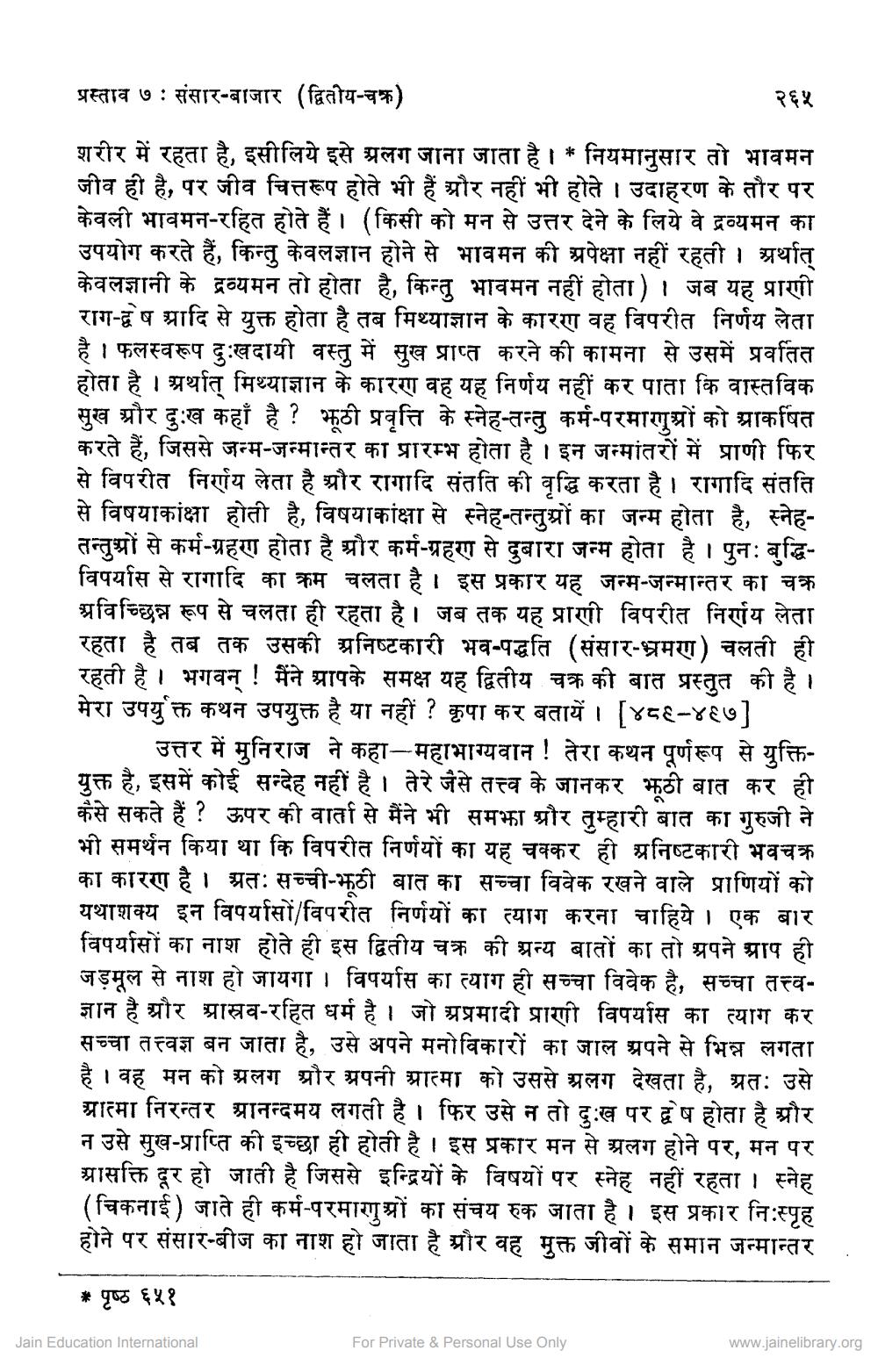________________
प्रस्ताव ७ : संसार-बाजार (द्वितीय-चक्र)
२६५
शरीर में रहता है, इसीलिये इसे अलग जाना जाता है। * नियमानुसार तो भावमन जीव ही है, पर जीव चित्तरूप होते भी हैं और नहीं भी होते । उदाहरण के तौर पर केवली भावमन-रहित होते हैं। (किसी को मन से उत्तर देने के लिये वे द्रव्यमन का उपयोग करते हैं, किन्तु केवलज्ञान होने से भावमन की अपेक्षा नहीं रहती। अर्थात् केवलज्ञानी के द्रव्यमन तो होता है, किन्तु भावमन नहीं होता)। जब यह प्राणी राग-द्वेष आदि से युक्त होता है तब मिथ्याज्ञान के कारण वह विपरीत निर्णय लेता है । फलस्वरूप दुःखदायी वस्तु में सुख प्राप्त करने की कामना से उसमें प्रवर्तित होता है । अर्थात् मिथ्याज्ञान के कारण वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तविक सुख और दुःख कहाँ है ? झूठी प्रवृत्ति के स्नेह-तन्तु कर्म-परमाणुओं को आकर्षित करते हैं, जिससे जन्म-जन्मान्तर का प्रारम्भ होता है । इन जन्मांतरों में प्राणी फिर से विपरीत निर्णय लेता है और रागादि संतति की वृद्धि करता है। रागादि संतति से विषयाकांक्षा होती है, विषयाकांक्षा से स्नेह-तन्तुओं का जन्म होता है, स्नेहतन्तुओं से कर्म-ग्रहण होता है और कर्म-ग्रहण से दुबारा जन्म होता है । पुनः बुद्धिविपर्यास से रागादि का क्रम चलता है। इस प्रकार यह जन्म-जन्मान्तर का चक्र अविच्छिन्न रूप से चलता ही रहता है। जब तक यह प्राणी विपरीत निर्णय लेता रहता है तब तक उसकी अनिष्टकारी भव-पद्धति (संसार-भ्रमण) चलती ही रहती है। भगवन् ! मैंने आपके समक्ष यह द्वितीय चक्र की बात प्रस्तुत की है । मेरा उपर्युक्त कथन उपयुक्त है या नहीं ? कृपा कर बतायें। [४८६-४६७]
उत्तर में मुनिराज ने कहा-महाभाग्यवान ! तेरा कथन पूर्णरूप से युक्तियुक्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। तेरे जैसे तत्त्व के जानकर झूठी बात कर ही कैसे सकते हैं ? ऊपर की वार्ता से मैंने भी समझा और तुम्हारी बात का गुरुजी ने भी समर्थन किया था कि विपरीत निर्णयों का यह चक्कर ही अनिष्टकारी भवचक्र का कारण है। अतः सच्ची-झूठी बात का सच्चा विवेक रखने वाले प्राणियों को यथाशक्य इन विपर्यासों/विपरीत निर्णयों का त्याग करना चाहिये । एक बार विपर्यासों का नाश होते ही इस द्वितीय चक्र की अन्य बातों का तो अपने आप ही जड़मूल से नाश हो जायगा। विपर्यास का त्याग ही सच्चा विवेक है, सच्चा तत्त्वज्ञान है और प्रास्रव-रहित धर्म है। जो अप्रमादी प्राणी विपर्यास का त्याग कर सच्चा तत्त्वज्ञ बन जाता है, उसे अपने मनोविकारों का जाल अपने से भिन्न लगता है । वह मन को अलग और अपनी आत्मा को उससे अलग देखता है, अतः उसे
आत्मा निरन्तर आनन्दमय लगती है। फिर उसे न तो दुःख पर द्वेष होता है और न उसे सुख-प्राप्ति की इच्छा ही होती है । इस प्रकार मन से अलग होने पर, मन पर आसक्ति दूर हो जाती है जिससे इन्द्रियों के विषयों पर स्नेह नहीं रहता। स्नेह (चिकनाई) जाते ही कर्म-परमाणुओं का संचय रुक जाता है। इस प्रकार निःस्पृह होने पर संसार-बीज का नाश हो जाता है और वह मुक्त जीवों के समान जन्मान्तर
* पृष्ठ ६५१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org