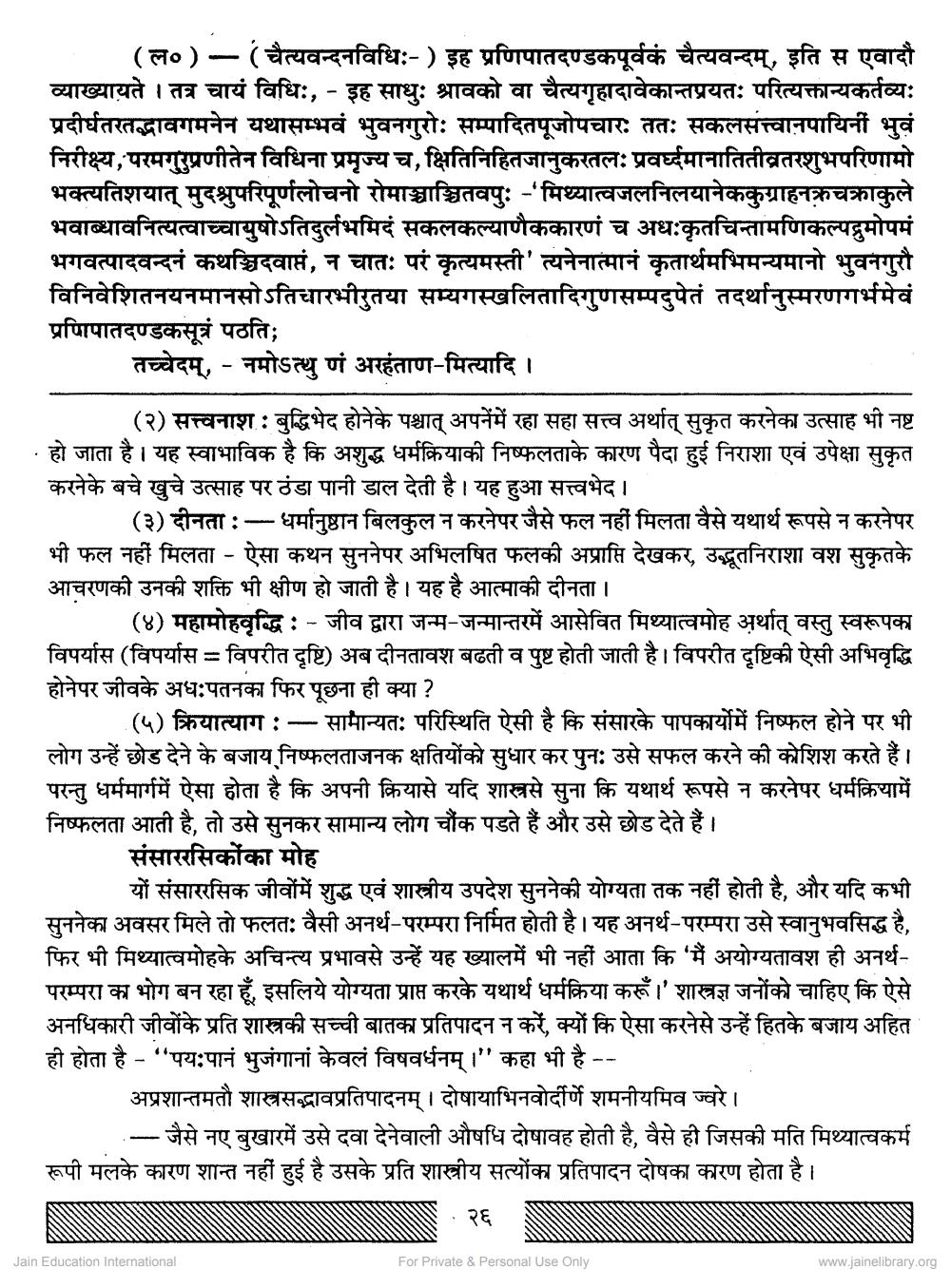________________
ad
( ल० ) (चैत्यवन्दनविधि:- ) इह प्रणिपातदण्डकपूर्वकं चैत्यवन्दम्, इति स एवादौ व्याख्यायते । तत्र चायं विधिः, - इह साधुः श्रावको वा चैत्यगृहादावेकान्तप्रयतः परित्यक्तान्यकर्तव्यः प्रदीर्घतरतद्भावगमनेन यथासम्भवं भुवनगुरोः सम्पादितपूजोपचारः ततः सकलसंत्त्वानपायिनीं भुवं निरीक्ष्य, परमगुरुप्रणीतेन विधिना प्रमृज्य च, क्षितिनिहितजानुकरतलः प्रवर्द्धमानातितीव्रतरशुभपरिणामो भक्त्यतिशयात् मुदश्रुपरिपूर्णलोचनो रोमाञ्चाञ्चितवपुः - 'मिथ्यात्वजलनिलयानेककुग्राहनक्रचक्राकुले भवाब्धावनित्यत्वाच्चायुषोऽतिदुर्लभमिदं सकलकल्याणैककारणं च अधः कृतचिन्तामणिकल्पद्रुमोपमं भगवत्पादवन्दनं कथञ्चिदवाप्तं, न चातः परं कृत्यमस्ती' त्यनेनात्मानं कृतार्थमभिमन्यमानो भुवनगुरौ विनिवेशितनयनमानसोऽतिचारभीरुतया सम्यगस्खलितादिगुणसम्पदुपेतं तदर्थानुस्मरणगर्भमेवं प्रणिपातदण्डकसूत्रं पठति;
तच्चेदम्, - नमोऽत्थु णं अरहंताण - मित्यादि ।
(२) सत्त्वनाश: बुद्धिभेद होनेके पश्चात् अपनेंमें रहा सहा सत्त्व अर्थात् सुकृत करनेका उत्साह भी नष्ट हो जाता है। यह स्वाभाविक है कि अशुद्ध धर्मक्रियाकी निष्फलताके कारण पैदा हुई निराशा एवं उपेक्षा सुकृत करनेके बचे खुचे उत्साह पर ठंडा पानी डाल देती है। यह हुआ सत्त्वभेद ।
(३) दीनता : - - धर्मानुष्ठान बिलकुल न करनेपर जैसे फल नहीं मिलता वैसे यथार्थ रूपसे न करनेपर भी फल नहीं मिलता - ऐसा कथन सुननेपर अभिलषित फलकी अप्राप्ति देखकर, उद्भूतनिराशा वश सुकृतके आचरणकी उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। यह है आत्माकी दीनता ।
(४) महामोहवृद्धि : - जीव द्वारा जन्म-जन्मान्तरमें आसेवित मिथ्यात्वमोह अर्थात् वस्तु स्वरूपका विपर्यास (विपर्यास = विपरीत दृष्टि) अब दीनतावश बढती व पुष्ट होती जाती है। विपरीत दृष्टिकी ऐसी अभिवृद्धि होनेपर जीवके अधःपतनका फिर पूछना ही क्या ?
(५) क्रियात्याग : सामान्यतः परिस्थिति ऐसी है कि संसारके पापकार्योंमें निष्फल होने पर भी लोग उन्हें छोड़ देने बजाय निष्फलताजनक क्षतियोंको सुधार कर पुनः उसे सफल करने की कोशिश करते हैं । परन्तु धर्ममार्गमें ऐसा होता है कि अपनी क्रियासे यदि शास्त्रसे सुना कि यथार्थ रूपसे न करनेपर धर्मक्रियामें निष्फलता आती है, तो उसे सुनकर सामान्य लोग चौंक पडते हैं और उसे छोड देते हैं ।
संसाररसिकोंका मोह
यों संसाररसिक जीवोंमें शुद्ध एवं शास्त्रीय उपदेश सुननेकी योग्यता तक नहीं होती है, और यदि कभी सुननेका अवसर मिले तो फलत: वैसी अनर्थ-परम्परा निर्मित होती है । यह अनर्थ - परम्परा उसे स्वानुभवसिद्ध है, फिर भी मिथ्यात्वमोहके अचिन्त्य प्रभावसे उन्हें यह ख्यालमें भी नहीं आता कि 'मैं अयोग्यतावश ही अनर्थपरम्परा का भोग बन रहा हूँ, इसलिये योग्यता प्राप्त करके यथार्थ धर्मक्रिया करूँ।' शास्त्रज्ञ जनोंको चाहिए कि ऐसे अनधिकारी जीवोंके प्रति शास्त्रकी सच्ची बातका प्रतिपादन न करें, क्यों कि ऐसा करनेसे उन्हें हितके बजाय अहित ही होता है - " पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् ।" कहा भी है
"
अप्रशान्तमतौ शास्त्रसद्भावप्रतिपादनम् । दोषायाभिनवोर्दीर्णे शमनीयमिव ज्वरे ।
---
- जैसे नए बुखारमें उसे दवा देनेवाली औषधि दोषावह होती है, वैसे ही जिसकी मति मिथ्यात्वकर्म रूपी मलके कारण शान्त नहीं हुई है उसके प्रति शास्त्रीय सत्योंका प्रतिपादन दोषका कारण होता है।
२६
Jain Education International
---
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org