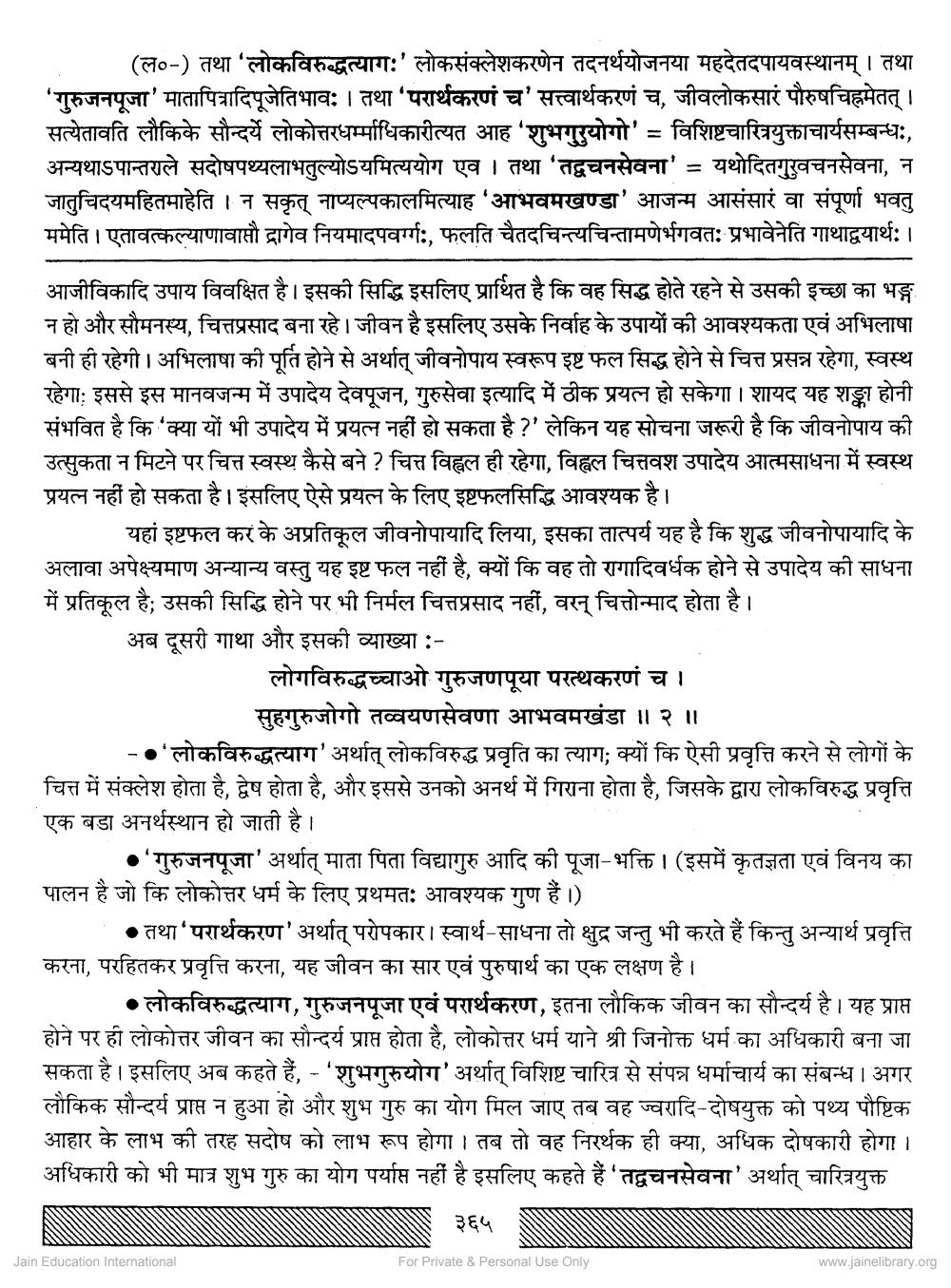________________
(ल०-) तथा 'लोकविरुद्धत्यागः' लोकसंक्लेशकरणेन तदनर्थयोजनया महदेतदपायवस्थानम् । तथा 'गुरुजनपूजा' मातापित्रादिपूजेतिभावः । तथा 'परार्थकरणं च' सत्त्वार्थकरणं च, जीवलोकसारं पौरुषचिह्नमेतत् । सत्येतावति लौकिके सौन्दर्ये लोकोत्तरधर्माधिकारीत्यत आह 'शुभगुरुयोगो' = विशिष्टचारित्रयुक्ताचार्यसम्बन्धः, अन्यथाऽपान्तराले सदोषपथ्यलाभतुल्योऽयमित्ययोग एव । तथा 'तद्वचनसेवना' = यथोदितगुरुवचनसेवना, न जातुचिदयमहितमाहेति । न सकृत् नाप्यल्पकालमित्याह 'आभवमखण्डा' आजन्म आसंसारं वा संपूर्णा भवतु ममेति । एतावत्कल्याणावाप्तौ द्रागेव नियमादपवर्गः, फलति चैतदचिन्त्यचिन्तामणेभगवतः प्रभावेनेति गाथाद्वयार्थः ।
आजीविकादि उपाय विवक्षित है। इसकी सिद्धि इसलिए प्रार्थित है कि वह सिद्ध होते रहने से उसकी इच्छा का भङ्ग न हो और सौमनस्य, चित्तप्रसाद बना रहे। जीवन है इसलिए उसके निर्वाह के उपायों की आवश्यकता एवं अभिलाषा बनी ही रहेगी। अभिलाषा की पूर्ति होने से अर्थात् जीवनोपाय स्वरूप इष्ट फल सिद्ध होने से चित्त प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा; इससे इस मानवजन्म में उपादेय देवपूजन, गुरुसेवा इत्यादि में ठीक प्रयत्न हो सकेगा। शायद यह शङ्का होनी संभवित है कि क्या यों भी उपादेय में प्रयत्न नहीं हो सकता है?' लेकिन यह सोचना जरूरी है कि जीवनोपाय की उत्सुकता न मिटने पर चित्त स्वस्थ कैसे बने ? चित्त विह्वल ही रहेगा, विह्वल चित्तवश उपादेय आत्मसाधना में स्वस्थ प्रयत्न नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रयत्न के लिए इष्टफलसिद्धि आवश्यक है।
यहां इष्टफल कर के अप्रतिकूल जीवनोपायादि लिया, इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध जीवनोपायादि के अलावा अपेक्ष्यमाण अन्यान्य वस्तु यह इष्ट फल नहीं है, क्यों कि वह तो रागादिवर्धक होने से उपादेय की साधना में प्रतिकूल है; उसकी सिद्धि होने पर भी निर्मल चित्तप्रसाद नहीं, वरन् चित्तोन्माद होता है। अब दूसरी गाथा और इसकी व्याख्या :
लोगविरुद्धच्चाओ गुरुजणपूया परत्थकरणं च ।
सुहगुरुजोगो तव्वयणसेवणा आभवमखंडा ।। २ ।। -.'लोकविरुद्धत्याग' अर्थात् लोकविरुद्ध प्रवृति का त्याग; क्यों कि ऐसी प्रवृत्ति करने से लोगों के चित्त में संक्लेश होता है, द्वेष होता है, और इससे उनको अनर्थ में गिराना होता है, जिसके द्वारा लोकविरुद्ध प्रवृत्ति एक बडा अनर्थस्थान हो जाती है।
• 'गुरुजनपूजा' अर्थात् माता पिता विद्यागुरु आदि की पूजा-भक्ति। (इसमें कृतज्ञता एवं विनय का पालन है जो कि लोकोत्तर धर्म के लिए प्रथमतः आवश्यक गुण हैं।)
• तथा परार्थकरण' अर्थात् परोपकार। स्वार्थ-साधना तो क्षुद्र जन्तु भी करते हैं किन्तु अन्यार्थ प्रवृत्ति करना, परहितकर प्रवृत्ति करना, यह जीवन का सार एवं पुरुषार्थ का एक लक्षण है।
• लोकविरुद्धत्याग, गुरुजनपूजा एवं परार्थकरण, इतना लौकिक जीवन का सौन्दर्य है। यह प्राप्त होने पर ही लोकोत्तर जीवन का सौन्दर्य प्राप्त होता है, लोकोत्तर धर्म याने श्री जिनोक्त धर्म का अधिकारी बना जा सकता है। इसलिए अब कहते हैं, - 'शुभगुरुयोग' अर्थात् विशिष्ट चारित्र से संपन्न धर्माचार्य का संबन्ध । अगर लौकिक सौन्दर्य प्राप्त न हुआ हो और शुभ गुरु का योग मिल जाए तब वह ज्वरादि-दोषयुक्त को पथ्य पौष्टिक आहार के लाभ की तरह सदोष को लाभ रूप होगा। तब तो वह निरर्थक ही क्या, अधिक दोषकारी होगा। अधिकारी को भी मात्र शुभ गुरु का योग पर्याप्त नहीं है इसलिए कहते हैं तद्वचनसेवना' अर्थात् चारित्रयुक्त
। ३६५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org