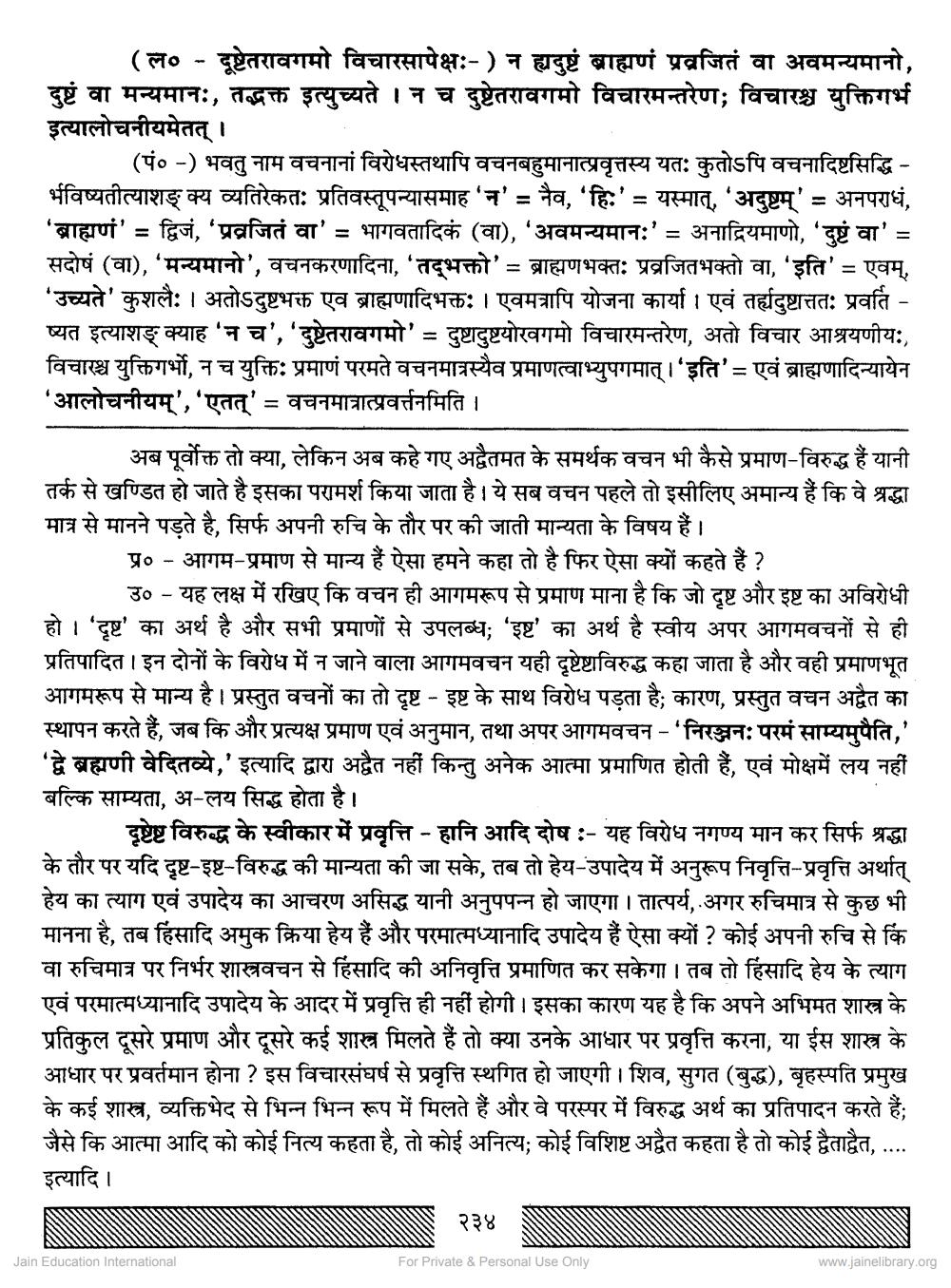________________
( ल० दूष्टेतरावगमो विचारसापेक्ष:-) न ह्यदुष्टं ब्राह्मणं प्रव्रजितं वा अवमन्यमानो, दुष्टं वा मन्यमानः, तद्भक्त इत्युच्यते । न च दुष्टेतरावगमो विचारमन्तरेण; विचारश्च युक्तिगर्भ इत्यालोचनीयमेतत् ।
(पं० -) भवतु नाम वचनानां विरोधस्तथापि वचनबहुमानात्प्रवृत्तस्य यतः कुतोऽपि वचनादिष्टसिद्धि - र्भविष्यतीत्याशङ्क्य व्यतिरेकतः प्रतिवस्तूपन्यासमाह 'न' = नैव, 'हि: ' = यस्मात्, 'अदुष्टम्' = अनपराधं, 'ब्राह्मणं' = द्विजं, 'प्रव्रजितं वा' = भागवतादिकं (वा), 'अवमन्यमानः ' = अनाद्रियमाणो, 'दुष्टं वा' = सदोषं (वा), 'मन्यमानो', वचनकरणादिना, 'तद्भक्तो' = ब्राह्मणभक्तः प्रव्रजितभक्तो वा 'इति' = एवम्, 'उच्यते' कुशलैः । अतोऽदुष्टभक्त एव ब्राह्मणादिभक्तः । एवमत्रापि योजना कार्या । एवं तर्ह्यदुष्टात्ततः प्रवर्ति - ष्यत इत्याशङ् क्याह 'न च', 'दुष्टेतरावगमो' = दुष्टादुष्टयोरवगमो विचारमन्तरेण, अतो विचार आश्रयणीयः, विचारश्च युक्तिगर्भो, न च युक्ति: प्रमाणं परमते वचनमात्रस्यैव प्रमाणत्वाभ्युपगमात् । 'इति' = एवं ब्राह्मणादिन्यायेन 'आलोचनीयम्', 'एतत् ' = वचनमात्रात्प्रवर्त्तनमिति ।
अब पूर्वोक्त तो क्या, लेकिन अब कहे गए अद्वैतमत के समर्थक वचन भी कैसे प्रमाण-विरुद्ध हैं यानी तर्क से खण्डित हो जाते है इसका परामर्श किया जाता है। ये सब वचन पहले तो इसीलिए अमान्य हैं कि वे श्रद्धा मात्र से मानने पड़ते है, सिर्फ अपनी रुचि के तौर पर की जाती मान्यता के विषय हैं।
आगम-प्रमाण से मान्य हैं ऐसा हमने कहा तो है फिर ऐसा क्यों कहते हैं ?
प्र०
उ०- यह लक्ष में रखिए कि वचन ही आगमरूप से प्रमाण माना है कि जो दृष्ट और इष्ट का अविरोधी हो । 'दृष्ट' का अर्थ है और सभी प्रमाणों से उपलब्ध; 'इष्ट' का अर्थ है स्वीय अपर आगमवचनों से ही प्रतिपादित । इन दोनों के विरोध में न जाने वाला आगमवचन यही दृष्टेष्टाविरुद्ध कहा जाता है और वही प्रमाणभूत आगमरूप से मान्य है। प्रस्तुत वचनों का तो दृष्ट - इष्ट के साथ विरोध पड़ता है; कारण, प्रस्तुत वचन अद्वैत का स्थापन करते हैं, जब कि और प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान, तथा अपर आगमवचन - 'निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति, ' 'द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये,' इत्यादि द्वारा अद्वैत नहीं किन्तु अनेक आत्मा प्रमाणित होती हैं, एवं मोक्षमें लय नहीं बल्कि साम्यता, अ-लय सिद्ध होता है ।
-
दृष्टेष्ट विरुद्ध के स्वीकार में प्रवृत्ति हानि आदि दोष :- यह विरोध नगण्य मान कर सिर्फ श्रद्धा के तौर पर यदि दृष्ट-इष्ट-विरुद्ध की मान्यता की जा सके, तब तो हेय-उपादेय में अनुरूप निवृत्ति - प्रवृत्ति अर्थात् हेय का त्याग एवं उपादेय का आचरण असिद्ध यानी अनुपपन्न हो जाएगा। तात्पर्य, अगर रुचिमात्र से कुछ भी मानना है, तब हिंसादि अमुक क्रिया हेय हैं और परमात्मध्यानादि उपादेय हैं ऐसा क्यों ? कोई अपनी रुचि से किं वा रुचिमात्र पर निर्भर शास्त्रवचन से हिंसादि की अनिवृत्ति प्रमाणित कर सकेगा । तब तो हिंसादि हेय के त्याग एवं परमात्मध्यानादि उपादेय के आदर में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसका कारण यह है कि अपने अभिमत शास्त्र के प्रतिकुल दूसरे प्रमाण और दूसरे कई शास्त्र मिलते हैं तो क्या उनके आधार पर प्रवृत्ति करना, या ईस शास्त्र के आधार पर प्रवर्तमान होना ? इस विचारसंघर्ष से प्रवृत्ति स्थगित हो जाएगी। शिव, सुगत (बुद्ध), बृहस्पति प्रमुख के कई शास्त्र, व्यक्तिभेद से भिन्न भिन्न रूप में मिलते हैं और वे परस्पर में विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हैं; जैसे कि आत्मा आदि को कोई नित्य कहता है, तो कोई अनित्य; कोई विशिष्ट अद्वैत कहता है तो कोई द्वैताद्वैत,
इत्यादि ।
Jain Education International
२३४
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org