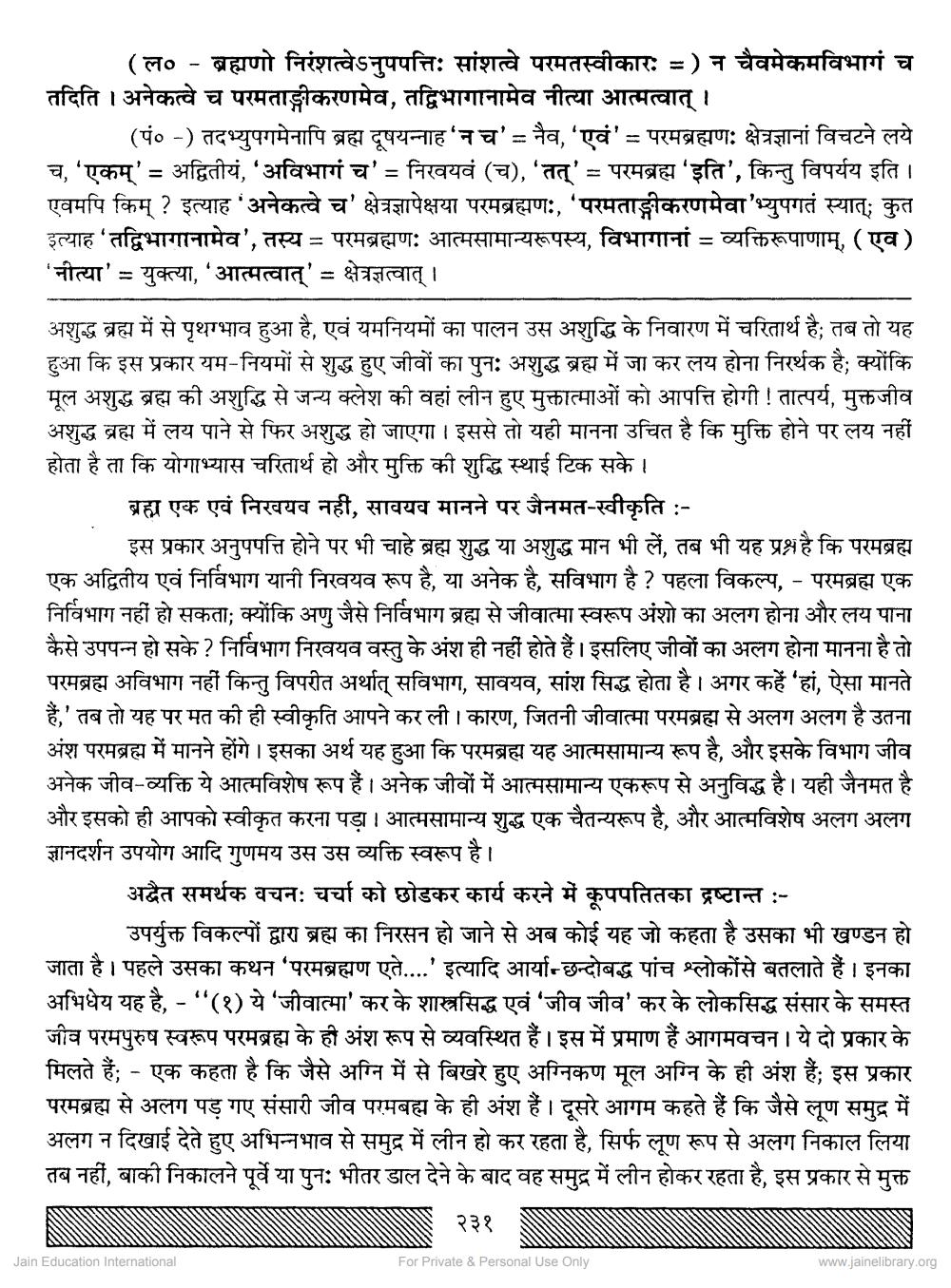________________
(ल० - ब्रह्मणो निरंशत्वेऽनुपपत्तिः सांशत्वे परमतस्वीकारः =) न चैवमेकमविभागं च तदिति । अनेकत्वे च परमताङ्गीकरणमेव, तद्विभागानामेव नीत्या आत्मत्वात् ।
(पं० -) तदभ्युपगमेनापि ब्रह्म दूषयन्नाह 'न च' = नैव, ‘एवं' = परमब्रह्मणः क्षेत्रज्ञानां विचटने लये च, 'एकम्' = अद्वितीयं, 'अविभागं च' = निरवयवं (च), 'तत्' = परमब्रह्म 'इति', किन्तु विपर्यय इति । एवमपि किम् ? इत्याह अनेकत्वे च' क्षेत्रज्ञापेक्षया परमब्रह्मणः, 'परमताङ्गीकरणमेवा'भ्युपगतं स्यात्; कुत इत्याह 'तद्विभागानामेव', तस्य = परमब्रह्मणः आत्मसामान्यरूपस्य, विभागानां = व्यक्तिरूपाणाम्, (एव) 'नीत्या' = युक्त्या, 'आत्मत्वात्' = क्षेत्रज्ञत्वात् ।
अशुद्ध ब्रह्म में से पृथग्भाव हुआ है, एवं यमनियमों का पालन उस अशुद्धि के निवारण में चरितार्थ है; तब तो यह हुआ कि इस प्रकार यम-नियमों से शुद्ध हुए जीवों का पुनः अशुद्ध ब्रह्म में जा कर लय होना निरर्थक है; क्योंकि मूल अशुद्ध ब्रह्म की अशुद्धि से जन्य क्लेश की वहां लीन हुए मुक्तात्माओं को आपत्ति होगी ! तात्पर्य, मुक्तजीव अशुद्ध ब्रह्म में लय पाने से फिर अशुद्ध हो जाएगा। इससे तो यही मानना उचित है कि मुक्ति होने पर लय नहीं होता है ता कि योगाभ्यास चरितार्थ हो और मुक्ति की शुद्धि स्थाई टिक सके।
ब्रह्म एक एवं निरवयव नहीं, सावयव मानने पर जैनमत-स्वीकृति :
इस प्रकार अनुपपत्ति होने पर भी चाहे ब्रह्म शुद्ध या अशुद्ध मान भी लें, तब भी यह प्रश्न है कि परमब्रह्म एक अद्वितीय एवं निविभाग यानी निरवयव रूप है, या अनेक है, सविभाग है? पहला विकल्प, - परमब्रह्म एक निर्विभाग नहीं हो सकता; क्योंकि अणु जैसे निर्विभाग ब्रह्म से जीवात्मा स्वरूप अंशो का अलग होना और लय पाना कैसे उपपन्न हो सके? निविभाग निरवयव वस्तु के अंश ही नहीं होते हैं। इसलिए जीवों का अलग होना मानना है तो परमब्रह्म अविभाग नहीं किन्तु विपरीत अर्थात् सविभाग, सावयव, सांश सिद्ध होता है। अगर कहें 'हां, ऐसा मानते हैं,' तब तो यह पर मत की ही स्वीकृति आपने कर ली। कारण, जितनी जीवात्मा परमब्रह्म से अलग अलग है उतना अंश परमब्रह्म में मानने होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि परमब्रह्म यह आत्मसामान्य रूप है, और इसके विभाग जीव अनेक जीव-व्यक्ति ये आत्मविशेष रूप हैं। अनेक जीवों में आत्मसामान्य एकरूप से अनुविद्ध है। यही जैनमत है और इसको ही आपको स्वीकृत करना पड़ा। आत्मसामान्य शुद्ध एक चैतन्यरूप है, और आत्मविशेष अलग अलग ज्ञानदर्शन उपयोग आदि गुणमय उस उस व्यक्ति स्वरूप है।
अद्वैत समर्थक वचन: चर्चा को छोडकर कार्य करने में कूपपतितका द्रष्टान्त :
उपर्युक्त विकल्पों द्वारा ब्रह्म का निरसन हो जाने से अब कोई यह जो कहता है उसका भी खण्डन हो जाता है। पहले उसका कथन 'परमब्रह्मण एते....' इत्यादि आर्या-छन्दोबद्ध पांच श्लोकोंसे बतलाते हैं। इनका अभिधेय यह है, - "(१) ये 'जीवात्मा' कर के शास्त्रसिद्ध एवं 'जीव जीव' कर के लोकसिद्ध संसार के समस्त जीव परमपुरुष स्वरूप परमब्रह्म के ही अंश रूप से व्यवस्थित हैं। इस में प्रमाण हैं आगमवचन । ये दो प्रकार के मिलते हैं; - एक कहता है कि जैसे अग्नि में से बिखरे हुए अग्निकण मूल अग्नि के ही अंश हैं; इस प्रकार परमब्रह्म से अलग पड़ गए संसारी जीव परमबह्म के ही अंश हैं। दूसरे आगम कहते हैं कि जैसे लूण समुद्र में अलग न दिखाई देते हुए अभिन्नभाव से समुद्र में लीन हो कर रहता है, सिर्फ लूण रूप से अलग निकाल लिया तब नहीं, बाकी निकालने पूर्वे या पुनः भीतर डाल देने के बाद वह समुद्र में लीन होकर रहता है, इस प्रकार से मुक्त
२३१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org