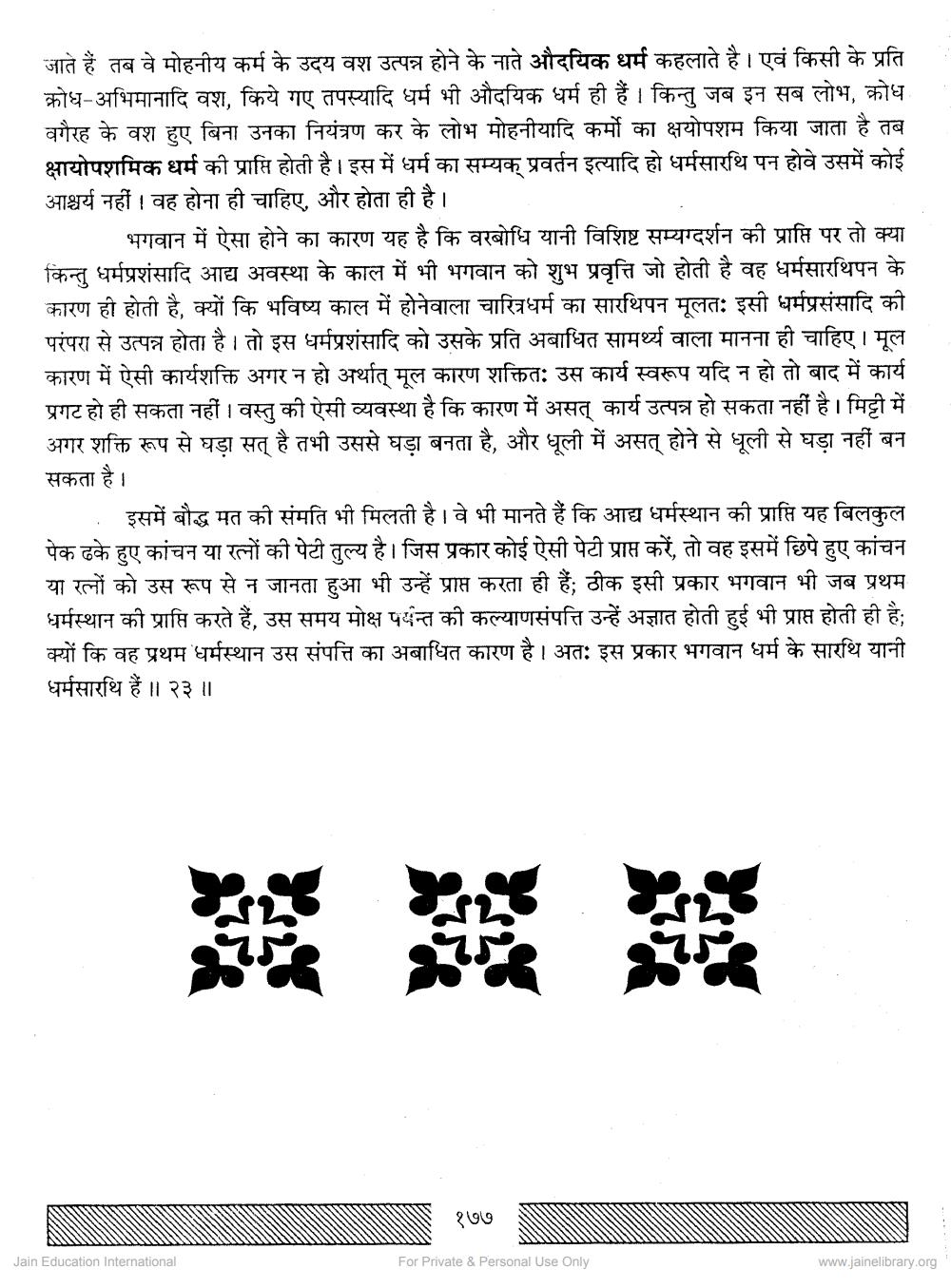________________
जाते हैं तब वे मोहनीय कर्म के उदय वश उत्पन्न होने के नाते औदयिक धर्म कहलाते है। एवं किसी के प्रति क्रोध-अभिमानादि वश, किये गए तपस्यादि धर्म भी औदयिक धर्म ही हैं । किन्तु जब इन सब लोभ, क्रोध वगैरह के वश हुए बिना उनका नियंत्रण कर के लोभ मोहनीयादि कर्मो का क्षयोपशम किया जाता है तब क्षायोपशमिक धर्म की प्राप्ति होती है। इस में धर्म का सम्यक् प्रवर्तन इत्यादि हो धर्मसारथि पन होवे उसमें कोई आश्चर्य नहीं । वह होना ही चाहिए, और होता ही है।
भगवान में ऐसा होने का कारण यह है कि वरबोधि यानी विशिष्ट सम्यग्दर्शन की प्राप्ति पर तो क्या किन्तु धर्मप्रशंसादि आद्य अवस्था के काल में भी भगवान को शुभ प्रवृत्ति जो होती है वह धर्मसारथिपन के कारण ही होती है, क्यों कि भविष्य काल में होनेवाला चारित्रधर्म का सारथिपन मूलतः इसी धर्मप्रसंसादि की परंपरा से उत्पन्न होता है। तो इस धर्मप्रशंसादि को उसके प्रति अबाधित सामर्थ्य वाला मानना ही चाहिए। मूल कारण में ऐसी कार्यशक्ति अगर न हो अर्थात् मूल कारण शक्तित: उस कार्य स्वरूप यदि न हो तो बाद में कार्य प्रगट हो ही सकता नहीं । वस्तु की ऐसी व्यवस्था है कि कारण में असत् कार्य उत्पन्न हो सकता नहीं है। मिट्टी में अगर शक्ति रूप से घड़ा सत् है तभी उससे घड़ा बनता है, और धूली में असत् होने से धूली से घड़ा नहीं बन सकता है।
. इसमें बौद्ध मत की संमति भी मिलती है। वे भी मानते हैं कि आद्य धर्मस्थान की प्राप्ति यह बिलकुल पेक ढके हुए कांचन या रत्नों की पेटी तुल्य है। जिस प्रकार कोई ऐसी पेटी प्राप्त करें, तो वह इसमें छिपे हुए कांचन या रत्नों को उस रूप से न जानता हुआ भी उन्हें प्राप्त करता ही हैं; ठीक इसी प्रकार भगवान भी जब प्रथम धर्मस्थान की प्राप्ति करते हैं, उस समय मोक्ष पर्यन्त की कल्याणसंपत्ति उन्हें अज्ञात होती हुई भी प्राप्त होती ही है; क्यों कि वह प्रथम धर्मस्थान उस संपत्ति का अबाधित कारण है। अतः इस प्रकार भगवान धर्म के सारथि यानी धर्मसारथि हैं ॥ २३ ॥
१७७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org,