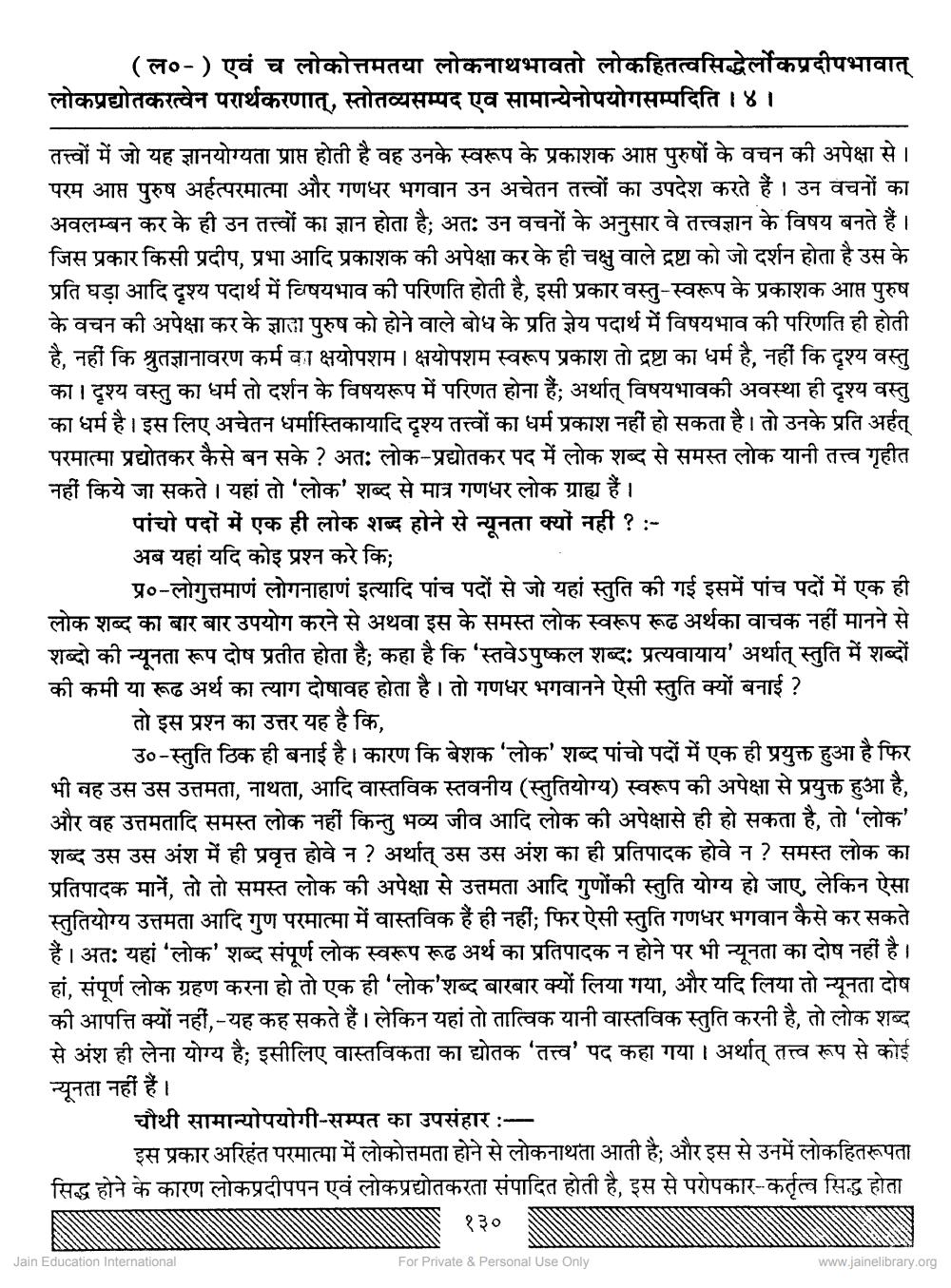________________
(ल०-) एवं च लोकोत्तमतया लोकनाथभावतो लोकहितत्वसिद्धेर्लोकप्रदीपभावात् लोकप्रद्योतकरत्वेन परार्थकरणात्, स्तोतव्यसम्पद एव सामान्येनोपयोगसम्पदिति । ४।।
तत्त्वों में जो यह ज्ञानयोग्यता प्राप्त होती है वह उनके स्वरूप के प्रकाशक आप्त पुरुषों के वचन की अपेक्षा से । परम आप्त पुरुष अर्हत्परमात्मा और गणधर भगवान उन अचेतन तत्त्वों का उपदेश करते हैं। उन वचनों का अवलम्बन कर के ही उन तत्त्वों का ज्ञान होता है; अतः उन वचनों के अनुसार वे तत्त्वज्ञान के विषय बनते हैं। जिस प्रकार किसी प्रदीप, प्रभा आदि प्रकाशक की अपेक्षा कर के ही चक्षु वाले द्रष्टा को जो दर्शन होता है उस के प्रति घड़ा आदि दृश्य पदार्थ में विषयभाव की परिणति होती है, इसी प्रकार वस्तु-स्वरूप के प्रकाशक आप्त पुरुष के वचन की अपेक्षा कर के ज्ञाता पुरुष को होने वाले बोध के प्रति ज्ञेय पदार्थ में विषयभाव की परिणति ही होती है, नहीं कि श्रुतज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम । क्षयोपशम स्वरूप प्रकाश तो द्रष्टा का धर्म है, नहीं कि दृश्य वस्तु का । दृश्य वस्तु का धर्म तो दर्शन के विषयरूप में परिणत होना हैं; अर्थात् विषयभावकी अवस्था ही दृश्य वस्तु का धर्म है। इस लिए अचेतन धर्मास्तिकायादि दृश्य तत्त्वों का धर्म प्रकाश नहीं हो सकता है। तो उनके प्रति अर्हत् परमात्मा प्रद्योतकर कैसे बन सके? अतः लोक-प्रद्योतकर पद में लोक शब्द से समस्त लोक यानी तत्त्व गृहीत नहीं किये जा सकते । यहां तो 'लोक' शब्द से मात्र गणधर लोक ग्राह्य हैं।
पांचो पदों में एक ही लोक शब्द होने से न्यूनता क्यों नहीं ? :अब यहां यदि कोइ प्रश्न करे कि;
प्र०-लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं इत्यादि पांच पदों से जो यहां स्तुति की गई इसमें पांच पदों में एक ही लोक शब्द का बार बार उपयोग करने से अथवा इस के समस्त लोक स्वरूप रूढ अर्थका वाचक नहीं मानने से शब्दो की न्यूनता रूप दोष प्रतीत होता है; कहा है कि 'स्तवेऽपुष्कल शब्दः प्रत्यवायाय' अर्थात् स्तुति में शब्दों की कमी या रूढ अर्थ का त्याग दोषावह होता है। तो गणधर भगवानने ऐसी स्तुति क्यों बनाई ?
तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि,
उ०-स्तुति ठिक ही बनाई है। कारण कि बेशक 'लोक' शब्द पांचो पदों में एक ही प्रयुक्त हुआ है फिर भी वह उस उस उत्तमता, नाथता, आदि वास्तविक स्तवनीय (स्तुतियोग्य) स्वरूप की अपेक्षा से प्रयुक्त हुआ है, और वह उत्तमतादि समस्त लोक नहीं किन्तु भव्य जीव आदि लोक की अपेक्षासे ही हो सकता है, तो 'लोक' शब्द उस उस अंश में ही प्रवृत्त होवे न ? अर्थात् उस उस अंश का ही प्रतिपादक होवे न? समस्त लोक का प्रतिपादक मानें, तो तो समस्त लोक की अपेक्षा से उत्तमता आदि गुणोंकी स्तुति योग्य हो जाए, लेकिन ऐसा स्तुतियोग्य उत्तमता आदि गुण परमात्मा में वास्तविक हैं ही नहीं; फिर ऐसी स्तुति गणधर भगवान कैसे कर सकते हैं। अत: यहां 'लोक' शब्द संपूर्ण लोक स्वरूप रूढ अर्थ का प्रतिपादक न होने पर भी न्यूनता का दोष नहीं है। हां, संपूर्ण लोक ग्रहण करना हो तो एक ही 'लोक'शब्द बारबार क्यों लिया गया, और यदि लिया तो न्यूनता दोष की आपत्ति क्यों नहीं,-यह कह सकते हैं। लेकिन यहां तो तात्विक यानी वास्तविक स्तुति करनी है, तो लोक शब्द से अंश ही लेना योग्य है; इसीलिए वास्तविकता का द्योतक 'तत्त्व' पद कहा गया। अर्थात् तत्त्व रूप से कोई न्यूनता नहीं हैं।
चौथी सामान्योपयोगी-सम्पत का उपसंहार :
इस प्रकार अरिहंत परमात्मा में लोकोत्तमता होने से लोकनाथता आती है; और इस से उनमें लोकहितरूपता सिद्ध होने के कारण लोकप्रदीपपन एवं लोकप्रद्योतकरता संपादित होती है, इस से परोपकार-कर्तृत्व सिद्ध होता
AS १३०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org