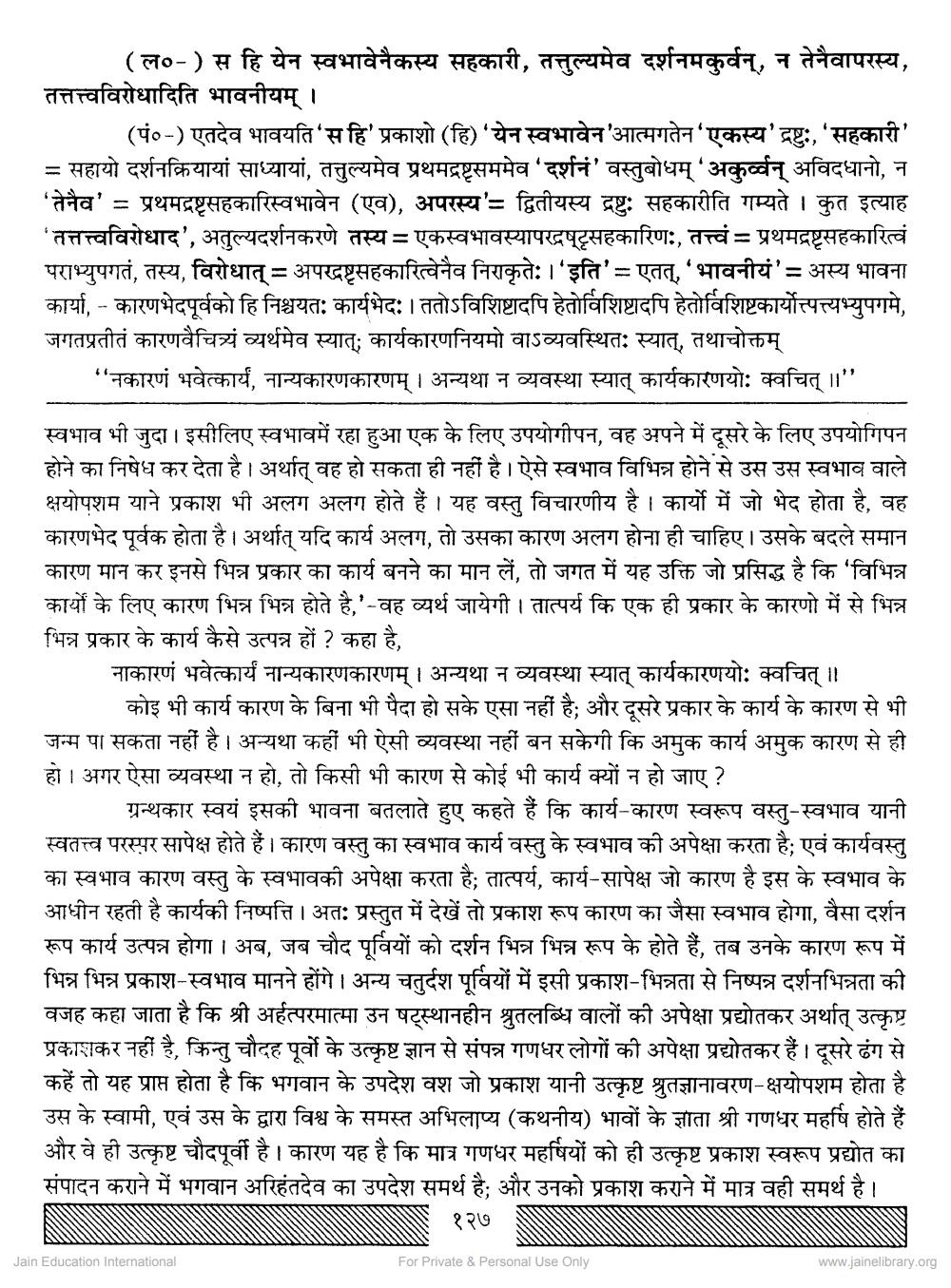________________
(ल०-) स हि येन स्वभावेनैकस्य सहकारी, तत्तुल्यमेव दर्शनमकुर्वन्, न तेनैवापरस्य, तत्तत्त्वविरोधादिति भावनीयम् ।
(पं०-) एतदेव भावयति स हि' प्रकाशो (हि) 'येन स्वभावेन'आत्मगतेन 'एकस्य' द्रष्टुः, 'सहकारी' = सहायो दर्शनक्रियायां साध्यायां, तत्तुल्यमेव प्रथमद्रष्टसममेव 'दर्शनं' वस्तुबोधम् ‘अकुर्वन् अविदधानो, न 'तेनैव' = प्रथमद्रष्टसहकारिस्वभावेन (एव), अपरस्य'= द्वितीयस्य द्रष्टः सहकारीति गम्यते । कुत इत्याह 'तत्तत्त्वविरोधाद', अतुल्यदर्शनकरणे तस्य = एकस्वभावस्यापरद्रष्टृसहकारिणः, तत्त्वं = प्रथमद्रष्टुसहकारित्वं पराभ्युपगतं, तस्य, विरोधात् = अपरद्रष्टसहकारित्वेनैव निराकृतेः । इति' = एतत्, 'भावनीयं' = अस्य भावना कार्या, - कारणभेदपूर्वको हि निश्चयतः कार्यभेदः । ततोऽविशिष्टादपि हेतोविशिष्टादपि हेतोविशिष्टकार्योत्पत्त्यभ्युपगमे, जगतप्रतीतं कारणवैचित्र्यं व्यर्थमेव स्यात्; कार्यकारणनियमो वाऽव्यवस्थितः स्यात्, तथाचोक्तम्
"नकारणं भवेत्कार्य, नान्यकारणकारणम् । अन्यथा न व्यवस्था स्यात् कार्यकारणयोः क्वचित् ।।" स्वभाव भी जुदा । इसीलिए स्वभावमें रहा हुआ एक के लिए उपयोगीपन, वह अपने में दूसरे के लिए उपयोगिपन होने का निषेध कर देता है। अर्थात् वह हो सकता ही नहीं है। ऐसे स्वभाव विभिन्न होने से उस उस स्वभाव वाले क्षयोपशम याने प्रकाश भी अलग अलग होते हैं। यह वस्तु विचारणीय है। कार्यो में जो भेद होता है, वह कारणभेद पूर्वक होता है। अर्थात् यदि कार्य अलग, तो उसका कारण अलग होना ही चाहिए। उसके बदले समान कारण मान कर इनसे भिन्न प्रकार का कार्य बनने का मान लें, तो जगत में यह उक्ति जो प्रसिद्ध है कि 'विभिन्न कार्यों के लिए कारण भिन्न भिन्न होते है,'-वह व्यर्थ जायेगी। तात्पर्य कि एक ही प्रकार के कारणो में से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कैसे उत्पन्न हों ? कहा है,
नाकारणं भवेत्कार्यं नान्यकारणकारणम् । अन्यथा न व्यवस्था स्यात् कार्यकारणयोः क्वचित् ।।
कोइ भी कार्य कारण के बिना भी पैदा हो सके एसा नहीं है; और दूसरे प्रकार के कार्य के कारण से भी जन्म पा सकता नहीं है। अन्यथा कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकेगी कि अमुक कार्य अमुक कारण से ही हो। अगर ऐसा व्यवस्था न हो, तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य क्यों न हो जाए?
ग्रन्थकार स्वयं इसकी भावना बतलाते हुए कहते हैं कि कार्य-कारण स्वरूप वस्तु-स्वभाव यानी स्वतत्त्व परस्पर सापेक्ष होते हैं। कारण वस्तु का स्वभाव कार्य वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा करता है; एवं कार्यवस्तु का स्वभाव कारण वस्तु के स्वभावकी अपेक्षा करता है; तात्पर्य, कार्य-सापेक्ष जो कारण है इस के स्वभाव के आधीन रहती है कार्यकी निष्पत्ति । अतः प्रस्तुत में देखें तो प्रकाश रूप कारण का जैसा स्वभाव होगा, वैसा दर्शन रूप कार्य उत्पन्न होगा। अब, जब चौद पूर्वियों को दर्शन भिन्न भिन्न रूप के होते हैं, तब उनके कारण रूप में भिन्न भिन्न प्रकाश-स्वभाव मानने होंगे। अन्य चतुर्दश पूर्वियों में इसी प्रकाश-भिन्नता से निष्पन्न दर्शनभिन्नता की वजह कहा जाता है कि श्री अर्हत्परमात्मा उन षट्स्थानहीन श्रुतलब्धि वालों की अपेक्षा प्रद्योतकर अर्थात् उत्कृष्ट प्रकाशकर नहीं है, किन्तु चौदह पूर्वो के उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न गणधर लोगों की अपेक्षा प्रद्योतकर हैं। दूसरे ढंग से कहें तो यह प्राप्त होता है कि भगवान के उपदेश वश जो प्रकाश यानी उत्कृष्ट श्रुतज्ञानावरण-क्षयोपशम होता है उस के स्वामी, एवं उस के द्वारा विश्व के समस्त अभिलाप्य (कथनीय) भावों के ज्ञाता श्री गणधर महर्षि होते हैं और वे ही उत्कृष्ट चौदपूर्वी है। कारण यह है कि मात्र गणधर महर्षियों को ही उत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप प्रद्योत का संपादन कराने में भगवान अरिहंतदेव का उपदेश समर्थ है; और उनको प्रकाश कराने में मात्र वही समर्थ है।
१२७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org