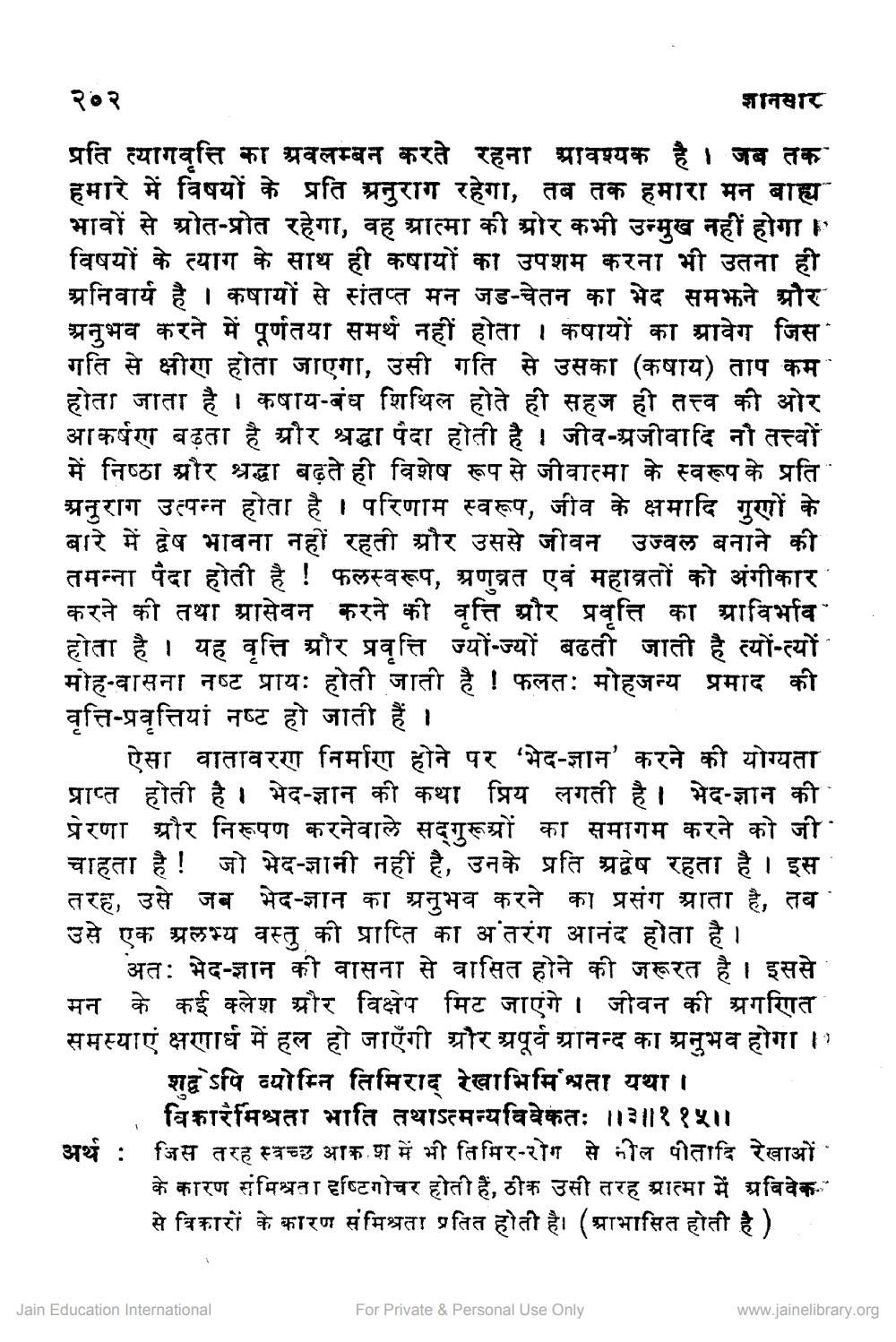________________
२०२
ज्ञानसार प्रति त्यागवत्ति का अवलम्बन करते रहना आवश्यक है। जब तक हमारे में विषयों के प्रति अनुराग रहेगा, तब तक हमारा मन बाह्य भावों से प्रोत-प्रोत रहेगा, वह आत्मा की ओर कभी उन्मूख नहीं होगा।' विषयों के त्याग के साथ ही कषायों का उपशम करना भी उतना ही अनिवार्य है । कषायों से संतप्त मन जड-चेतन का भेद समझने और अनुभव करने में पूर्णतया समर्थ नहीं होता । कषायों का आवेग जिस गति से क्षीण होता जाएगा, उसी गति से उसका (कषाय) ताप कम होता जाता है । कषाय-बंध शिथिल होते ही सहज ही तत्त्व की ओर आकर्षण बढ़ता है और श्रद्धा पैदा होती है । जीव-अजीवादि नौ तत्त्वों में निष्ठा और श्रद्धा बढ़ते ही विशेष रूप से जीवात्मा के स्वरूप के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है । परिणाम स्वरूप, जीव के क्षमादि गुणों के बारे में द्वेष भावना नहीं रहती और उससे जीवन उज्वल बनाने की तमन्ना पैदा होती है ! फलस्वरूप, प्रणवत एवं महाव्रतों को अंगीकार करने की तथा प्रासेवन करने की वृत्ति और प्रवृत्ति का प्राविर्भाव होता है । यह वृत्ति और प्रवृत्ति ज्यों-ज्यों बढती जाती है त्यों-त्यों मोह-वासना नष्ट प्रायः होती जाती है ! फलतः मोहजन्य प्रमाद की वृत्ति-प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं ।
ऐसा वातावरण निर्माण होने पर 'भेद-ज्ञान' करने की योग्यता प्राप्त होती है। भेद-ज्ञान की कथा प्रिय लगती है। भेद-ज्ञान की प्रेरणा और निरूपण करनेवाले सद्गुरूओं का समागम करने को जी चाहता है ! जो भेद-ज्ञानी नहीं है, उनके प्रति अद्वेष रहता है । इस तरह, उसे जब भेद-ज्ञान का अनुभव करने का प्रसंग पाता है, तब उसे एक अलभ्य वस्तु की प्राप्ति का अंतरंग आनंद होता है।
अत: भेद-ज्ञान की वासना से वासित होने की जरूरत है। इससे मन के कई क्लेश और विक्षेप मिट जाएंगे। जीवन की अगणित समस्याएं क्षणार्ध में हल हो जाएँगी और अपूर्व प्रानन्द का अनुभव होगा।'
शद्रऽपि व्योम्नि तिमिराद रेखाभिमिश्रता यथा ।
विकारैमिश्रता भाति तथाऽत्मन्यविवेकतः ॥३॥११॥ अर्थ : जिस तरह स्वच्छ आक श में भी तिमिर-रोग से नील पीतादि रेखाओं
के कारण संमिश्रता दृष्टिगोचर होती हैं, ठीक उसी तरह प्रात्मा में अविवेकसे विकारों के कारण संमिश्रता प्रतित होती है। (प्राभासित होती है)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org