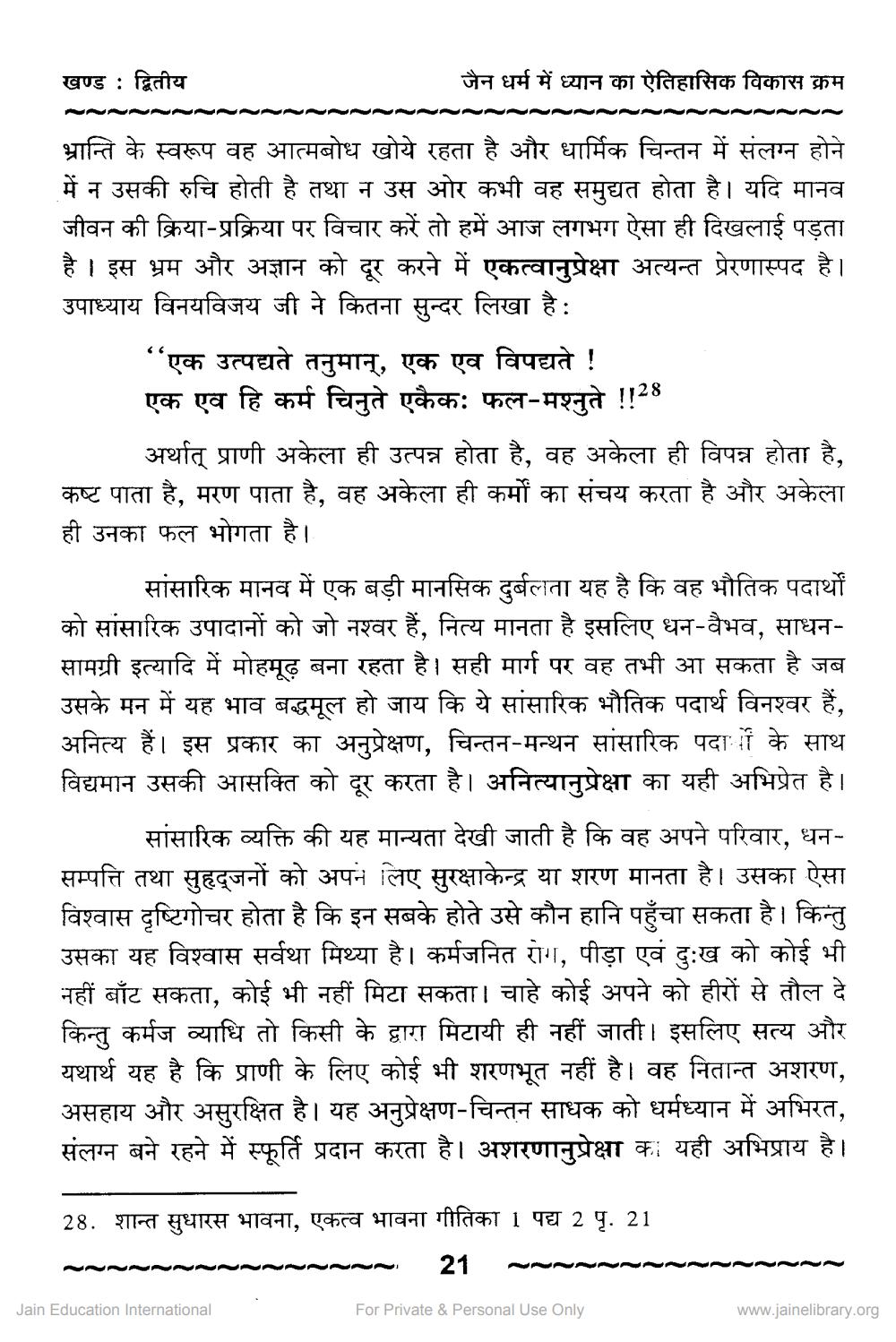________________
खण्ड : द्वितीय
जैन धर्म में ध्यान का ऐतिहासिक विकास क्रम
भ्रान्ति के स्वरूप वह आत्मबोध खोये रहता है और धार्मिक चिन्तन में संलग्न होने में न उसकी रुचि होती है तथा न उस ओर कभी वह समुद्यत होता है। यदि मानव जीवन की क्रिया-प्रक्रिया पर विचार करें तो हमें आज लगभग ऐसा ही दिखलाई पड़ता है। इस भ्रम और अज्ञान को दूर करने में एकत्वानुप्रेक्षा अत्यन्त प्रेरणास्पद है। उपाध्याय विनयविजय जी ने कितना सुन्दर लिखा है :
“एक उत्पद्यते तनुमान्, एक एव विपद्यते ! एक एव हि कर्म चिनुते एकैकः फल-मश्नुते !!28
अर्थात् प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, वह अकेला ही विपन्न होता है, कष्ट पाता है, मरण पाता है, वह अकेला ही कर्मों का संचय करता है और अकेला ही उनका फल भोगता है।
सांसारिक मानव में एक बड़ी मानसिक दुर्बलता यह है कि वह भौतिक पदार्थों को सांसारिक उपादानों को जो नश्वर हैं, नित्य मानता है इसलिए धन-वैभव, साधनसामग्री इत्यादि में मोहमूढ़ बना रहता है। सही मार्ग पर वह तभी आ सकता है जब उसके मन में यह भाव बद्धमूल हो जाय कि ये सांसारिक भौतिक पदार्थ विनश्वर हैं,
अनित्य हैं। इस प्रकार का अनुप्रेक्षण, चिन्तन-मन्थन सांसारिक पदागों के साथ विद्यमान उसकी आसक्ति को दूर करता है। अनित्यानुप्रेक्षा का यही अभिप्रेत है।
सांसारिक व्यक्ति की यह मान्यता देखी जाती है कि वह अपने परिवार, धनसम्पत्ति तथा सुहृद्जनों को अपने लिए सुरक्षाकेन्द्र या शरण मानता है। उसका ऐसा विश्वास दृष्टिगोचर होता है कि इन सबके होते उसे कौन हानि पहुँचा सकता है। किन्तु उसका यह विश्वास सर्वथा मिथ्या है। कर्मजनित रोग, पीड़ा एवं दु:ख को कोई भी नहीं बाँट सकता, कोई भी नहीं मिटा सकता। चाहे कोई अपने को हीरों से तौल दे किन्तु कर्मज व्याधि तो किसी के द्वारा मिटायी ही नहीं जाती। इसलिए सत्य और यथार्थ यह है कि प्राणी के लिए कोई भी शरणभूत नहीं है। वह नितान्त अशरण, असहाय और असुरक्षित है। यह अनुप्रेक्षण-चिन्तन साधक को धर्मध्यान में अभिरत, संलग्न बने रहने में स्फूर्ति प्रदान करता है। अशरणानुप्रेक्षा क यही अभिप्राय है।
28. शान्त सुधारस भावना, एकत्व भावना गीतिका 1 पद्य 2 पृ. 21
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org