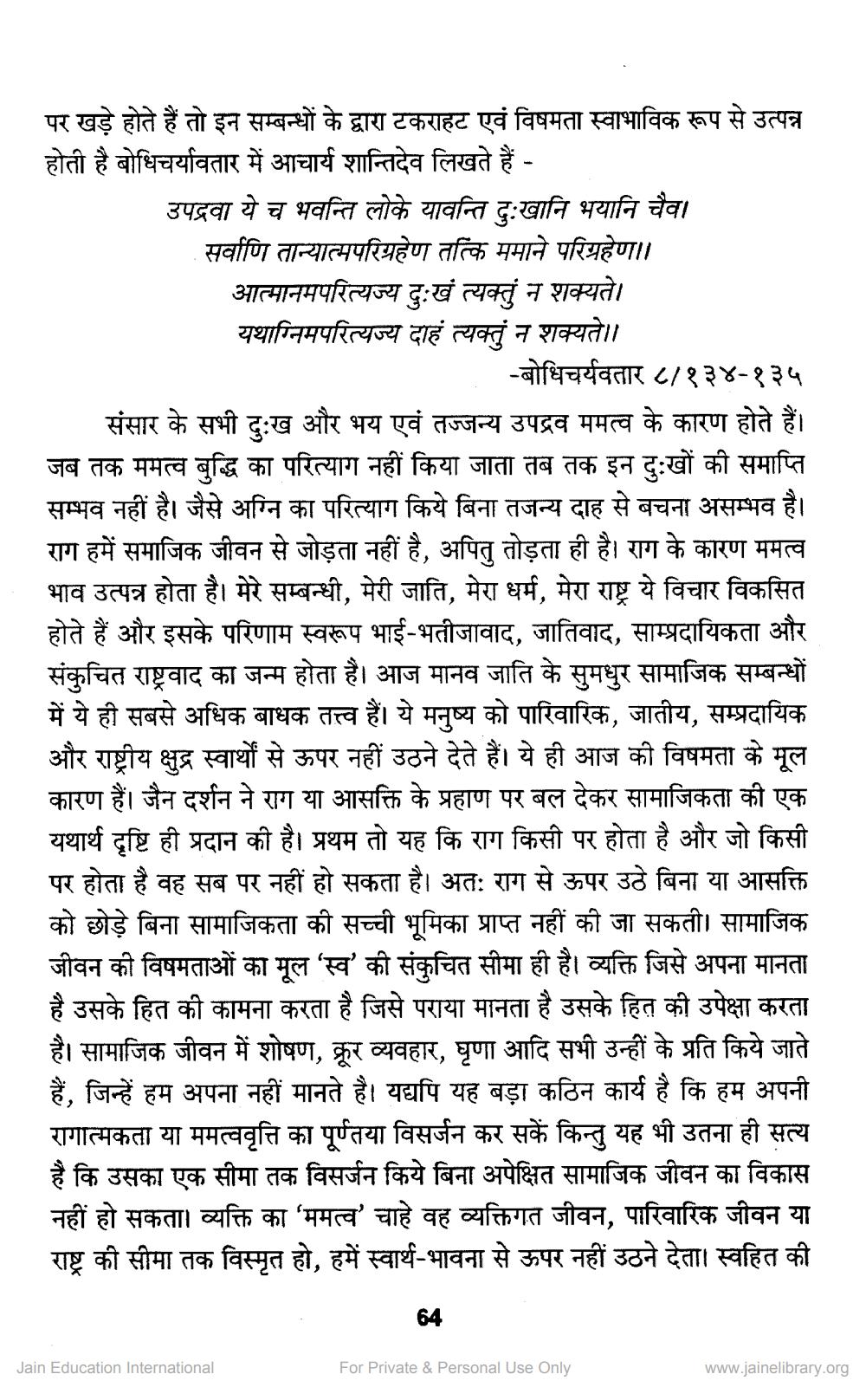________________
पर खड़े होते हैं तो इन सम्बन्धों के द्वारा टकराहट एवं विषमता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है बोधिचर्यावतार में आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं
उपद्रवा ये च भवन्ति लोके यावन्ति दुःखानि भयानि चैव । सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण तत्कि ममाने परिग्रहेण ।। आत्मानमपरित्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते । यथाग्निमपरित्यज्य दाहं त्यक्तुं न शक्यते ॥
संसार के सभी दुःख और भय एवं तज्जन्य उपद्रव ममत्व के कारण होते हैं। जब तक ममत्व बुद्धि का परित्याग नहीं किया जाता तब तक इन दुःखों की समाप्ति सम्भव नहीं है। जैसे अग्नि का परित्याग किये बिना तजन्य दाह से बचना असम्भव है। राग हमें समाजिक जीवन से जोड़ता नहीं है, अपितु तोड़ता ही है। राग के कारण ममत्व भाव उत्पन्न होता है। मेरे सम्बन्धी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र ये विचार विकसित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप भाई-भतीजावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और संकुचित राष्ट्रवाद का जन्म होता है। आज मानव जाति के सुमधुर सामाजिक सम्बन्धों में ये ही सबसे अधिक बाधक तत्त्व हैं। ये मनुष्य को पारिवारिक, जातीय, सम्प्रदायिक और राष्ट्रीय क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर नहीं उठने देते हैं। ये ही आज की विषमता के मूल कारण हैं। जैन दर्शन ने राग या आसक्ति के प्रहाण पर बल देकर सामाजिकता की एक यथार्थ दृष्टि ही प्रदान की है। प्रथम तो यह कि राग किसी पर होता है और जो किसी पर होता है वह सब पर नहीं हो सकता है। अतः राग से ऊपर उठे बिना या आसक्ति को छोड़े बिना सामाजिकता की सच्ची भूमिका प्राप्त नहीं की जा सकती । सामाजिक जीवन की विषमताओं का मूल 'स्व' की संकुचित सीमा ही है। व्यक्ति जिसे अपना मानता है उसके हित की कामना करता है जिसे पराया मानता है उसके हित की उपेक्षा करता है। सामाजिक जीवन में शोषण, क्रूर व्यवहार, घृणा आदि सभी उन्हीं के प्रति किये जाते हैं, जिन्हें हम अपना नहीं मानते है । यद्यपि यह बड़ा कठिन कार्य है कि हम अपनी रागात्मकता या ममत्ववृत्ति का पूर्णतया विसर्जन कर सकें किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उसका एक सीमा तक विसर्जन किये बिना अपेक्षित सामाजिक जीवन का विकास नहीं हो सकता । व्यक्ति का 'ममत्व' चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या राष्ट्र की सीमा तक विस्मृत हो, हमें स्वार्थ भावना से ऊपर नहीं उठने देता । स्वहित की
Jain Education International
- बोधिचर्यवतार ८ / १३४-१३५
64
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org