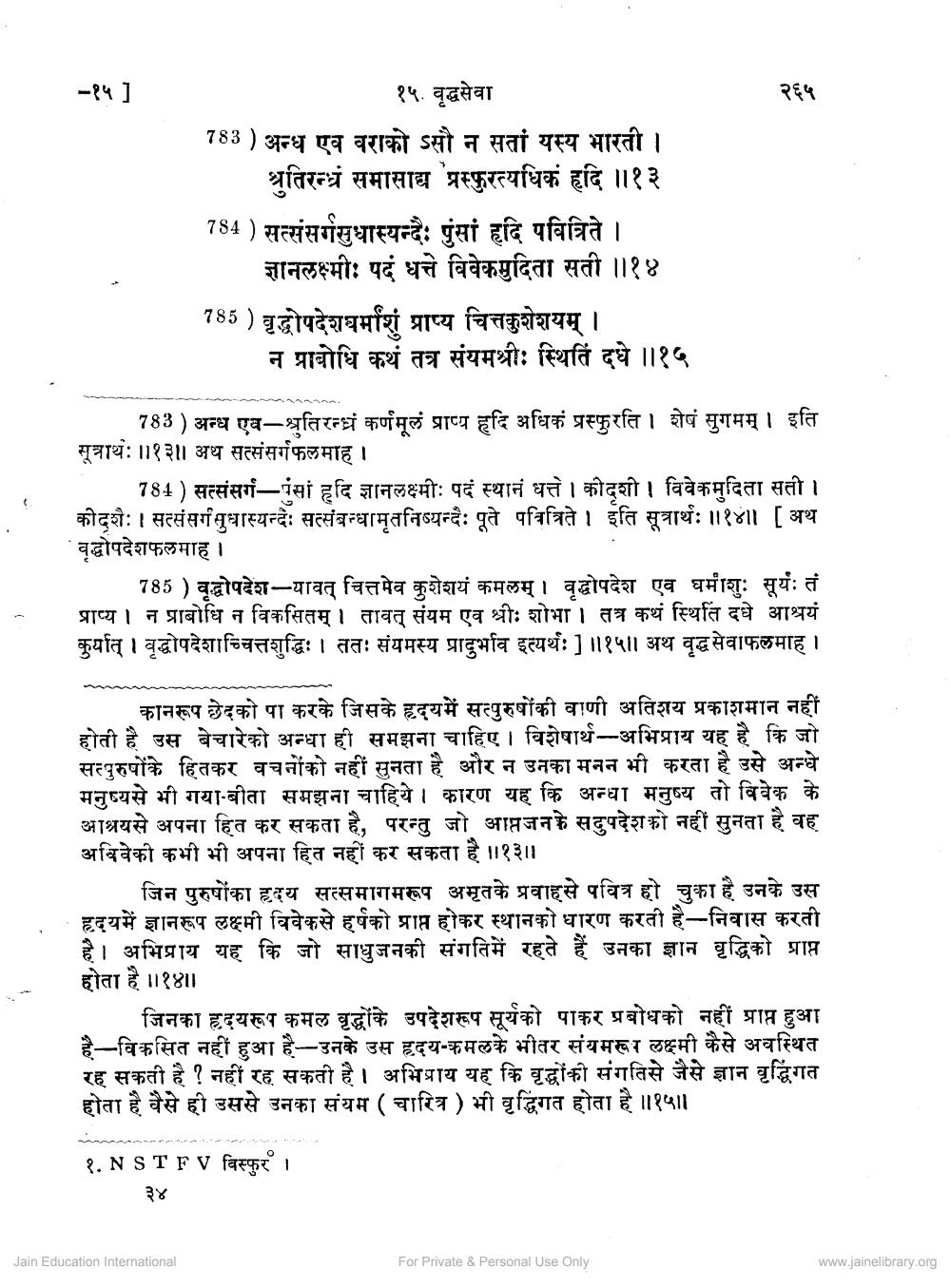________________
- १५ ]
१५. वृद्धसेवा
783 ) अन्ध एव वराको ऽसौ न सतां यस्य भारती । श्रुतिरन्धं समासाद्य प्रस्फुरत्यधिकं हृदि ||१३ 784 ) सत्संसर्गसुधास्यन्दैः पुंसां हृदि पवित्रिते । ज्ञानलक्ष्मीः पदं धत्ते विवेकमुदिता सती ||१४
785 ) वृद्धोपदेशधर्मांशुं प्राप्य चित्तकुशेशयम् । न प्राबोधि कथं तत्र संयमश्रीः स्थितिं दधे ॥१५
783 ) अन्ध एव - श्रुतिरन्धं कर्णमूलं प्राप्य हृदि अधिकं प्रस्फुरति । शेषं सुगमम् । इति सूत्रार्थः ||१३|| अथ सत्संसर्गफलमाह ।
784 ) सत्संसर्ग — पुंसां हृदि ज्ञानलक्ष्मीः पदं स्थानं धत्ते । कीदृशी । विवेकमुदिता सती । कीदृशैः । सत्संसर्गसुधास्यन्दः सत्संबन्धामृतनिष्यन्दैः पूते पवित्रिते । इति सूत्रार्थः ॥ १४ ॥ [ अथ `वृद्धोपदेशफलमाह ।
२६५
785 ) वृद्धोपदेश - यावत् चित्तमेव कुशेशयं कमलम् । वृद्धोपदेश एवं घमाशुः सूर्यः तं प्राप्य । न प्राबोधि न विकसितम् । तावत् संयम एव श्रीः शोभा । तत्र कथं स्थिति दधे आश्रयं कुर्यात् । वृद्धोपदेशाच्चित्तशुद्धिः । ततः संयमस्य प्रादुर्भाव इत्यर्थः ] ||१५|| अथ वृद्ध सेवा फलमाह ।
कानरूप छेदको पा करके जिसके हृदय में सत्पुरुषोंकी वाणी अतिशय प्रकाशमान नहीं होती है उस बेचारेको अन्धा ही समझना चाहिए। विशेषार्थ - अभिप्राय यह है कि जो सत्पुरुषोंके हितकर वचनोंको नहीं सुनता है और न उनका मनन भी करता है उसे अन्धे मनुष्य से भी गया- बीता समझना चाहिये । कारण यह कि अन्धा मनुष्य तो विवेक के आश्रय से अपना हित कर सकता है, परन्तु जो आप्तजनके सदुपदेशको नहीं सुनता है वह अविवेकी कभी भी अपना हित नहीं कर सकता है || १३ ||
जिन पुरुषों का हृदय सत्समागमरूप अमृतके प्रवाहसे पवित्र हो चुका है उनके उस हृदय में ज्ञानरूप लक्ष्मी विवेकसे हर्षको प्राप्त होकर स्थानको धारण करती है - निवास करती है | अभिप्राय यह कि जो साधुजनकी संगतिमें रहते हैं उनका ज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता है ||१४||
Jain Education International
जिनका हृदयरूप कमल वृद्धोंके उपदेशरूप सूर्यको पाकर प्रबोधको नहीं प्राप्त हुआ है - विकसित नहीं हुआ है- उनके उस हृदय-कमलके भीतर संयमरून लक्ष्मी कैसे अवस्थित रह सकती है ? नहीं रह सकती है । अभिप्राय यह कि वृद्धोंकी संगतिसे जैसे ज्ञान वृद्धिंगत होता है वैसे ही उससे उनका संयम ( चारित्र ) भी वृद्धिंगत होता है || १५ ||
१. N STF V विस्फुरं ।
३४
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org