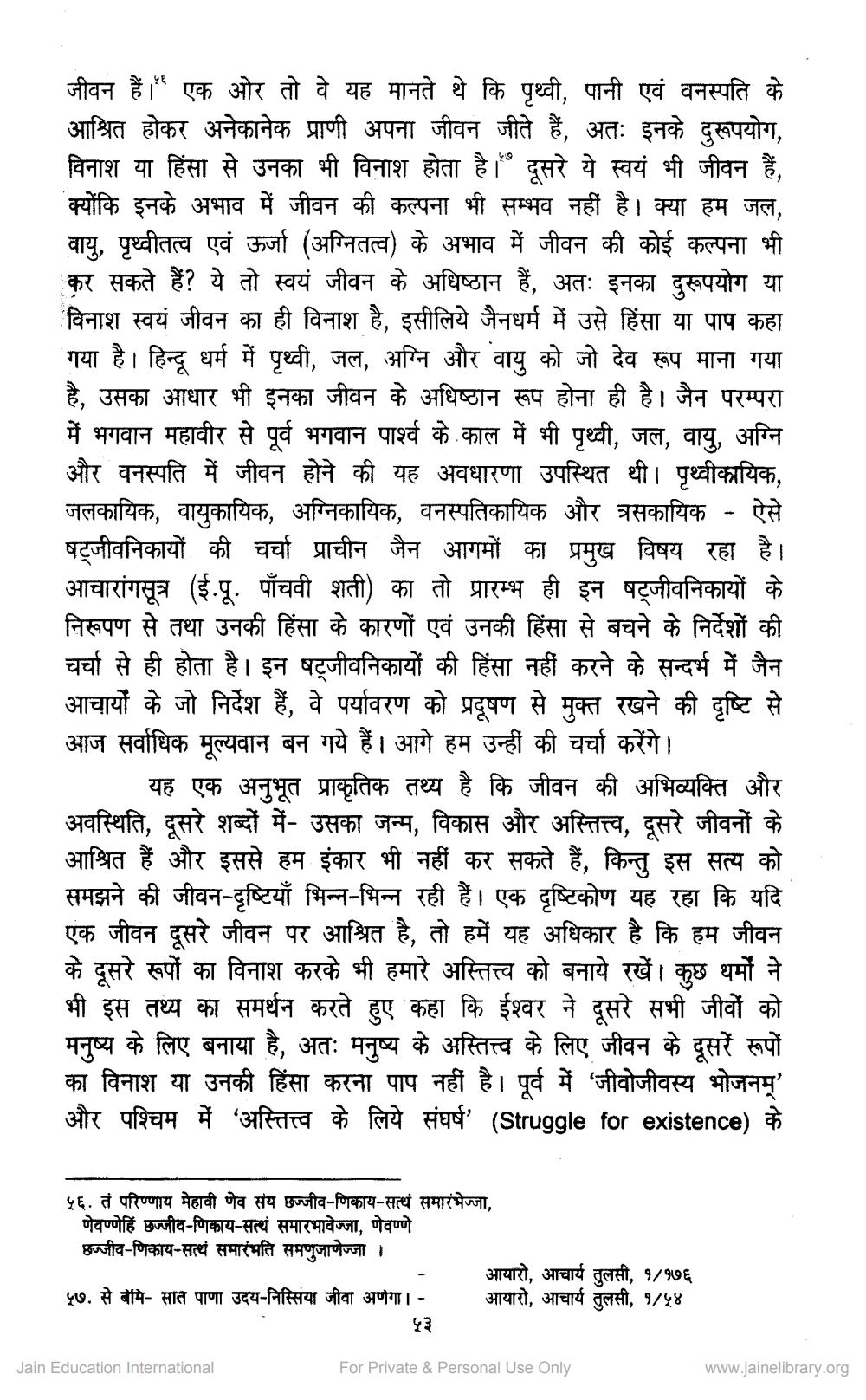________________
जीवन हैं। " एक ओर तो वे यह मानते थे कि पृथ्वी, पानी एवं वनस्पति के आश्रित होकर अनेकानेक प्राणी अपना जीवन जीते हैं, अतः इनके दुरूपयोग, विनाश या हिंसा से उनका भी विनाश होता है। दूसरे ये स्वयं भी जीवन हैं, क्योंकि इनके अभाव में जीवन की कल्पना भी सम्भव नहीं है । क्या हम जल, वायु, पृथ्वीतत्व एवं ऊर्जा (अग्नितत्व ) के अभाव में जीवन की कोई कल्पना भी कर सकते हैं? ये तो स्वयं जीवन के अधिष्ठान हैं, अतः इनका दुरूपयोग या विनाश स्वयं जीवन का ही विनाश है, इसीलिये जैनधर्म में उसे हिंसा या पाप कहा दूधर्म पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को जो देव रूप माना गया है, उसका आधार भी इनका जीवन के अधिष्ठान रूप होना ही है। जैन परम्परा में भगवान महावीर से पूर्व भगवान पार्श्व के काल में भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति में जीवन होने की यह अवधारणा उपस्थित थी । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक ऐसे षट्जीवनिकायों की चर्चा प्राचीन जैन आगमों का प्रमुख विषय रहा है आचारांगसूत्र (ई.पू. पाँचवी शती) का तो प्रारम्भ ही इन षट्जीवनिकायों के निरूपण से तथा उनकी हिंसा के कारणों एवं उनकी हिंसा से बचने के निर्देशों की चर्चा से ही होता है । इन षट्जीवनिकायों की हिंसा नहीं करने के सन्दर्भ में जैन आचार्यों के जो निर्देश हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने की दृष्टि से आज सर्वाधिक मूल्यवान बन गये हैं। आगे हम उन्हीं की चर्चा करेंगे ।
I
यह एक अनुभूत प्राकृतिक तथ्य है कि जीवन की अभिव्यक्ति और अवस्थिति, दूसरे शब्दों में- उसका जन्म, विकास और अस्तित्त्व, दूसरे जीवनों के आश्रित हैं और इससे हम इंकार भी नहीं कर सकते हैं, किन्तु इस सत्य को समझने की जीवन-दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न रही हैं। एक दृष्टिकोण यह रहा कि यदि एक जीवन दूसरे जीवन पर आश्रित है, तो हमें यह अधिकार है कि हम जीवन के दूसरे रूपों का विनाश करके भी हमारे अस्तित्त्व को बनाये रखें कुछ धर्मों ने भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा कि ईश्वर ने दूसरे सभी जीवों को मनुष्य के लिए बनाया है, अतः मनुष्य के अस्तित्त्व के लिए जीवन के दूसरें रूपों का विनाश या उनकी हिंसा करना पाप नहीं है। पूर्व में ' जीवोजीवस्य भोजनम्' और पश्चिम में ‘अस्तित्त्व के लिये संघर्ष' (Struggle for existence) के
५६. तं परिण्णाय मेहावी णेव संय छज्जीव- णिकाय-सत्थं समारंभेज्जा, वणेहिं छज्जीव- णिकाय-सत्थं समारभावेज्जा, जेवणे
छज्जीव- णिकाय-सत्थं समारंभति समणुजाणेज्जा ।
५७. से बेमि- सात पाणा उदय निस्सिया जीवा अणेगा। -
५३
Jain Education International
आयारो, आचार्य तुलसी, १/१७६ आयारो, आचार्य तुलसी, १ / ५४
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org