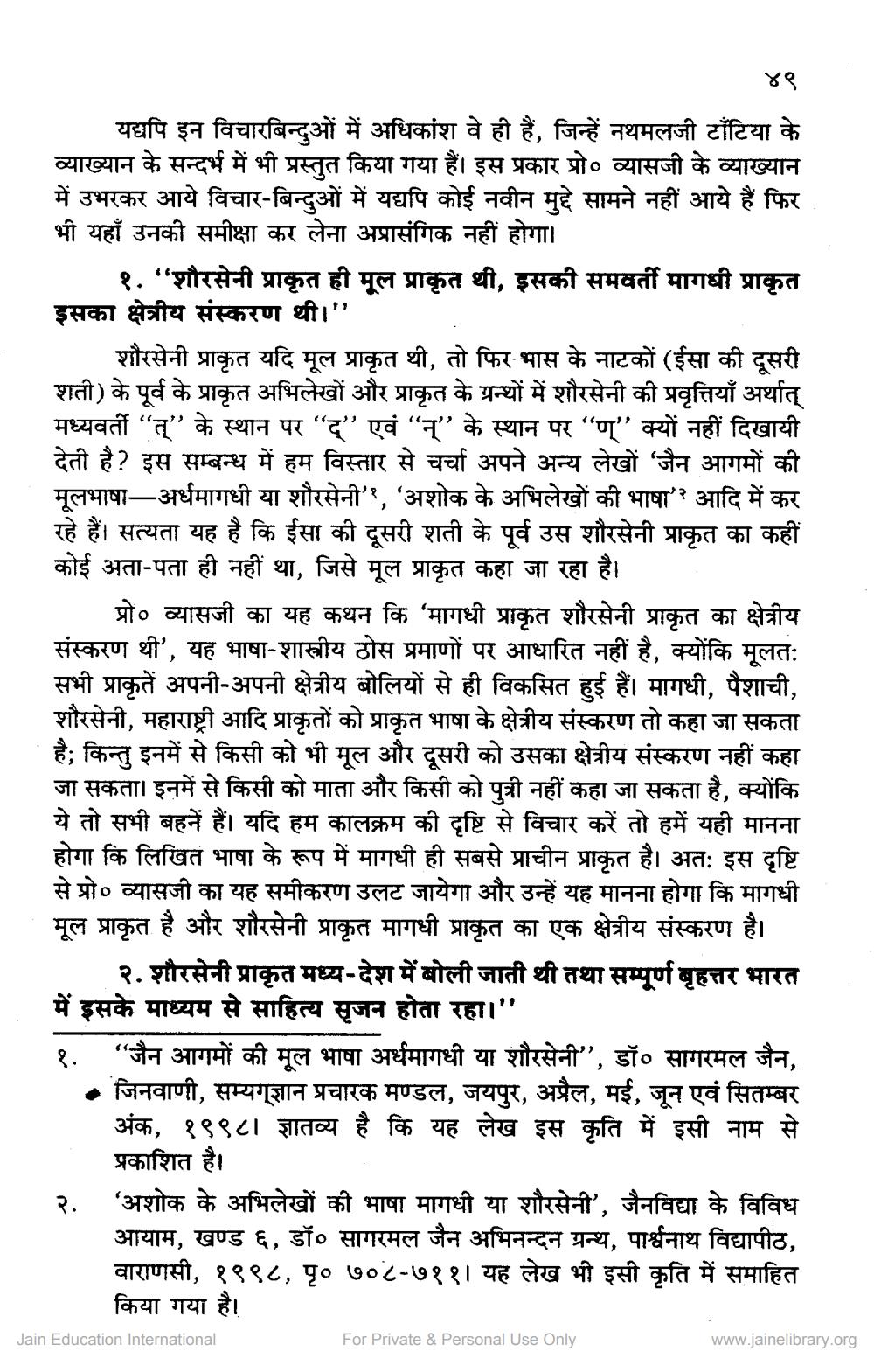________________
४९
यद्यपि इन विचारबिन्दुओं में अधिकांश वे ही हैं, जिन्हें नथमलजी टाँटिया के व्याख्यान के सन्दर्भ में भी प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार प्रो० व्यासजी के व्याख्यान में उभरकर आये विचार-बिन्दुओं में यद्यपि कोई नवीन मुद्दे सामने नहीं आये हैं फिर भी यहाँ उनकी समीक्षा कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा।
१. "शौरसेनी प्राकृत ही मूल प्राकृत थी, इसकी समवर्ती मागधी प्राकृत इसका क्षेत्रीय संस्करण थी।"
शौरसेनी प्राकृत यदि मूल प्राकृत थी, तो फिर भास के नाटकों (ईसा की दूसरी शती) के पूर्व के प्राकृत अभिलेखों और प्राकृत के ग्रन्थों में शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ अर्थात् मध्यवर्ती "त्" के स्थान पर “द्' एवं “न्" के स्थान पर “ण” क्यों नहीं दिखायी देती है? इस सम्बन्ध में हम विस्तार से चर्चा अपने अन्य लेखों 'जैन आगमों की मलभाषा-अर्धमागधी या शौरसेनी', 'अशोक के अभिलेखों की भाषा'२ आदि में कर रहे हैं। सत्यता यह है कि ईसा की दूसरी शती के पूर्व उस शौरसेनी प्राकृत का कहीं कोई अता-पता ही नहीं था, जिसे मूल प्राकृत कहा जा रहा है।
प्रो० व्यासजी का यह कथन कि 'मागधी प्राकृत शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्रीय संस्करण थी', यह भाषा-शास्त्रीय ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है, क्योंकि मूलतः सभी प्राकृतें अपनी-अपनी क्षेत्रीय बोलियों से ही विकसित हुई हैं। मागधी, पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि प्राकृतों को प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय संस्करण तो कहा जा सकता है; किन्तु इनमें से किसी को भी मूल और दूसरी को उसका क्षेत्रीय संस्करण नहीं कहा जा सकता। इनमें से किसी को माता और किसी को पुत्री नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो सभी बहनें हैं। यदि हम कालक्रम की दृष्टि से विचार करें तो हमें यही मानना होगा कि लिखित भाषा के रूप में मागधी ही सबसे प्राचीन प्राकृत है। अत: इस दृष्टि से प्रो० व्यासजी का यह समीकरण उलट जायेगा और उन्हें यह मानना होगा कि मागधी मूल प्राकृत है और शौरसेनी प्राकृत मागधी प्राकृत का एक क्षेत्रीय संस्करण है।
२.शौरसेनी प्राकृत मध्य-देश में बोली जाती थी तथा सम्पूर्ण बृहत्तर भारत में इसके माध्यम से साहित्य सृजन होता रहा।" १. “जैन आगमों की मूल भाषा अर्धमागधी या शौरसेनी', डॉ० सागरमल जैन, • जिनवाणी, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर, अप्रैल, मई, जून एवं सितम्बर
अंक, १९९८। ज्ञातव्य है कि यह लेख इस कृति में इसी नाम से प्रकाशित है। 'अशोक के अभिलेखों की भाषा मागधी या शौरसेनी', जैनविद्या के विविध
आयाम, खण्ड ६, डॉ० सागरमल जैन अभिनन्दन ग्रन्थ, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी, १९९८, पृ० ७०८-७११। यह लेख भी इसी कृति में समाहित किया गया है।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org