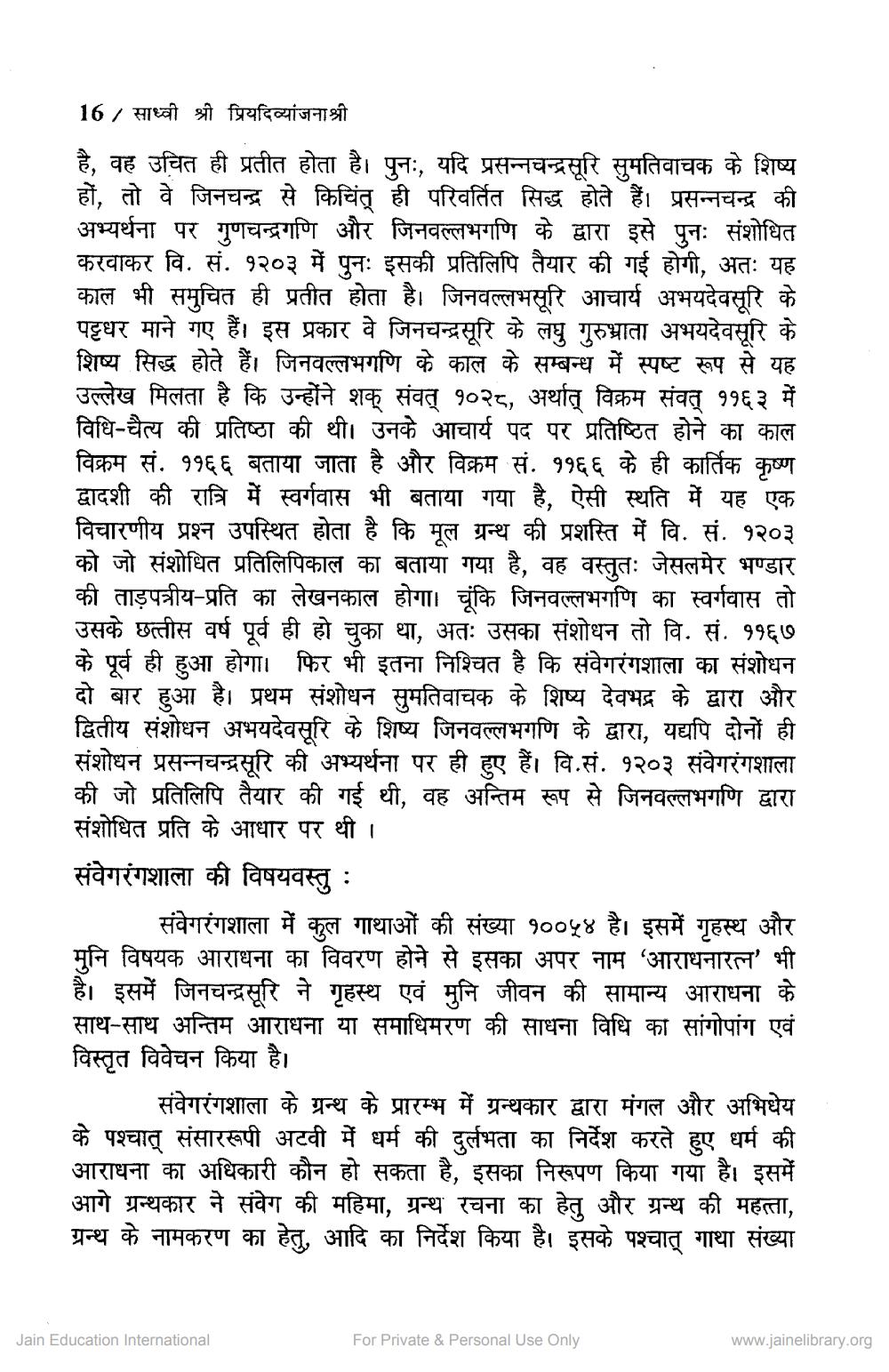________________
16 / साध्वी श्री प्रियदिव्यांजनाश्री है, वह उचित ही प्रतीत होता है। पुनः, यदि प्रसन्नचन्द्रसूरि सुमतिवाचक के शिष्य हों, तो वे जिनचन्द्र से किचिंतू ही परिवर्तित सिद्ध होते हैं। प्रसन्नचन्द्र की अभ्यर्थना पर गुणचन्द्रगणि और जिनवल्लभगणि के द्वारा इसे पुनः संशोधित करवाकर वि. सं. १२०३ में पुनः इसकी प्रतिलिपि तैयार की गई होगी, अतः यह काल भी समुचित ही प्रतीत होता है। जिनवल्लभसूरि आचार्य अभयदेवसूरि के पट्टधर माने गए हैं। इस प्रकार वे जिनचन्द्रसूरि के लघु गुरुभ्राता अभयदेवसूरि के शिष्य सिद्ध होते हैं। जिनवल्लभगणि के काल के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने शक् संवत् १०२८, अर्थात् विक्रम संवत् ११६३ में विधि-चैत्य की प्रतिष्ठा की थी। उनके आचार्य पद पर प्रतिष्टित होने का काल विक्रम सं. ११६६ बताया जाता है और विक्रम सं. ११६६ के ही कार्तिक कृष्ण द्वादशी की रात्रि में स्वर्गवास भी बताया गया है, ऐसी स्थति में यह एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है कि मूल ग्रन्थ की प्रशस्ति में वि. सं. १२०३ को जो संशोधित प्रतिलिपिकाल का बताया गया है, वह वस्तुतः जेसलमेर भण्डार की ताड़पत्रीय प्रति का लेखनकाल होगा। चूंकि जिनवल्लभगणि का स्वर्गवास तो उसके छत्तीस वर्ष पूर्व ही हो चुका था, अतः उसका संशोधन तो वि. सं. ११६७ के पूर्व ही हुआ होगा। फिर भी इतना निश्चित है कि संवेगरंगशाला का संशोधन दो बार हुआ है। प्रथम संशोधन सुमतिवाचक के शिष्य देवभद्र के द्वारा और द्वितीय संशोधन अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लभगणि के द्वारा, यद्यपि दोनों ही संशोधन प्रसन्नचन्द्रसूरि की अभ्यर्थना पर ही हुए हैं। वि.सं. १२०३ संवेगरंगशाला की जो प्रतिलिपि तैयार की गई थी, वह अन्तिम रूप से जिनवल्लभगणि द्वारा संशोधित प्रति के आधार पर थी। संवेगरंगशाला की विषयवस्तु :
संवेगरंगशाला में कुल गाथाओं की संख्या १००५४ है। इसमें गृहस्थ और मुनि विषयक आराधना का विवरण होने से इसका अपर नाम 'आराधनारत्न' भी है। इसमें जिनचन्द्रसूरि ने गृहस्थ एवं मुनि जीवन की सामान्य आराधना के साथ-साथ अन्तिम आराधना या समाधिमरण की साधना विधि का सांगोपांग एवं विस्तृत विवेचन किया है।
संवेगरंगशाला के ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार द्वारा मंगल और अभिधेय के पश्चात् संसाररूपी अटवी में धर्म की दुर्लभता का निर्देश करते हुए धर्म की आराधना का अधिकारी कौन हो सकता है, इसका निरूपण किया गया है। इसमें आगे ग्रन्थकार ने संवेग की महिमा, ग्रन्थ रचना का हेतु और ग्रन्थ की महत्ता, ग्रन्थ के नामकरण का हेतु, आदि का निर्देश किया है। इसके पश्चात् गाथा संख्या
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org