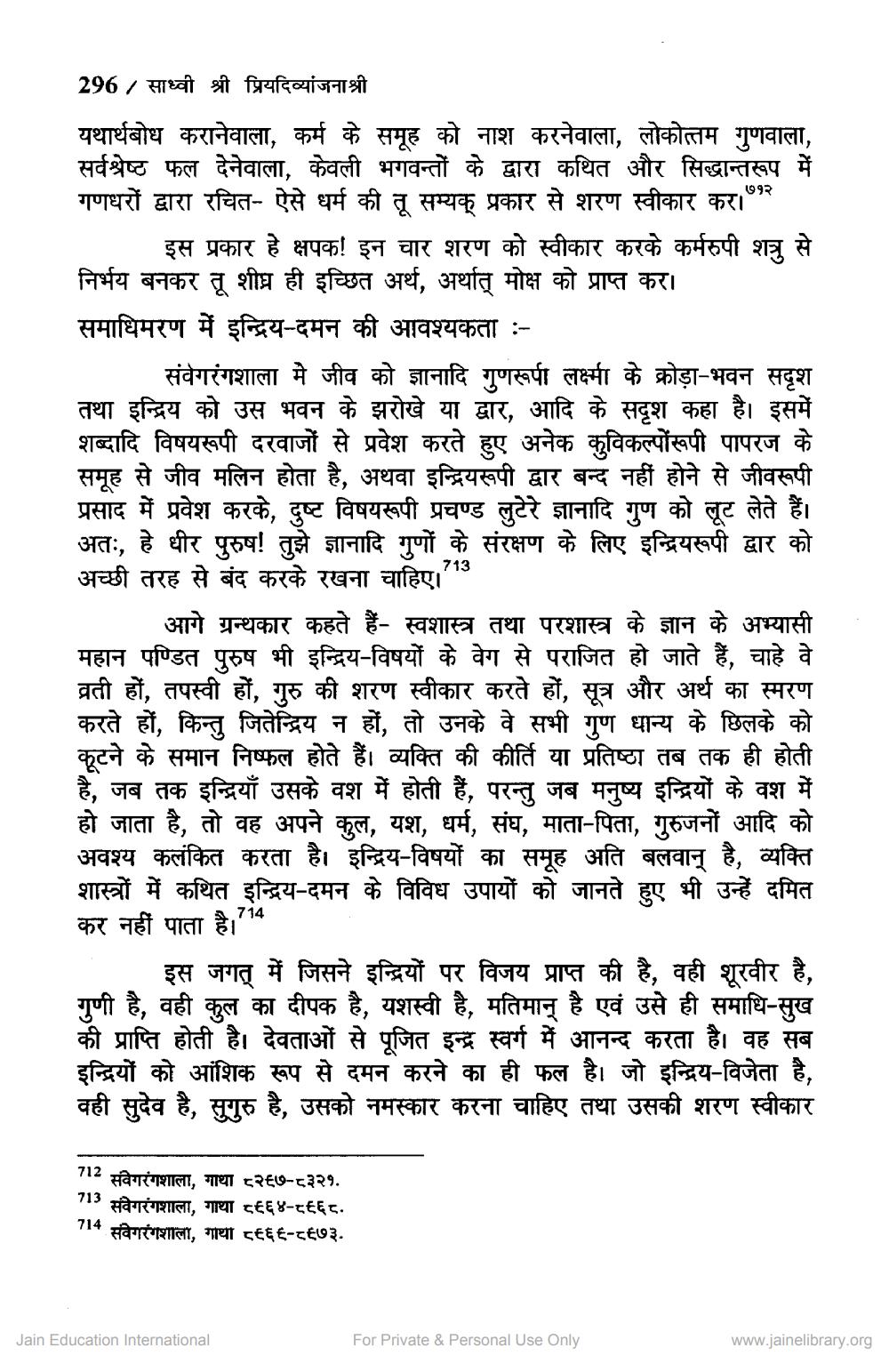________________
296 / साध्वी श्री प्रियदिव्यांजनाश्री यथार्थबोध करानेवाला, कर्म के समूह को नाश करनेवाला, लोकोत्तम गुणवाला, सर्वश्रेष्ठ फल देनेवाला, केवली भगवन्तों के द्वारा कथित और सिद्धान्तरूप में गणधरों द्वारा रचित- ऐसे धर्म की तू सम्यक् प्रकार से शरण स्वीकार कर। १२ ।
इस प्रकार हे क्षपक! इन चार शरण को स्वीकार करके कर्मरुपी शत्रु से निर्भय बनकर तू शीघ्र ही इच्छित अर्थ, अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर। समाधिमरण में इन्द्रिय-दमन की आवश्यकता :
__ संवेगरंगशाला मे जीव को ज्ञानादि गुणरूपी लक्ष्मी के क्रोड़ा-भवन सदृश तथा इन्द्रिय को उस भवन के झरोखे या द्वार, आदि के सदृश कहा है। इसमें शब्दादि विषयरूपी दरवाजों से प्रवेश करते हुए अनेक कुविकल्पोंरूपी पापरज के समूह से जीव मलिन होता है, अथवा इन्द्रियरूपी द्वार बन्द नहीं होने से जीवरूपी प्रसाद में प्रवेश करके, दुष्ट विषयरूपी प्रचण्ड लुटेरे ज्ञानादि गुण को लूट लेते हैं। अतः, हे धीर पुरुष! तुझे ज्ञानादि गुणों के संरक्षण के लिए इन्द्रियरूपी द्वार को अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए।
आगे ग्रन्थकार कहते हैं- स्वशास्त्र तथा परशास्त्र के ज्ञान के अभ्यासी महान पण्डित पुरुष भी इन्द्रिय-विषयों के वेग से पराजित हो जाते हैं, चाहे वे व्रती हों, तपस्वी हों, गुरु की शरण स्वीकार करते हों, सूत्र और अर्थ का स्मरण करते हों, किन्तु जितेन्द्रिय न हों, तो उनके वे सभी गुण धान्य के छिलके को कूटने के समान निष्फल होते हैं। व्यक्ति की कीर्ति या प्रतिष्ठा तब तक ही होती है, जब तक इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं, परन्तु जब मनुष्य इन्द्रियों के वश में हो जाता है, तो वह अपने कुल, यश, धर्म, संघ, माता-पिता, गुरुजनों आदि को अवश्य कलंकित करता है। इन्द्रिय-विषयों का समूह अति बलवान् है, व्यक्ति शास्त्रों में कथित इन्द्रिय-दमन के विविध उपायों को जानते हुए भी उन्हें दमित कर नहीं पाता है।
इस जगत में जिसने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की है, वही शूरवीर है, गुणी है, वही कुल का दीपक है, यशस्वी है, मतिमान् है एवं उसे ही समाधि-सुख की प्राप्ति होती है। देवताओं से पूजित इन्द्र स्वर्ग में आनन्द करता है। वह सब इन्द्रियों को आंशिक रूप से दमन करने का ही फल है। जो इन्द्रिय-विजेता है, वही सुदेव है, सुगुरु है, उसको नमस्कार करना चाहिए तथा उसकी शरण स्वीकार
712 विंगरंगशाला, गाथा ८२६७-८३२१. 713 संवेगरंगशाला, गाथा ८६६४-८६६८. १ विगरंगशाला, गाथा ८६६६-८६७३.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org