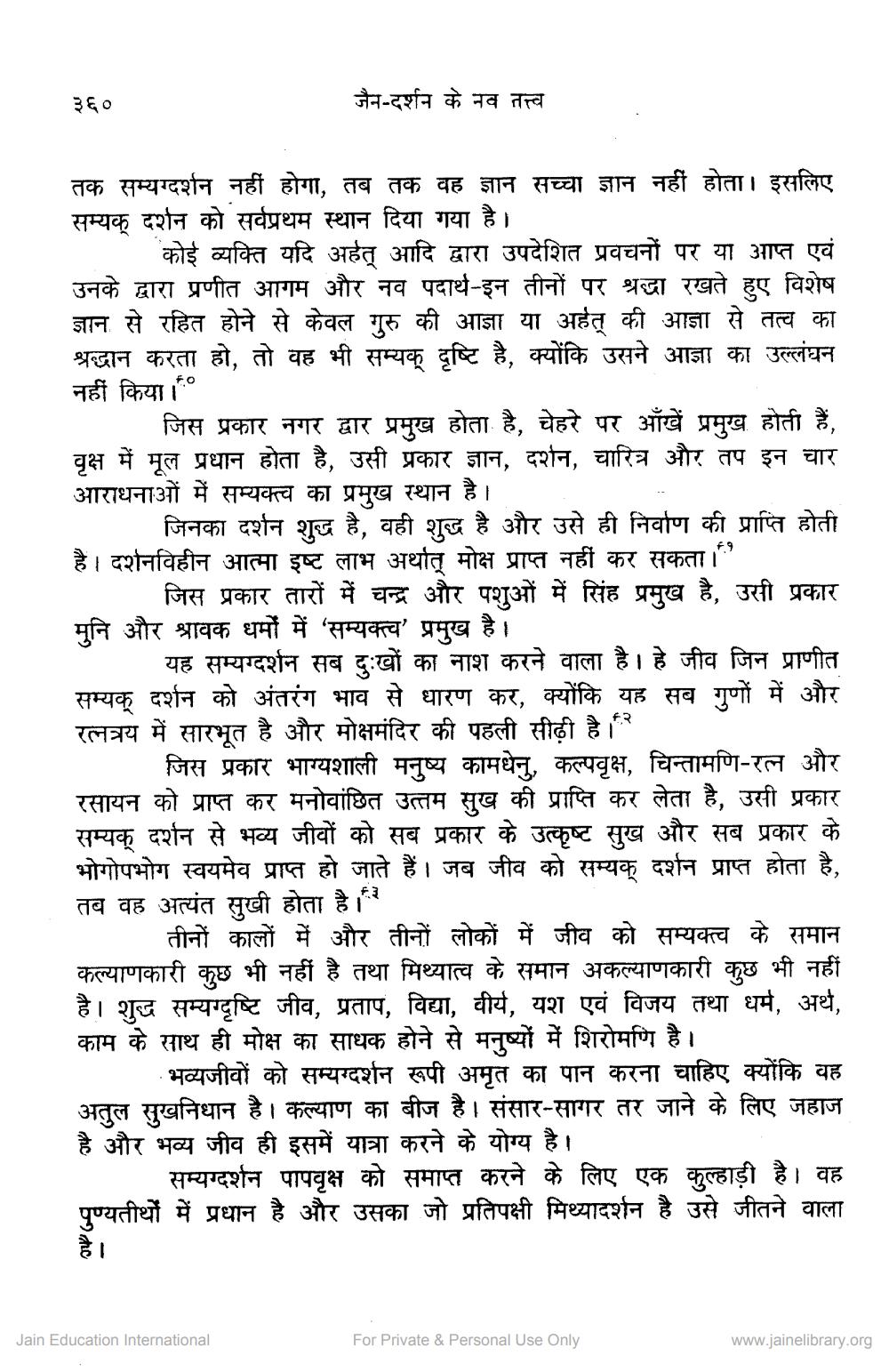________________
जैन-दर्शन के नव तत्त्व
तक सम्यग्दर्शन नहीं होगा, तब तक वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता। इसलिए सम्यक् दर्शन को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है।
कोई व्यक्ति यदि अर्हत् आदि द्वारा उपदेशित प्रवचनों पर या आप्त एवं उनके द्वारा प्रणीत आगम और नव पदार्थ-इन तीनों पर श्रद्धा रखते हुए विशेष ज्ञान से रहित होने से केवल गुरु की आज्ञा या अर्हत् की आज्ञा से तत्व का श्रद्धान करता हो, तो वह भी सम्यक् दृष्टि है, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।
जिस प्रकार नगर द्वार प्रमुख होता है, चेहरे पर आँखें प्रमुख होती हैं, वृक्ष में मूल प्रधान होता है, उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चार आराधनाओं में सम्यक्त्व का प्रमुख स्थान है।
जिनका दर्शन शुद्ध है, वही शुद्ध है और उसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। दर्शनविहीन आत्मा इष्ट लाभ अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।"
जिस प्रकार तारों में चन्द्र और पशुओं में सिंह प्रमुख है, उसी प्रकार मुनि और श्रावक धमों में 'सम्यक्त्व' प्रमुख है।
यह सम्यग्दर्शन सब दुःखों का नाश करने वाला है। हे जीव जिन प्राणीत सम्यक् दर्शन को अंतरंग भाव से धारण कर, क्योंकि यह सब गुणों में और रत्नत्रय में सारभूत है और मोक्षमंदिर की पहली सीढ़ी है।
जिस प्रकार भाग्यशाली मनुष्य कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि-रत्न और रसायन को प्राप्त कर मनोवांछित उत्तम सुख की प्राप्ति कर लेता है, उसी प्रकार सम्यक् दर्शन से भव्य जीवों को सब प्रकार के उत्कृष्ट सुख और सब प्रकार के भोगोपभोग स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं। जब जीव को सम्यक् दर्शन प्राप्त होता है, तब वह अत्यंत सुखी होता है।
तीनों कालों में और तीनों लोकों में जीव को सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी कुछ भी नहीं है तथा मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कुछ भी नहीं है। शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, प्रताप, विद्या, वीर्य, यश एवं विजय तथा धर्म, अर्थ, काम के साथ ही मोक्ष का साधक होने से मनुष्यों में शिरोमणि है।
भव्यजीवों को सम्यग्दर्शन रूपी अमृत का पान करना चाहिए क्योंकि वह अतुल सुखनिधान है। कल्याण का बीज है। संसार-सागर तर जाने के लिए जहाज है और भव्य जीव ही इसमें यात्रा करने के योग्य है।
सम्यग्दर्शन पापवृक्ष को समाप्त करने के लिए एक कुल्हाड़ी है। वह पुण्यतीथों में प्रधान है और उसका जो प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शन है उसे जीतने वाला
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org