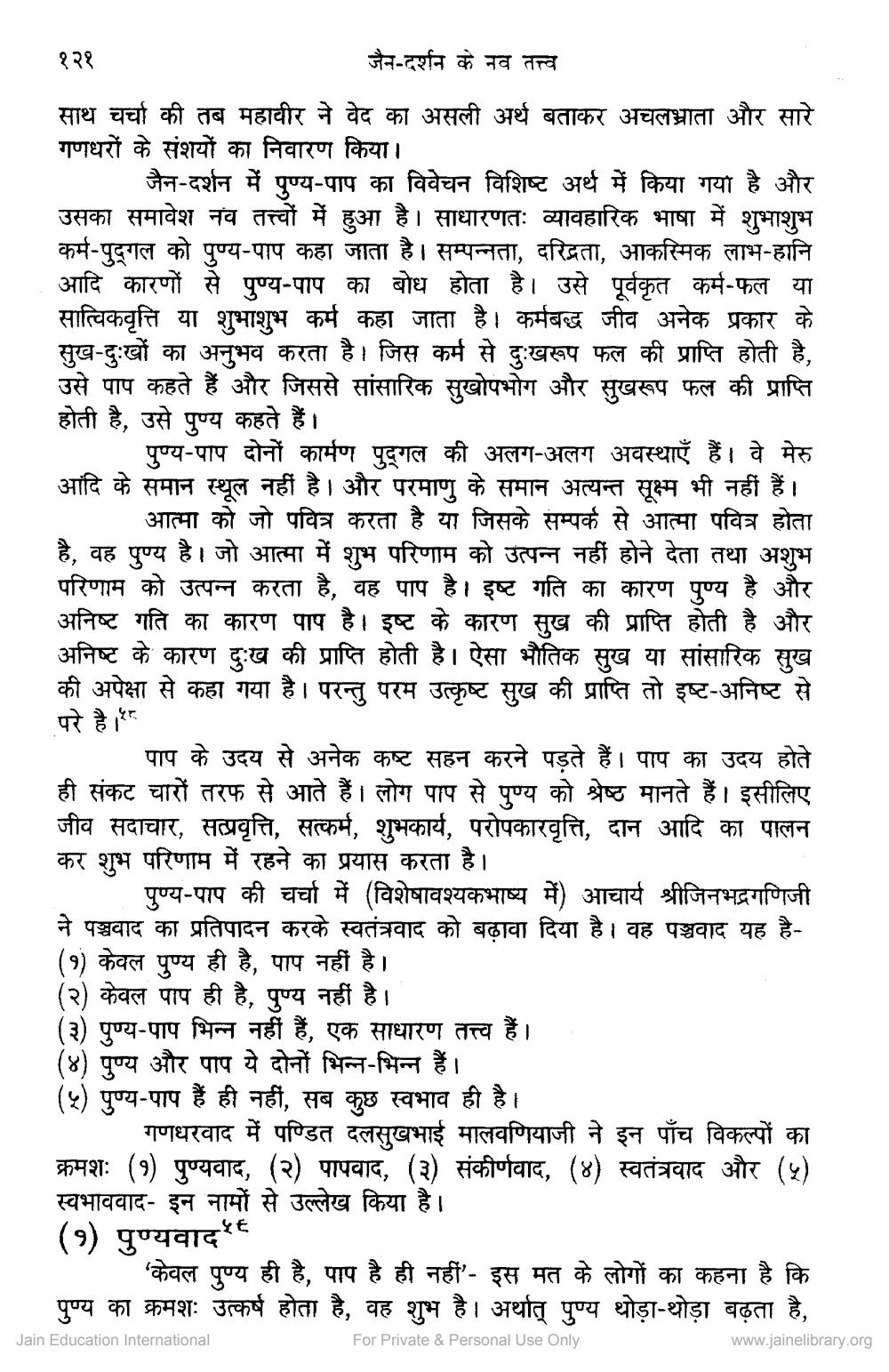________________
१२१
जैन-दर्शन के नव तत्त्व साथ चर्चा की तब महावीर ने वेद का असली अर्थ बताकर अचलभ्राता और सारे गणधरों के संशयों का निवारण किया।
जैन-दर्शन में पुण्य-पाप का विवेचन विशिष्ट अर्थ में किया गया है और उसका समावेश नव तत्त्वों में हुआ है। साधारणतः व्यावहारिक भाषा में शुभाशुभ कर्म-पुद्गल को पुण्य-पाप कहा जाता है। सम्पन्नता, दरिद्रता, आकस्मिक लाभ-हानि आदि कारणों से पुण्य-पाप का बोध होता है। उसे पूर्वकृत कर्म-फल या सात्विकवृत्ति या शुभाशुभ कर्म कहा जाता है। कर्मबद्ध जीव अनेक प्रकार के सुख-दुःखों का अनुभव करता है। जिस कर्म से दुःखरूप फल की प्राप्ति होती है, उसे पाप कहते हैं और जिससे सांसारिक सुखोपभोग और सुखरूप फल की प्राप्ति होती है, उसे पुण्य कहते हैं।
पुण्य-पाप दोनों कार्मण पुद्गल की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। वे मेरु आदि के समान स्थूल नहीं है। और परमाणु के समान अत्यन्त सूक्ष्म भी नहीं हैं।
आत्मा को जो पवित्र करता है या जिसके सम्पर्क से आत्मा पवित्र होता है, वह पुण्य है। जो आत्मा में शुभ परिणाम को उत्पन्न नहीं होने देता तथा अशुभ परिणाम को उत्पन्न करता है, वह पाप है। इष्ट गति का कारण पुण्य है और अनिष्ट गति का कारण पाप है। इष्ट के कारण सुख की प्राप्ति होती है और अनिष्ट के कारण दुःख की प्राप्ति होती है। ऐसा भौतिक सुख या सांसारिक सुख की अपेक्षा से कहा गया है। परन्तु परम उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति तो इष्ट-अनिष्ट से परे है।
पाप के उदय से अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। पाप का उदय होते ही संकट चारों तरफ से आते हैं। लोग पाप से पुण्य को श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए जीव सदाचार, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म, शुभकार्य, परोपकारवृत्ति, दान आदि का पालन कर शुभ परिणाम में रहने का प्रयास करता है।
पुण्य-पाप की चर्चा में (विशेषावश्यकभाष्य में) आचार्य श्रीजिनभद्रगणिजी ने पञ्चवाद का प्रतिपादन करके स्वतंत्रवाद को बढ़ावा दिया है। वह पञ्चवाद यह है(१) केवल पुण्य ही है, पाप नहीं है। (२) केवल पाप ही है, पुण्य नहीं है। (३) पुण्य-पाप भिन्न नहीं हैं, एक साधारण तत्त्व हैं। (४) पुण्य और पाप ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। (५) पुण्य-पाप हैं ही नहीं, सब कुछ स्वभाव ही है।
___ गणधरवाद में पण्डित दलसुखभाई मालवणियाजी ने इन पाँच विकल्पों का क्रमशः (१) पुण्यवाद, (२) पापवाद, (३) संकीर्णवाद, (४) स्वतंत्रवाद और (५) स्वभाववाद- इन नामों से उल्लेख किया है। (१) पुण्यवाद
'केवल पुण्य ही है, पाप है ही नहीं'- इस मत के लोगों का कहना है कि पुण्य का क्रमशः उत्कर्ष होता है, वह शुभ है। अर्थात् पुण्य थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है, Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org