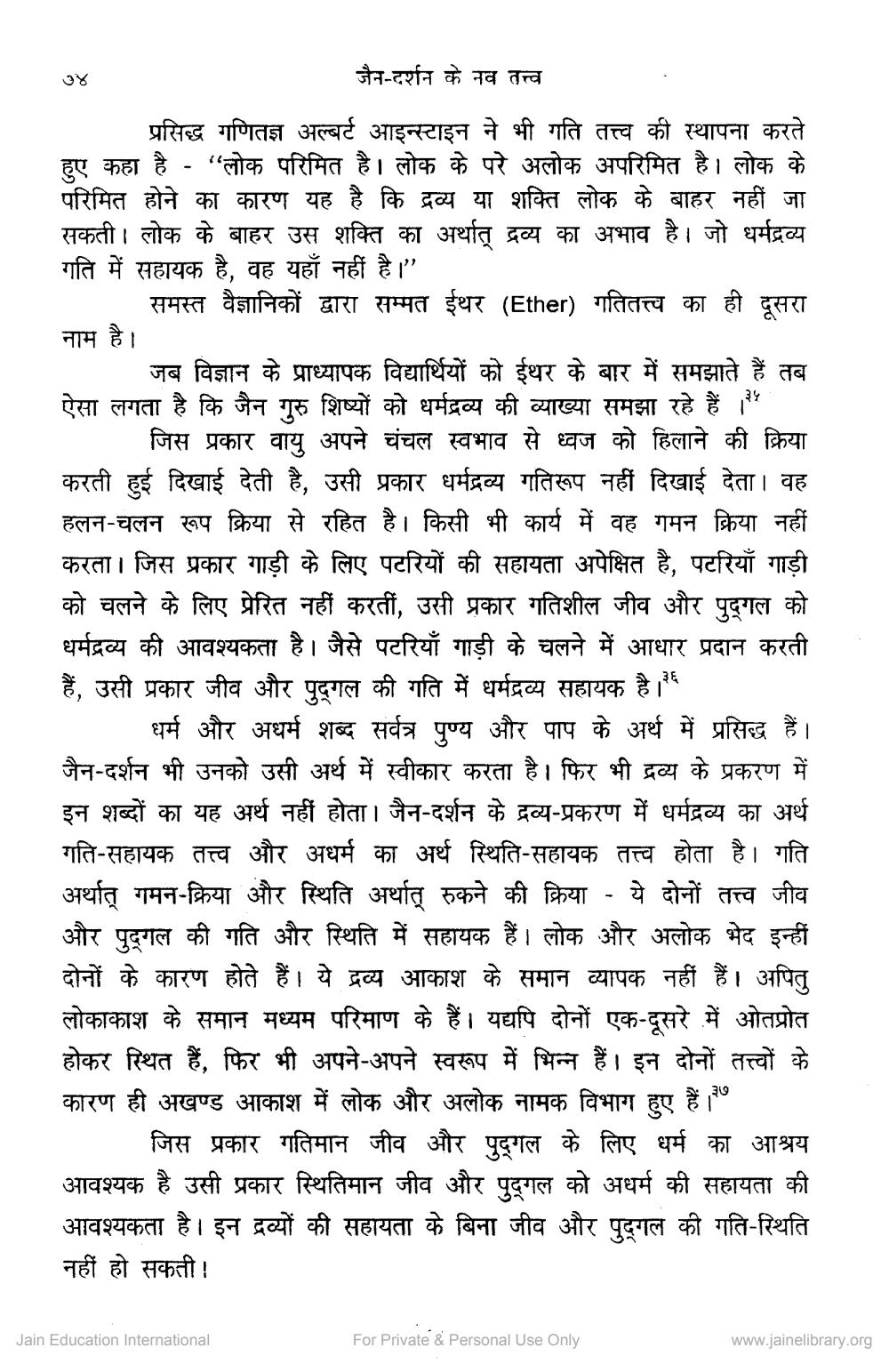________________
७४
जैन-दर्शन के नव तत्त्व प्रसिद्ध गणितज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने भी गति तत्त्व की स्थापना करते हुए कहा है - "लोक परिमित है। लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य या शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का अर्थात् द्रव्य का अभाव है। जो धर्मद्रव्य गति में सहायक है, वह यहाँ नहीं है।"
समस्त वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर (Ether) गतितत्त्व का ही दूसरा नाम है।
जब विज्ञान के प्राध्यापक विद्यार्थियों को ईथर के बार में समझाते हैं तब ऐसा लगता है कि जैन गुरु शिष्यों को धर्मद्रव्य की व्याख्या समझा रहे हैं ।३५
जिस प्रकार वायु अपने चंचल स्वभाव से ध्वज को हिलाने की क्रिया करती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य गतिरूप नहीं दिखाई देता। वह हलन-चलन रूप क्रिया से रहित है। किसी भी कार्य में वह गमन क्रिया नहीं करता। जिस प्रकार गाड़ी के लिए पटरियों की सहायता अपेक्षित है, पटरियाँ गाड़ी को चलने के लिए प्रेरित नहीं करतीं, उसी प्रकार गतिशील जीव और पुद्गल को धर्मद्रव्य की आवश्यकता है। जैसे पटरियाँ गाड़ी के चलने में आधार प्रदान करती हैं, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति में धर्मद्रव्य सहायक है।
धर्म और अधर्म शब्द सर्वत्र पुण्य और पाप के अर्थ में प्रसिद्ध हैं। जैन-दर्शन भी उनको उसी अर्थ में स्वीकार करता है। फिर भी द्रव्य के प्रकरण में इन शब्दों का यह अर्थ नहीं होता। जैन-दर्शन के द्रव्य-प्रकरण में धर्मद्रव्य का अर्थ गति-सहायक तत्त्व और अधर्म का अर्थ स्थिति-सहायक तत्त्व होता है। गति अर्थात् गमन-क्रिया और स्थिति अर्थात् रुकने की क्रिया - ये दोनों तत्त्व जीव
और पुद्गल की गति और स्थिति में सहायक हैं। लोक और अलोक भेद इन्हीं दोनों के कारण होते हैं। ये द्रव्य आकाश के समान व्यापक नहीं हैं। अपितु लोकाकाश के समान मध्यम परिमाण के हैं। यद्यपि दोनों एक-दूसरे में ओतप्रोत होकर स्थित हैं, फिर भी अपने-अपने स्वरूप में भिन्न हैं। इन दोनों तत्त्वों के कारण ही अखण्ड आकाश में लोक और अलोक नामक विभाग हुए हैं।२७
जिस प्रकार गतिमान जीव और पुद्गल के लिए धर्म का आश्रय आवश्यक है उसी प्रकार स्थितिमान जीव और पुद्गल को अधर्म की सहायता की आवश्यकता है। इन द्रव्यों की सहायता के बिना जीव और पुद्गल की गति-स्थिति नहीं हो सकती।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org