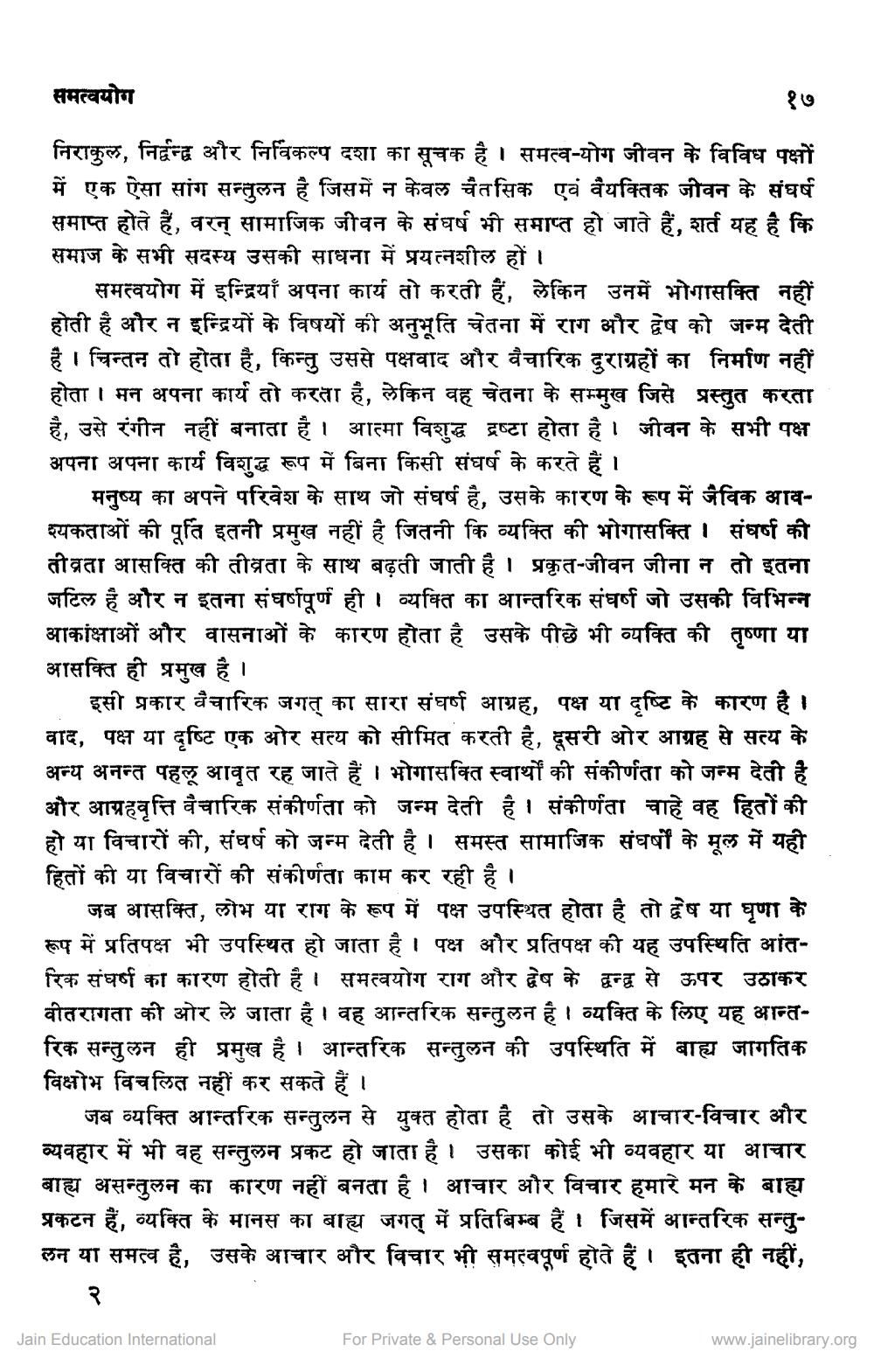________________
समत्वयोग
१७
निराकुल, निर्द्वन्द्व और निर्विकल्प दशा का सूचक है । समत्व-योग जीवन के विविध पक्षों में एक ऐसा सांग सन्तुलन है जिसमें न केवल चैतसिक एवं वैयक्तिक जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, वरन् सामाजिक जीवन के संघर्ष भी समाप्त हो जाते हैं, शर्त यह है कि समाज के सभी सदस्य उसकी साधना में प्रयत्नशील हों।
समत्वयोग में इन्द्रियाँ अपना कार्य तो करती हैं, लेकिन उनमें भोगासक्ति नहीं होती है और न इन्द्रियों के विषयों की अनुभूति चेतना में राग और द्वेष को जन्म देती है । चिन्तन तो होता है, किन्तु उससे पक्षवाद और वैचारिक दुराग्रहों का निर्माण नहीं होता । मन अपना कार्य तो करता है, लेकिन वह चेतना के सम्मुख जिसे प्रस्तुत करता है, उसे रंगीन नहीं बनाता है। आत्मा विशुद्ध द्रष्टा होता है। जीवन के सभी पक्ष अपना अपना कार्य विशुद्ध रूप में बिना किसी संघर्ष के करते हैं। ____ मनुष्य का अपने परिवेश के साथ जो संघर्ष है, उसके कारण के रूप में जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी प्रमुख नहीं है जितनी कि व्यक्ति की भोगासक्ति । संघर्ष की तीव्रता आसक्ति की तीव्रता के साथ बढ़ती जाती है। प्रकृत-जीवन जीना न तो इतना जटिल है और न इतना संघर्षपूर्ण ही। व्यक्ति का आन्तरिक संघर्ष जो उसकी विभिन्न आकांक्षाओं और वासनाओं के कारण होता है उसके पीछे भी व्यक्ति की तृष्णा या आसक्ति ही प्रमुख है।
इसी प्रकार वैचारिक जगत् का सारा संघर्ष आग्रह, पक्ष या दृष्टि के कारण है। वाद, पक्ष या दृष्टि एक ओर सत्य को सीमित करती है, दूसरी ओर आग्रह से सत्य के अन्य अनन्त पहलू आवृत रह जाते हैं । भोगासक्ति स्वार्थों की संकीर्णता को जन्म देती है और आग्रहवृत्ति वैचारिक संकीर्णता को जन्म देती है। संकीर्णता चाहे वह हितों की हो या विचारों की, संघर्ष को जन्म देती है। समस्त सामाजिक संघर्षों के मूल में यही हितों की या विचारों की संकीर्णता काम कर रही है ।
जब आसक्ति, लोभ या राग के रूप में पक्ष उपस्थित होता है तो द्वेष या घृणा के रूप में प्रतिपक्ष भी उपस्थित हो जाता है । पक्ष और प्रतिपक्ष की यह उपस्थिति आंतरिक संघर्ष का कारण होती है। समत्वयोग राग और द्वेष के द्वन्द्व से ऊपर उठाकर वीतरागता की ओर ले जाता है । वह आन्तरिक सन्तुलन है । व्यक्ति के लिए यह आन्तरिक सन्तुलन ही प्रमुख है। आन्तरिक सन्तुलन की उपस्थिति में बाह्य जागतिक विक्षोभ विचलित नहीं कर सकते हैं ।
__ जब व्यक्ति आन्तरिक सन्तुलन से युक्त होता है तो उसके आचार-विचार और व्यवहार में भी वह सन्तुलन प्रकट हो जाता है। उसका कोई भी व्यवहार या आचार बाह्य असन्तुलन का कारण नहीं बनता है। आचार और विचार हमारे मन के बाह्य प्रकटन हैं, व्यक्ति के मानस का बाह्य जगत् में प्रतिबिम्ब हैं। जिसमें आन्तरिक सन्तुलन या समत्व है, उसके आचार और विचार भी समत्वपूर्ण होते हैं। इतना ही नहीं,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org